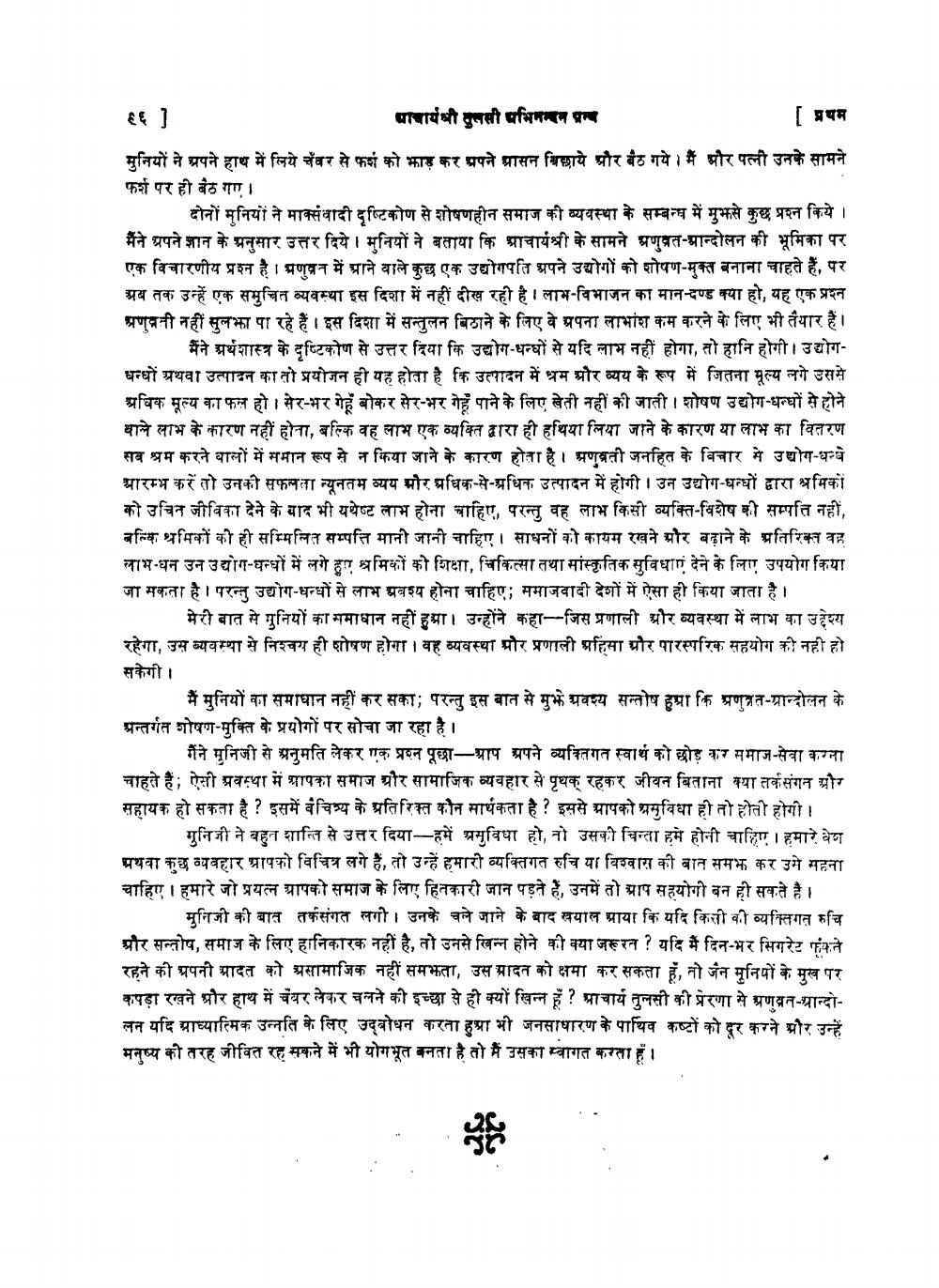________________
९६ ] पाचार्यश्री तुलसी पभिनन्दन अन्य
[ प्रथम मुनियों ने अपने हाथ में लिये वर से फर्श को झाड़ कर अपने प्रासन बिछाये और बैठ गये। मैं और पत्नी उनके सामने फर्श पर ही बैठ गए।
दोनों मनियों ने माक्सवादी दृष्टिकोण से शोषणहीन समाज की व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझसे कुछ प्रश्न किये। मैंने अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर दिये । मुनियों ने बताया कि आचार्यश्री के सामने अणुवत-आन्दोलन की भूमिका पर एक विचारणीय प्रश्न है । अणुव्रत में पाने वाले कुछ एक उद्योगपति अपने उद्योगों को शोषण-मुक्त बनाना चाहते हैं, पर अब तक उन्हें एक समुचित व्यवस्था इस दिशा में नहीं दीख रही है । लाभ-विभाजन का मान-दण्ड क्या हो, यह एक प्रश्न अणुवती नहीं सुलझा पा रहे हैं। इस दिशा में सन्तुलन बिठाने के लिए वे अपना लाभांश कम करने के लिए भी तैयार हैं।
मैंने अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से उत्तर दिया कि उद्योग-धन्धों से यदि लाभ नहीं होगा, तो हानि होगी। उद्योगधन्धों अथवा उत्पादन का तो प्रयोजन ही यह होता है कि उत्पादन में श्रम और व्यय के रूप में जितना मूल्य लगे उससे अधिक मूल्य का फल हो । सेर-भर गेहूँ बोकर सेर-भर गेहूँ पाने के लिए खेती नहीं की जाती। शोषण उद्योग-धन्धों से होने थाले लाभ के कारण नहीं होता, बल्कि वह लाभ एक व्यक्ति द्वारा ही हथिया लिया जाने के कारण या लाभ का वितरण सब श्रम करने वालों में समान रूप से न किया जाने के कारण होता है। अणुव्रती जनहित के विचार में उद्योग-धन्धे प्रारम्भ करें तो उनकी सफलता न्यूनतम व्यय और अधिक-से-अधिक उत्पादन में होगी। उन उद्योग-धन्धों द्वारा श्रमिकों को उचित जीविका देने के बाद भी यथेष्ट लाभ होना चाहिए, परन्तु वह लाभ किसी व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति नहीं, बल्कि श्रमिकों को ही सम्मिलित सम्पत्ति मानी जानी चाहिए। साधनों को कायम रखने और बढ़ाने के अतिरिक्त वह लाभ-धन उन उद्योग-धन्धों में लगे हुए श्रमिकों को शिक्षा, चिकित्सा तथा सांस्कृतिक सुविधाएं देने के लिए उपयोग किया जा मकता है। परन्तु उद्योग-धन्धों से लाभ अवश्य होना चाहिए; समाजवादी देशों में ऐसा ही किया जाता है।
मेरी बात से मुनियों का समाधान नहीं हुमा। उन्होंने कहा-जिस प्रणाली और व्यवस्था में लाभ का उद्देश्य रहेगा, उस ब्यवस्था से निश्चय ही शोषण होगा। वह व्यवस्था पोर प्रणाली अहिंसा और पारस्परिक सहयोग की नहीं हो सकेगी।
मैं मुनियों का समाधान नहीं कर सका; परन्तु इस बात से मुझे अवश्य सन्तोष प्रा कि प्रणवत-ग्रान्दोलन के अन्तर्गत गोषण-मुक्ति के प्रयोगों पर सोचा जा रहा है।
मैंने मुनिजी से अनुमति लेकर एक प्रश्न पूछा-आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ कर समाज-सेवा करना चाहते हैं; ऐसी अवस्था में आपका समाज और सामाजिक व्यवहार से पृथक् रहकर जीवन बिताना क्या तर्कसंगन और सहायक हो सकता है ? इसमें वैचित्र्य के अतिरिक्त कौन मार्थकता है ? इससे आपको अमुविधा ही तो होती होगी।
मुनिजी ने बहुत शान्ति से उत्तर दिया-हमें असुविधा हो, तो उसकी चिन्ता हमे होनी चाहिए। हमारे वेण प्रथवा कुछ व्यवहार प्रापको विचित्र लगे हैं, तो उन्हें हमारी व्यक्तिगत रुचि या विश्वास की बात समझ कर उमे महना चाहिए। हमारे जो प्रयत्न आपको समाज के लिए हितकारी जान पड़ते हैं, उनमें तो पाप सहयोगी बन ही सकते हैं।
मुनिजी की बात तर्कसंगत लगी। उनके चले जाने के बाद खयाल पाया कि यदि किसी की व्यक्तिगत रुचि और सन्तोष, समाज के लिए हानिकारक नहीं है, तो उनसे खिन्न होने की क्या जरूरत ? यदि मैं दिन-भर सिगरेट कंकते रहने की अपनी पादत को असामाजिक नहीं समझता, उस मादत को क्षमा कर सकता हूँ, तो जैन मुनियों के मुख पर कपड़ा रखने और हाथ में चंबर लेकर चलने की इच्छा से ही क्यों खिन्न हूँ? प्राचार्य तुलसी की प्रेरणा से अणुव्रत-यान्दोलन यदि प्राध्यात्मिक उन्नति के लिए उद्बोधन करता हा भी जनसाधारण के पार्थिव कष्टों को दूर करने और उन्हें मनुष्य की तरह जीवित रह सकने में भी योगभूत बनता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ।