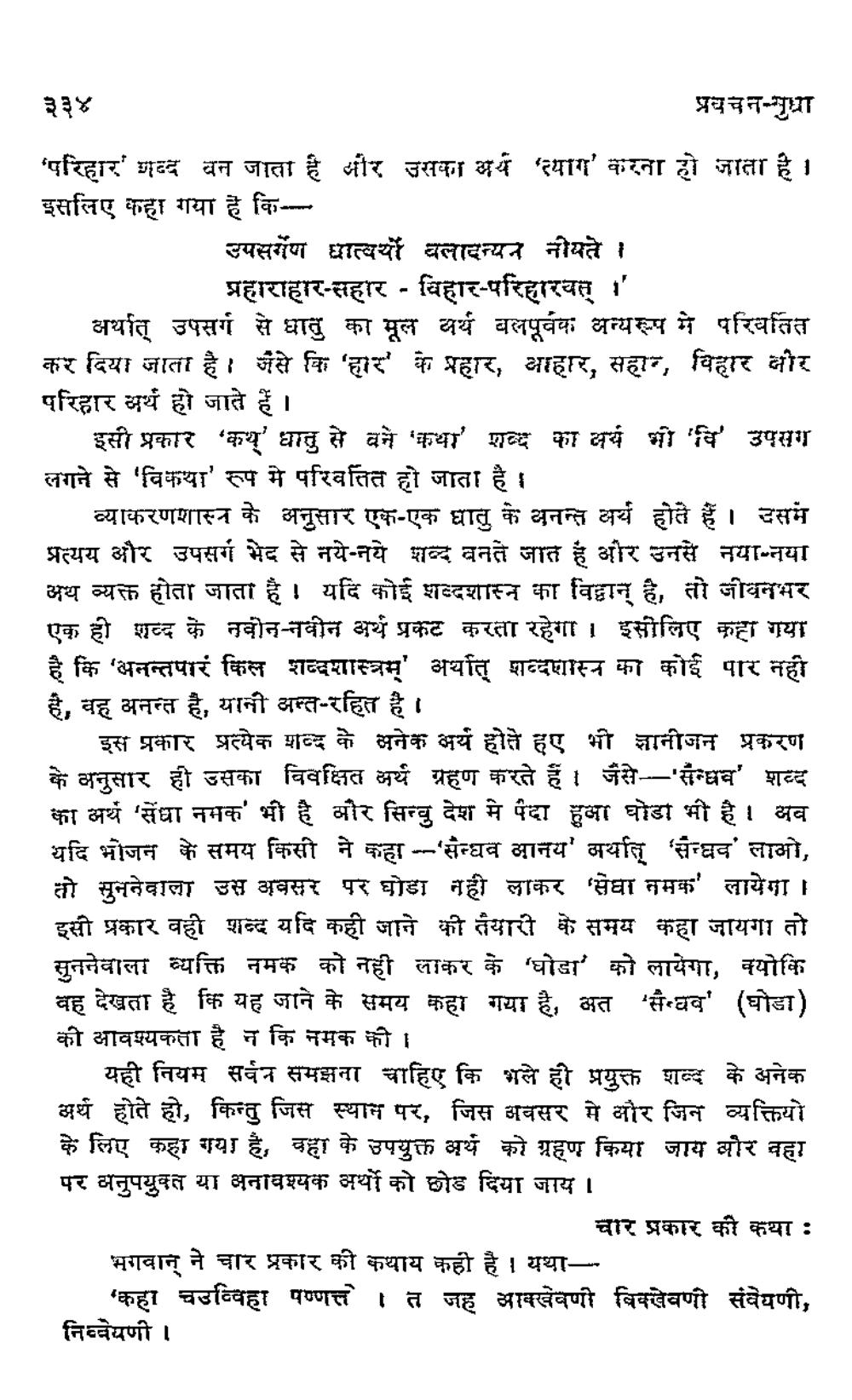________________
३३४
प्रवचन-सुधा
'परिहार' शब्द बन जाता है और उसका अर्थ 'त्याग' करना हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि---
उपसर्गेण धात्वयों बलादन्यन नीयते ।
प्रहाराहार-सहार - विहार-परिहारवत् ।' अर्थात् उपसर्ग से धातु का मूल अर्थ बलपूर्वक अन्यरूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि 'हार' के प्रहार, आहार, सहार, विहार और परिहार अर्थ हो जाते हैं।
__ इसी प्रकार 'कथ्' धातु से बने 'कथा' शब्द का अर्थ भी वि' उपसग लगने से 'विकथा' रूप में परिवर्तित हो जाता है।
व्याकरणशास्त्र के अनुसार एक-एक धातु के अनन्त अर्थ होते हैं। इसमें प्रत्यय और उपसर्ग भेद से नये-नये शब्द बनते जात है और उनसे नया-नया अथ व्यक्त होता जाता है। यदि कोई शब्दशास्न का विद्वान् है, तो जीवनभर एक ही शब्द के नवीन-नवीन अर्थ प्रकट करता रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि 'अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रम्' अर्थात् शब्दशास्त्र का कोई पार नहीं है, वह अनन्त है, यानी अन्त-रहित है।
इस प्रकार प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ होते हए भी ज्ञानीजन प्रकरण के अनुसार ही उसका विवक्षित अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे-'सैन्धव' शब्द का अर्थ 'सेंधा नमक' भी है और सिन्वु देश मे पैदा हुआ घोडा भी है। अब यदि भोजन के समय किसी ने कहा --'सैन्धव आनय' अर्थात् 'सन्धव लामो, तो सुननेवाला उस अवसर पर घोडा नहीं लाकर 'सेंधा नमक' लायेगा। इसी प्रकार वही शब्द यदि कही जाने की तैयारी के समय कहा जायगा तो सुननेवाला व्यक्ति नमक को नहीं लाकर के 'घोडा' को लायेगा, क्योकि वह देखता है कि यह जाने के समय कहा गया है, अत 'सैन्धव' (घोडा) की आवश्यकता है न कि नमक की।
यही नियम सर्वन समझना चाहिए कि भले ही प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ होते हो, किन्तु जिस स्थान पर, जिस अवसर मे और जिन व्यक्तियो के लिए कहा गया है, वहा के उपयुक्त अर्थ को ग्रहण किया जाय और वहा पर अनुपयुक्त या अनावश्यक अर्थो को छोड दिया जाय ।
चार प्रकार की कथा : भगवान् ने चार प्रकार की कथाय कही है । यथा--
'कहा चउन्विहा पण्णत्ते । त जह आक्खेवणी विक्खेवणी संवेयणी, निन्वेयणी।