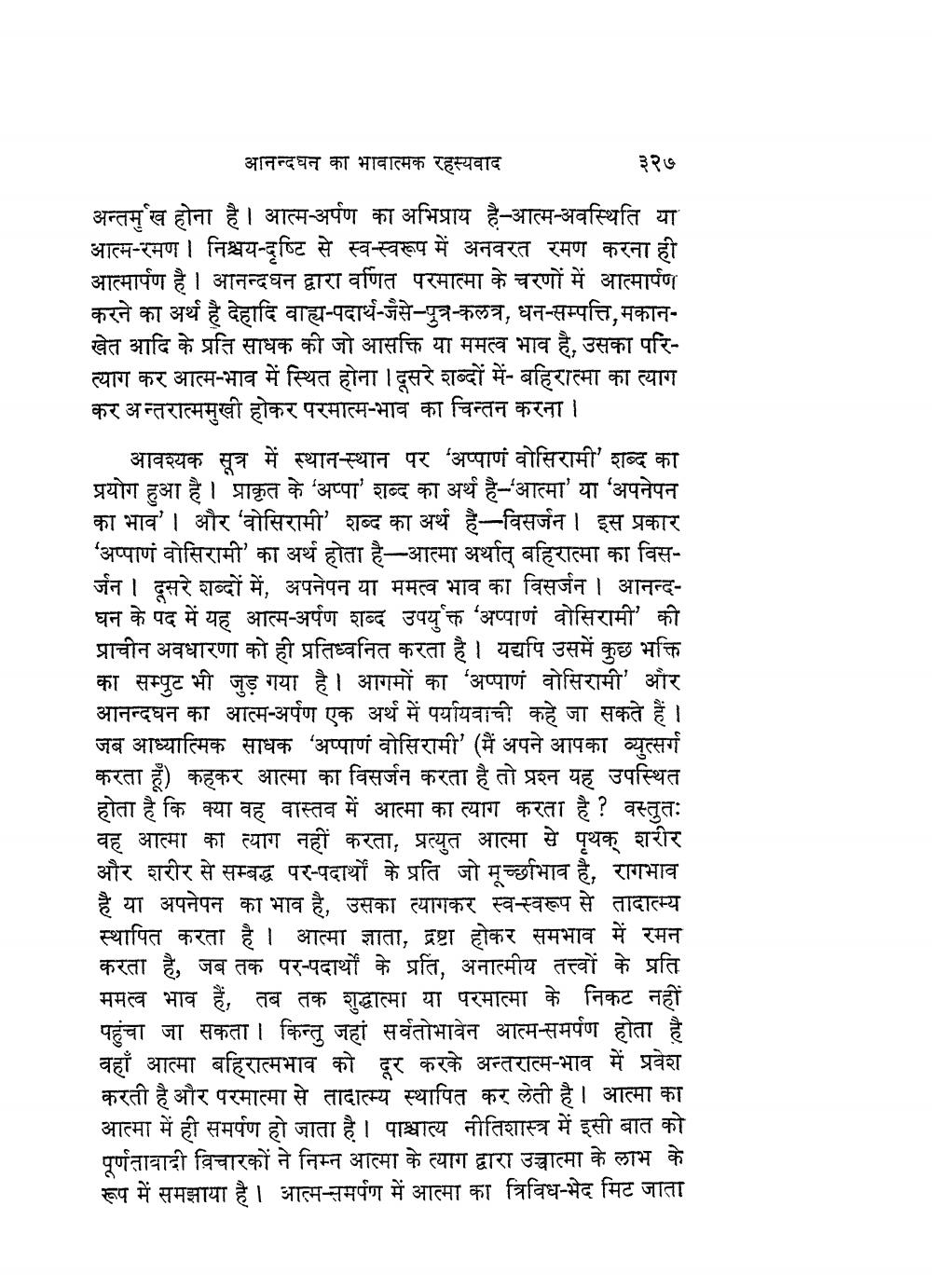________________
आनन्दघन का भावात्मक रहस्यवाद
३२७
अन्तर्मुख होना है। आत्म-अर्पण का अभिप्राय है-आत्म-अवस्थिति या आत्म-रमण । निश्चय-दृष्टि से स्व-स्वरूप में अनवरत रमण करना ही आत्मार्पण है । आनन्दघन द्वारा वर्णित परमात्मा के चरणों में आत्मार्पण करने का अर्थ है देहादि बाह्य-पदार्थ-जैसे-पुत्र-कलत्र, धन-सम्पत्ति,मकानखेत आदि के प्रति साधक की जो आसक्ति या ममत्व भाव है, उसका परित्याग कर आत्म-भाव में स्थित होना । दूसरे शब्दों में- बहिरात्मा का त्याग कर अन्तरात्ममुखी होकर परमात्म-भाव का चिन्तन करना।
आवश्यक सूत्र में स्थान-स्थान पर 'अप्पाणं वोसिरामी' शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राकृत के 'अप्पा' शब्द का अर्थ है-'आत्मा' या 'अपनेपन का भाव' । और 'वोसिरामी' शब्द का अर्थ है-विसर्जन । इस प्रकार 'अप्पाणं वोसिरामी' का अर्थ होता है-आत्मा अर्थात् बहिरात्मा का विसर्जन । दूसरे शब्दों में, अपनेपन या ममत्व भाव का विसर्जन । आनन्दघन के पद में यह आत्म-अर्पण शब्द उपर्युक्त 'अप्पाणं वोसिरामी' की प्राचीन अवधारणा को ही प्रतिध्वनित करता है। यद्यपि उसमें कुछ भक्ति का सम्पुट भी जुड़ गया है। आगमों का 'अप्पाणं वोसिरामी' और आनन्दघन का आत्म-अर्पण एक अर्थ में पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। जब आध्यात्मिक साधक 'अप्पाणं वोसिरामी' (मैं अपने आपका व्युत्सर्ग करता हूँ) कहकर आत्मा का विसर्जन करता है तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या वह वास्तव में आत्मा का त्याग करता है ? वस्तुतः वह आत्मा का त्याग नहीं करता, प्रत्युत आत्मा से पृथक् शरीर और शरीर से सम्बद्ध पर-पदार्थों के प्रति जो मूर्छाभाव है, रागभाव है या अपनेपन का भाव है, उसका त्यागकर स्व-स्वरूप से तादात्म्य स्थापित करता है। आत्मा ज्ञाता, द्रष्टा होकर समभाव में रमन करता है, जब तक पर-पदार्थों के प्रति, अनात्मीय तत्त्वों के प्रति ममत्व भाव हैं, तब तक शुद्धात्मा या परमात्मा के निकट नहीं पहुंचा जा सकता। किन्तु जहां सर्वतोभावेन आत्म-समर्पण होता है वहाँ आत्मा बहिरात्मभाव को दूर करके अन्तरात्म-भाव में प्रवेश करती है और परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। आत्मा का आत्मा में ही समर्पण हो जाता है। पाश्चात्य नीतिशास्त्र में इसी बात को पूर्णतावादी विचारकों ने निम्न आत्मा के त्याग द्वारा उच्चात्मा के लाभ के रूप में समझाया है। आत्म-समर्पण में आत्मा का त्रिविध-भेद मिट जाता