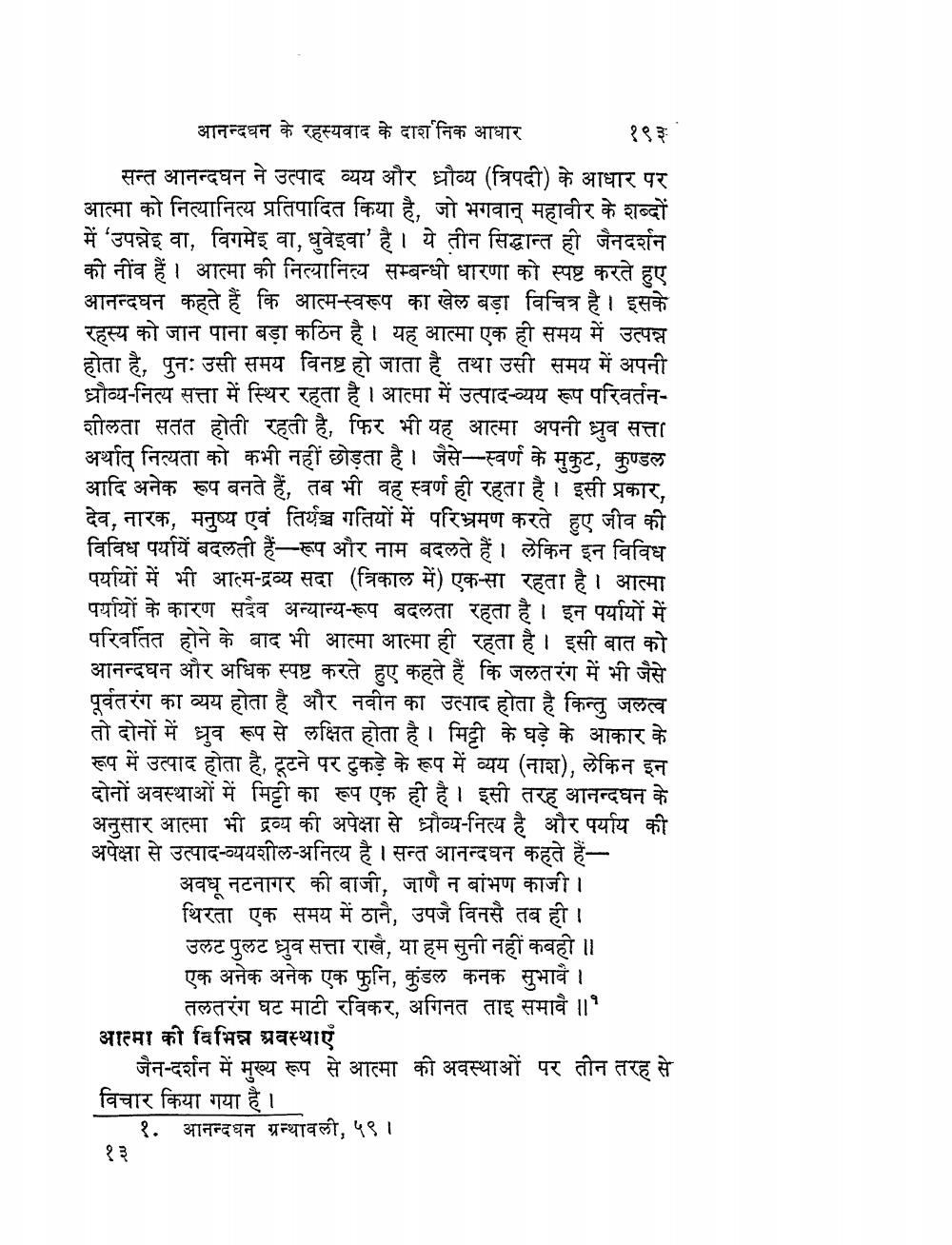________________
आनन्दघन के रहस्यवाद के दार्शनिक आधार
१९३
सन्त आनन्दघन ने उत्पाद व्यय और ध्रौव्य (त्रिपदी) के आधार पर आत्मा को नित्यानित्य प्रतिपादित किया है, जो भगवान् महावीर के शब्दों में 'उपन्नेइ वा, विगमेइ वा, धुवेइवा' है । ये तीन सिद्धान्त हो जैनदर्शन की नींव हैं । आत्मा की नित्यानित्व सम्बन्धी धारणा को स्पष्ट करते हुए आनन्दघन कहते हैं कि आत्म-स्वरूप का खेल बड़ा विचित्र है । इसके रहस्य को जान पाना बड़ा कठिन है । यह आत्मा एक ही समय में उत्पन्न होता है, पुनः उसी समय विनष्ट हो जाता है तथा उसी समय में अपनी star for सत्ता में स्थिर रहता है । आत्मा में उत्पाद व्यय रूप परिवर्तनशीलता सतत होती रहती है, फिर भी यह आत्मा अपनी ध्रुव सत्ता अर्थात् नित्यता को कभी नहीं छोड़ता है । जैसे—– स्वर्ण के मुकुट, कुण्डल आदि अनेक रूप बनते हैं, तब भी वह स्वर्ण ही रहता है । इसी प्रकार, देव, नारक, मनुष्य एवं तिर्यञ्च गतियों में परिभ्रमण करते हुए जीव की विविध पर्यायें बदलती हैं—रूप और नाम बदलते हैं । लेकिन इन विविध पर्यायों में भी आत्म-द्रव्य सदा ( त्रिकाल में) एक-सा रहता है । आत्मा पर्यायों के कारण सदैव अन्यान्य रूप बदलता रहता है । इन पर्यायों में परिवर्तित होने के बाद भी आत्मा आत्मा ही रहता है । इसी बात को आनन्दघन और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते कि जलतरंग में भी जैसे पूर्वतरंग का व्यय होता है और नवीन का उत्पाद होता है किन्तु जलत्व तो दोनों में ध्रुव रूप से लक्षित होता है । मिट्टी के घड़े के आकार के रूप में उत्पाद होता है, टूटने पर टुकड़े के रूप में व्यय ( नाश), लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में मिट्टी का रूप एक ही है। इसी तरह आनन्दघन के अनुसार आत्मा भी द्रव्य की अपेक्षा से धौव्य नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद व्ययशील - अनित्य है । सन्त आनन्दघन कहते हैं
हैं
अवधू नटनागर की बाजी, जाणै न बांभण काजी । थिरता एक समय में ठाने, उपजै विनसै तब ही । उलट पुलट ध्रुव सत्ता राखै, या हम सुनी नहीं कबही ॥ एक अनेक अनेक एक फुनि, कुंडल कनक सुभावें । तलतरंग घट माटी रविकर, अगिनत ताइ समावै ॥ आत्मा की विभिन्न अवस्थाएँ
जैन-दर्शन में मुख्य रूप से आत्मा की अवस्थाओं पर तीन तरह से
विचार किया गया है ।
१.
१३
आनन्दघन ग्रन्थावली, ५९ ।