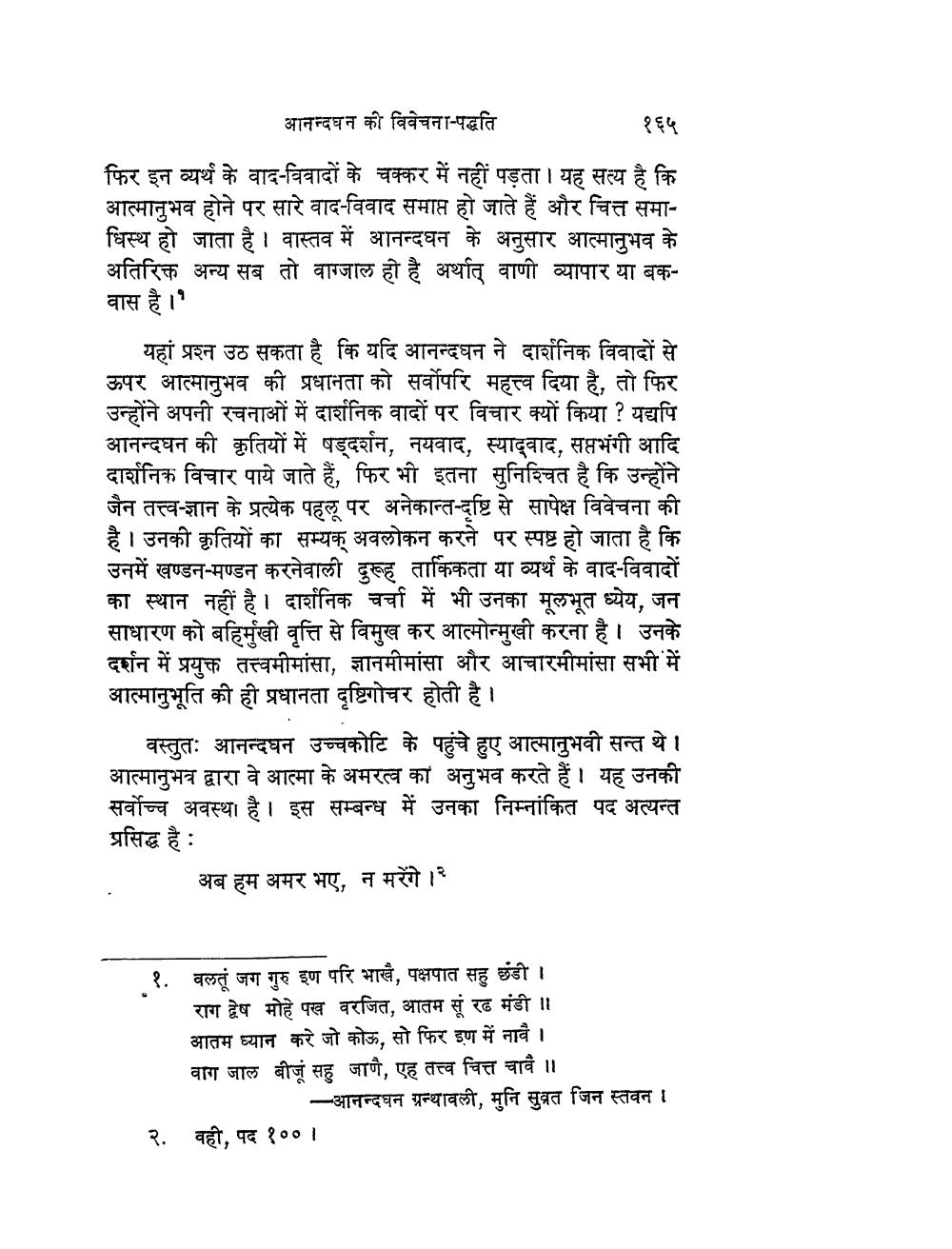________________
आनन्दघन की विवेचना-पद्धति
१६५
फिर इन व्यर्थ के वाद-विवादों के चक्कर में नहीं पड़ता। यह सत्य है कि आत्मानुभव होने पर सारे वाद-विवाद समाप्त हो जाते हैं और चित्त समाधिस्थ हो जाता है। वास्तव में आनन्दघन के अनुसार आत्मानुभव के अतिरिक्त अन्य सब तो वाग्जाल ही है अर्थात् वाणी व्यापार या बकवास है।
यहां प्रश्न उठ सकता है कि यदि आनन्दघन ने दार्शनिक विवादों से ऊपर आत्मानुभव की प्रधानता को सर्वोपरि महत्त्व दिया है, तो फिर उन्होंने अपनी रचनाओं में दार्शनिक वादों पर विचार क्यों किया ? यद्यपि आनन्दघन की कृतियों में षड्दर्शन, नयवाद, स्याद्वाद, सप्तभंगी आदि दार्शनिक विचार पाये जाते हैं, फिर भी इतना सुनिश्चित है कि उन्होंने जैन तत्त्व-ज्ञान के प्रत्येक पहलू पर अनेकान्त-दृष्टि से सापेक्ष विवेचना की है। उनकी कृतियों का सम्यक् अवलोकन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उनमें खण्डन-मण्डन करनेवाली दुरूह तार्किकता या व्यर्थ के वाद-विवादों का स्थान नहीं है। दार्शनिक चर्चा में भी उनका मूलभूत ध्येय, जन साधारण को बहिर्मुखी वृत्ति से विमुख कर आत्मोन्मुखी करना है। उनके दर्शन में प्रयुक्त तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा और आचारमीमांसा सभी में आत्मानुभूति की ही प्रधानता दृष्टिगोचर होती है।
वस्तुतः आनन्दघन उच्चकोटि के पहुंचे हुए आत्मानुभवी सन्त थे। आत्मानुभव द्वारा वे आत्मा के अमरत्व का अनुभव करते हैं। यह उनकी सर्वोच्च अवस्था है। इस सम्बन्ध में उनका निम्नांकित पद अत्यन्त प्रसिद्ध है :
अब हम अमर भए, न मरेंगे।'
१. वलतूं जग गुरु इण परि भाख, पक्षपात सहु छंडी।
राग द्वेष मोहे पख वरजित, आतम सूं रढ मंडी ॥ आतम ध्यान करे जो कोऊ, सो फिर इण में नावै । वाग जाल बीजूं सहु जाणे, एह तत्त्व चित्त चावै ॥
-आनन्दघन ग्रन्थावली, मुनि सुव्रत जिन स्तवन । २. वही, पद १००।