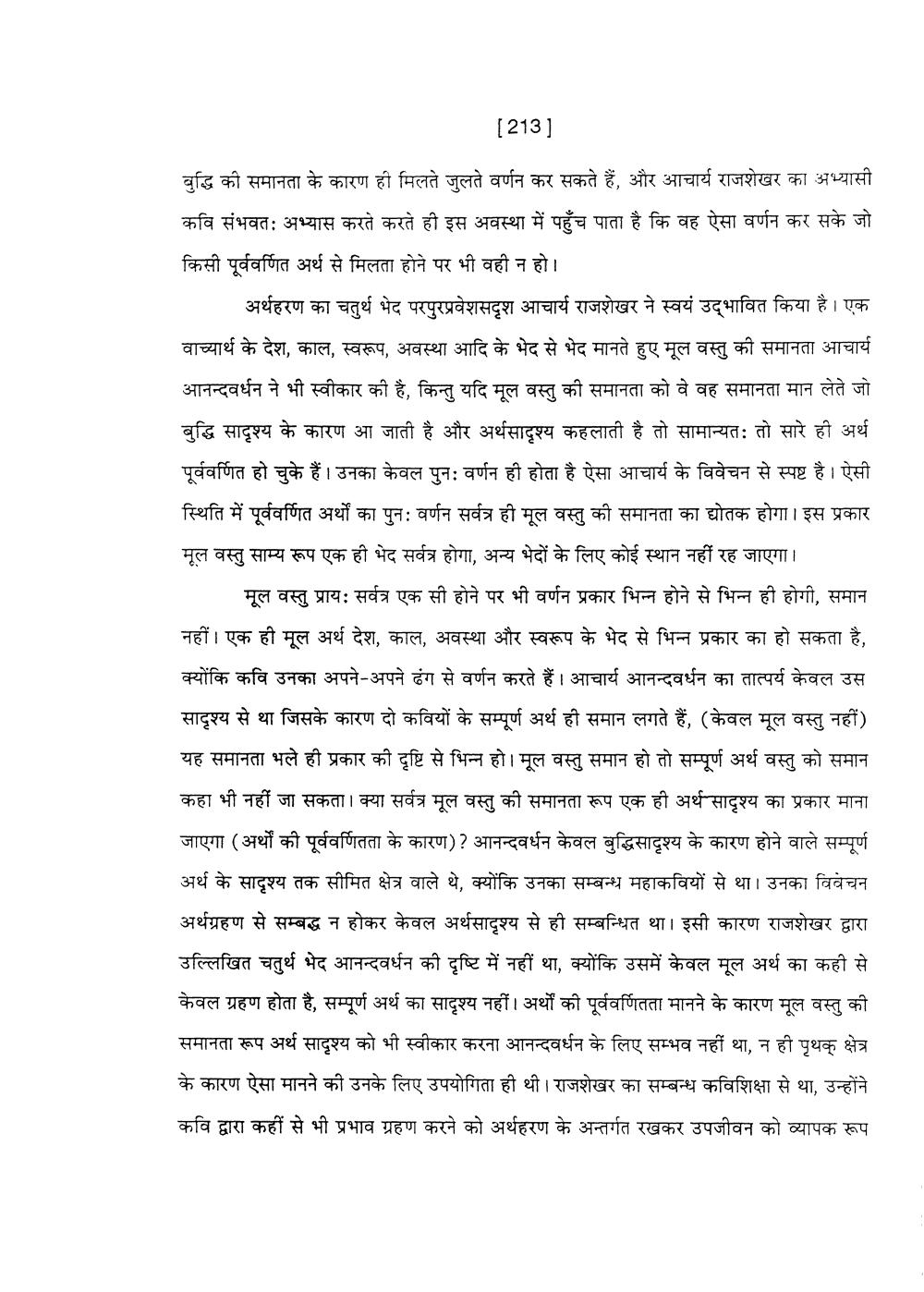________________
[213]
बुद्धि की समानता के कारण ही मिलते जुलते वर्णन कर सकते हैं, और आचार्य राजशेखर का अभ्यासी कवि संभवतः अभ्यास करते करते ही इस अवस्था में पहुँच पाता है कि वह ऐसा वर्णन कर सके जो किसी पूर्ववर्णित अर्थ से मिलता होने पर भी वही न हो।
अर्थहरण का चतुर्थ भेद परपुरप्रवेशसदृश आचार्य राजशेखर ने स्वयं उद्भावित किया है। एक वाच्यार्थ के देश, काल, स्वरूप, अवस्था आदि के भेद से भेद मानते हुए मूल वस्तु की समानता आचार्य आनन्दवर्धन ने भी स्वीकार की हैं, किन्तु यदि मूल वस्तु की समानता को वे वह समानता मान लेते जो बुद्धि सादृश्य के कारण आ जाती है और अर्थसादृश्य कहलाती है तो सामान्यतः तो सारे ही अर्थ पूर्ववर्णित हो चुके हैं। उनका केवल पुनः वर्णन ही होता है ऐसा आचार्य के विवेचन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में पूर्ववर्णित अर्थों का पुनः वर्णन सर्वत्र ही मूल वस्तु की समानता का द्योतक होगा। इस प्रकार मूल वस्तु साम्य रूप एक ही भेद सर्वत्र होगा, अन्य भेदों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा।
मूल वस्तु प्राय: सर्वत्र एक सी होने पर भी वर्णन प्रकार भिन्न होने से भिन्न ही होगी, समान नहीं। एक ही मूल अर्थ देश, काल, अवस्था और स्वरूप के भेद से भिन्न प्रकार का हो सकता है, क्योंकि कवि उनका अपने-अपने ढंग से वर्णन करते हैं। आचार्य आनन्दवर्धन का तात्पर्य केवल उस सादृश्य से था जिसके कारण दो कवियों के सम्पूर्ण अर्थ ही समान लगते हैं, (केवल मूल वस्तु नहीं) यह समानता भले ही प्रकार की दृष्टि से भिन्न हो। मूल वस्तु समान हो तो सम्पूर्ण अर्थ वस्तु को समान कहा भी नहीं जा सकता। क्या सर्वत्र मूल वस्तु की समानता रूप एक ही अर्थ सादृश्य का प्रकार माना जाएगा (अर्थों की पूर्ववर्णितता के कारण ) ? आनन्दवर्धन केवल बुद्धिसादृश्य के कारण होने वाले सम्पूर्ण अर्थ के सादृश्य तक सीमित क्षेत्र वाले थे, क्योंकि उनका सम्बन्ध महाकवियों से था उनका विवेचन अर्थग्रहण से सम्बद्ध न होकर केवल अर्थसादृश्य से ही सम्बन्धित था। इसी कारण राजशेखर द्वारा उल्लिखित चतुर्थ भेद आनन्दवर्धन की दृष्टि में नहीं था, क्योंकि उसमें केवल मूल अर्थ का कही से केवल ग्रहण होता है, सम्पूर्ण अर्थ का सादृश्य नहीं। अर्थों की पूर्ववर्णितता मानने के कारण मूल वस्तु की समानता रूप अर्थ सादृश्य को भी स्वीकार करना आनन्दवर्धन के लिए सम्भव नहीं था, न ही पृथक् क्षेत्र के कारण ऐसा मानने की उनके लिए उपयोगिता ही थी। राजशेखर का सम्बन्ध कविशिक्षा से था, उन्होंने कवि द्वारा कहीं से भी प्रभाव ग्रहण करने को अर्थहरण के अन्तर्गत रखकर उपजीवन को व्यापक रूप