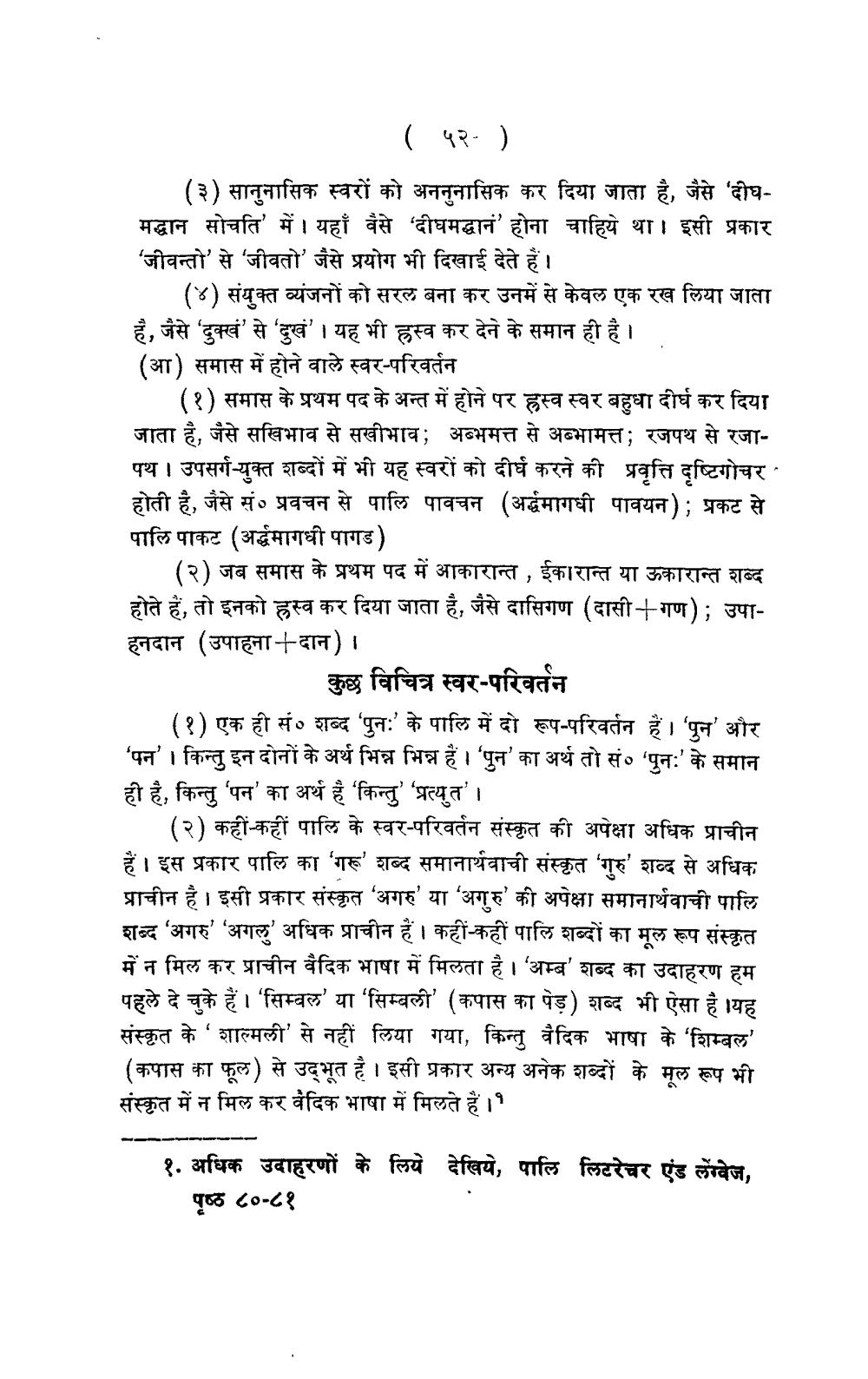________________
( ५२. ) (३) सानुनासिक स्वरों को अननुनासिक कर दिया जाता है, जैसे 'दीघमद्धान सोचति' में। यहाँ वैसे 'दीघमद्धानं' होना चाहिये था। इसी प्रकार 'जीवन्तो' से 'जीवतो' जैसे प्रयोग भी दिखाई देते हैं।
(४) संयुक्त व्यंजनों को सरल बना कर उनमें से केवल एक रख लिया जाता है, जैसे 'दुक्खं' से 'दुखं'। यह भी ह्रस्व कर देने के समान ही है। (आ) समास में होने वाले स्वर-परिवर्तन
(१) समास के प्रथम पद के अन्त में होने पर ह्रस्व स्वर बहुधा दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे सखिभाव से सखीभाव; अब्भमत्त से अब्भामत्त; रजपथ से रजापथ । उपसर्ग-युक्त शब्दों में भी यह स्वरों को दीर्घ करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, जैसे सं० प्रवचन से पालि पावचन (अर्द्धमागधी पावयन); प्रकट से पालि पाकट (अर्द्धमागधी पागड)
(२) जब समास के प्रथम पद में आकारान्त , ईकारान्त या ऊकारान्त शब्द होते हैं, तो इनको ह्रस्व कर दिया जाता है, जैसे दासिगण (दासी+गण); उपाहनदान (उपाहना+दान)।
कुछ विचित्र स्वर-परिवर्तन (१) एक ही सं० शब्द 'पुनः' के पालि में दो रूप-परिवर्तन हैं। 'पून' और 'पन' । किन्तु इन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं । 'पुन' का अर्थ तो सं० 'पुनः' के समान ही है, किन्तु ‘पन' का अर्थ है किन्तु' 'प्रत्युत'।
(२) कहीं-कहीं पालि के स्वर-परिवर्तन संस्कृत की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं। इस प्रकार पालि का 'गरू' शब्द समानार्थवाची संस्कृत 'गुरु' शब्द से अधिक प्राचीन है। इसी प्रकार संस्कृत 'अगरु' या 'अगुरु' की अपेक्षा समानार्थवाची पालि शब्द 'अगरु' 'अगलु' अधिक प्राचीन हैं। कहीं-कहीं पालि शब्दों का मूल रूप संस्कृत में न मिल कर प्राचीन वैदिक भाषा में मिलता है। 'अम्ब' शब्द का उदाहरण हम पहले दे चुके हैं। 'सिम्बल' या 'सिम्बली' (कपास का पेड़) शब्द भी ऐसा है यह संस्कृत के ' शाल्मली' से नहीं लिया गया, किन्तु वैदिक भाषा के 'शिम्बल' (कपास का फूल) से उद्भूत है । इसी प्रकार अन्य अनेक शब्दों के मूल रूप भी संस्कृत में न मिल कर वैदिक भाषा में मिलते हैं।'
१. अधिक उदाहरणों के लिये देखिये, पालि लिटरेचर एंड लेंग्वेज,
पृष्ठ ८०-८१