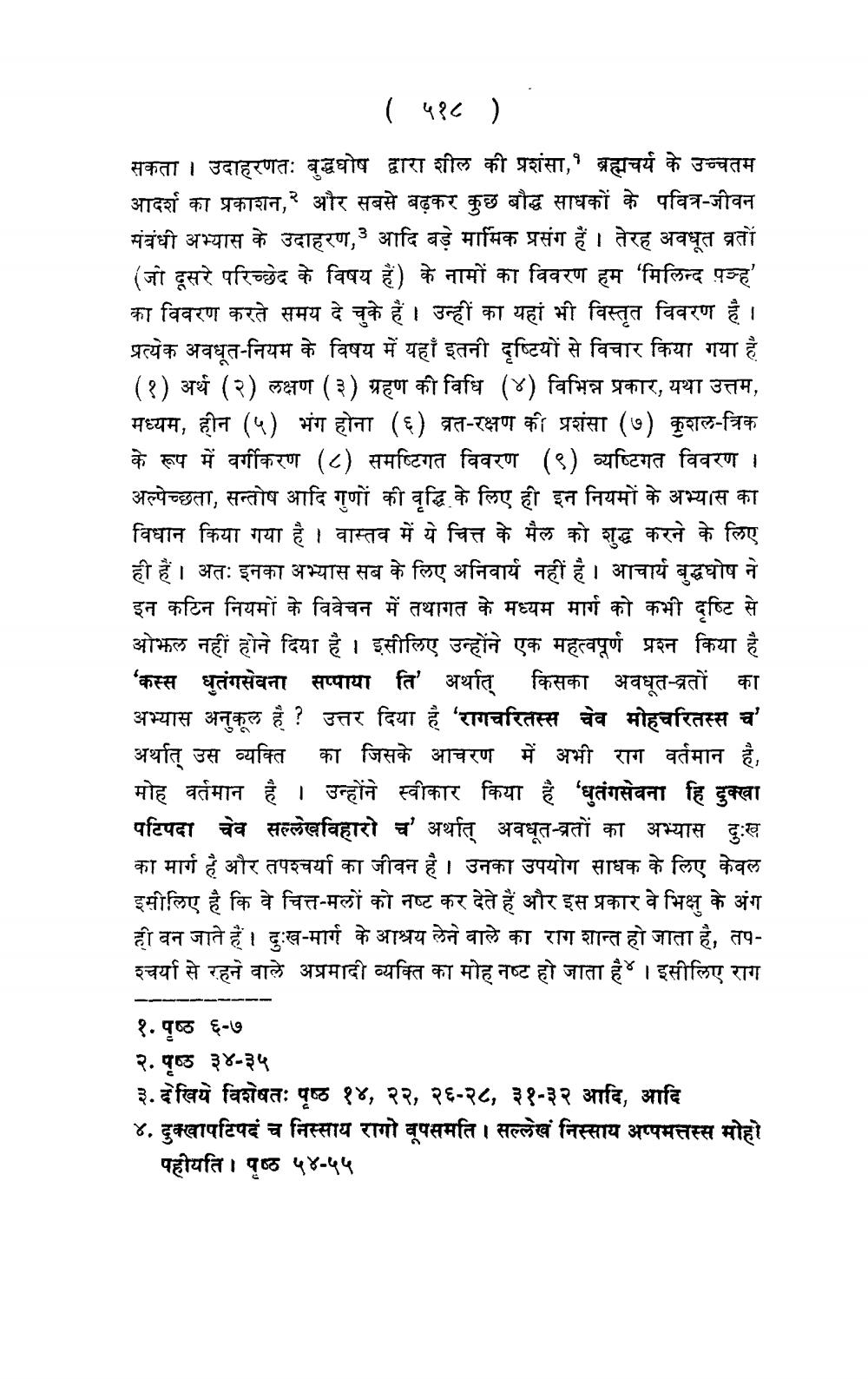________________
( ५१८ ) सकता। उदाहरणतः बुद्धघोष द्वारा शील की प्रशंसा,' ब्रह्मचर्य के उच्चतम आदर्श का प्रकाशन,२ और सबसे बढ़कर कुछ बौद्ध साधकों के पवित्र-जीवन संबंधी अभ्यास के उदाहरण, आदि बड़े मार्मिक प्रसंग हैं। तेरह अवधूत व्रतों (जो दूसरे परिच्छेद के विषय हैं) के नामों का विवरण हम 'मिलिन्द पन्ह' का विवरण करते समय दे चुके हैं। उन्हीं का यहां भी विस्तृत विवरण है । प्रत्येक अवधूत-नियम के विषय में यहाँ इतनी दृष्टियों से विचार किया गया है (१) अर्थ (२) लक्षण (३) ग्रहण की विधि (४) विभिन्न प्रकार, यथा उत्तम, मध्यम, हीन (५) भंग होना (६) व्रत-रक्षण की प्रशंसा (७) कुशल-त्रिक के रूप में वर्गीकरण (८) समष्टिगत विवरण (९) व्यष्टिगत विवरण । अल्पेच्छता, सन्तोष आदि गुणों की वृद्धि के लिए ही इन नियमों के अभ्यास का विधान किया गया है। वास्तव में ये चित्त के मैल को शुद्ध करने के लिए ही हैं। अतः इनका अभ्यास सब के लिए अनिवार्य नहीं है। आचार्य बुद्धघोष ने इन कटिन नियमों के विवेचन में तथागत के मध्यम मार्ग को कभी दृष्टि से
ओझल नहीं होने दिया है । इसीलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है 'कस्स धुतंगसेवना सप्पाया ति' अर्थात् किसका अवधूत-व्रतों का अभ्यास अनुकूल है ? उत्तर दिया है 'रागचरितस्स चेव मोहचरितस्स च' अर्थात् उस व्यक्ति का जिसके आचरण में अभी राग वर्तमान है, मोह वर्तमान है । उन्होंने स्वीकार किया है 'धुतंगसेवना हि दुक्खा पटिपदा चेव सल्लेखविहारो च' अर्थात् अवधूत-व्रतों का अभ्यास दुःख का मार्ग है और तपश्चर्या का जीवन है। उनका उपयोग साधक के लिए केवल इसीलिए है कि वे चित्त-मलों को नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार वे भिक्षु के अंग ही बन जाते हैं। दुःख-मार्ग के आश्रय लेने वाले का राग शान्त हो जाता है, तपश्चर्या से रहने वाले अप्रमादी व्यक्ति का मोह नष्ट हो जाता है । इसीलिए राग
१. पृष्ठ ६-७ २. पृष्ठ ३४-३५ ३. देखिये विशेषतः पृष्ठ १४, २२, २६-२८, ३१-३२ आदि, आदि ४. दुक्खापटिपदं च निस्साय रागो वूपसमति । सल्लेखं निस्साय अप्पमत्तस्स मोहो
पहीयति। पृष्ठ ५४-५५