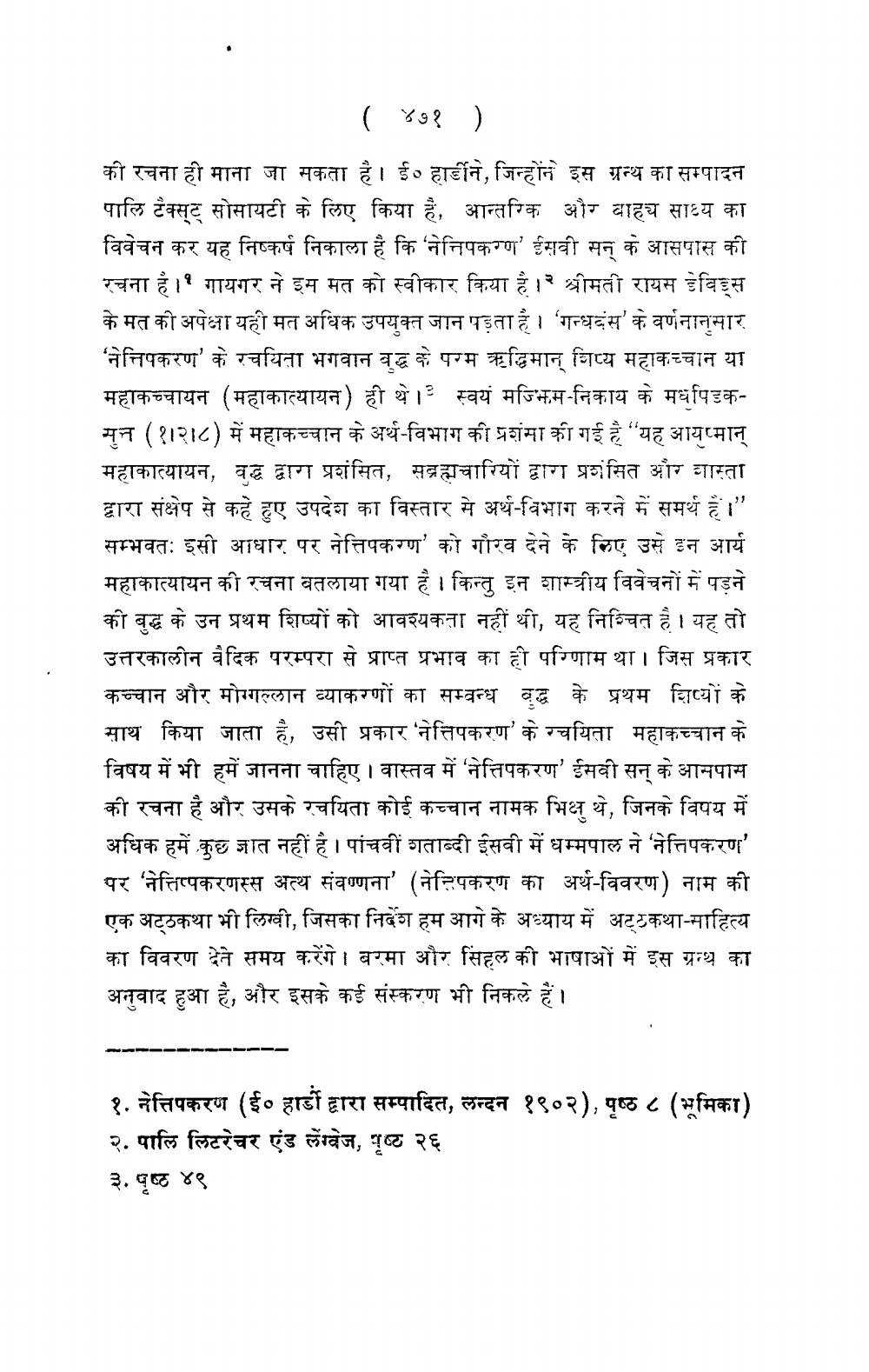________________
( ४७१ )
की रचना ही माना जा सकता है। ई० हार्डीने, जिन्होंने इस ग्रन्थ का सम्पादन पालि टैक्स्ट सोसायटी के लिए किया है, आन्तरिक और बाहय साध्य का विवेचन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि 'नेतिपकरण' ईसवी सन के आसपास की रचना है।' गायगर ने इस मत को स्वीकार किया है। श्रीमती रायस डेविड्स के मत की अपेक्षा यही मत अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। ‘गन्धवंस' के वर्णनानुसार 'नेनिपकरण' के रचयिता भगवान बुद्ध के परम ऋद्धिमान् गिप्य महाकच्चान या महाकच्चायन (महाकात्यायन) ही थे। स्वयं मज्झिम-निकाय के मधपिङकमुन (१।२।८) में महाकच्चान के अर्थ-विभाग की प्रशंमा की गई है “यह आयप्मान् महाकात्यायन, वृद्ध द्वारा प्रशंसित, सब्रह्मचारियों द्वारा प्रमंसित और गास्ता द्वारा संक्षेप से कहे हुए उपदेश का विस्तार से अर्थ-विभाग करने में समर्थ हैं।" सम्भवतः इसी आधार पर नेत्तिपकरण' को गौरव देने के लिए उसे इन आर्य महाकात्यायन की रचना वतलाया गया है। किन्तु इन शास्त्रीय विवेचनों में पड़ने की बुद्ध के उन प्रथम शिष्यों को आवश्यकता नहीं थी, यह निश्चित है । यह तो उत्तरकालीन वैदिक परम्परा से प्राप्त प्रभाव का ही परिणाम था। जिस प्रकार कच्चान और मोग्गल्लान व्याकरणों का सम्बन्ध बुद्ध के प्रथम शिष्यों के माथ किया जाता है, उसी प्रकार 'नेत्तिपकरण' के रचयिता महाकच्चान के विषय में भी हमें जानना चाहिए। वास्तव में नेत्तिपकरण' ईसवी सन् के आसपास की रचना है और उसके रचयिता कोई कच्चान नामक भिक्षु थे, जिनके विषय में अधिक हमें कुछ ज्ञात नहीं है। पांचवीं शताब्दी ईसवी में धम्मपाल ने 'नेत्तिपकरण' पर 'नेत्तिप्पकरणस्स अत्थ संवण्णना' (नेनिपकरण का अर्थ-विवरण) नाम की एक अट्ठकथा भी लिग्वी, जिसका निर्देश हम आगे के अध्याय में अट्ठकथा-माहित्य का विवरण देते समय करेंगे। बरमा और सिंहल की भाषाओं में इस ग्रन्थ का अनुवाद हुआ है, और इसके कई संस्करण भी निकले हैं।
१. नेत्तिपकरण (ई० हार्डी द्वारा सम्पादित, लन्दन १९०२), पृष्ठ ८ (भूमिका) २. पालि लिटरेचर एंड लेंग्वेज, पृष्ठ २६ ३. पृष्ठ ४९