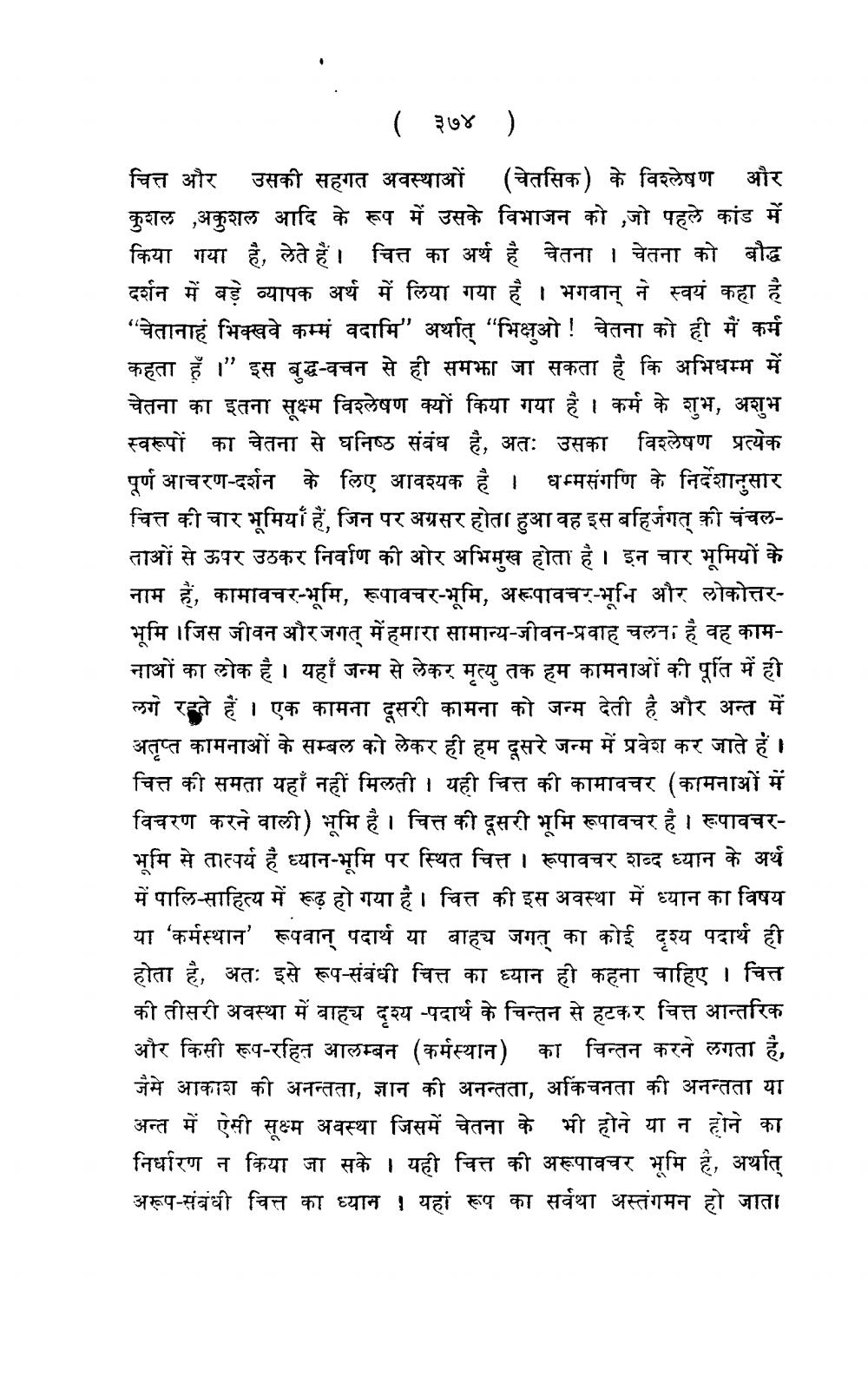________________
( ३७४ )
चित्त और उसकी सहगत अवस्थाओं (चेतसिक) के विश्लेषण और कुशल ,अकुशल आदि के रूप में उसके विभाजन को ,जो पहले कांड में किया गया है, लेते हैं। चित्त का अर्थ है चेतना । चेतना को बौद्ध दर्शन में बड़े व्यापक अर्थ में लिया गया है । भगवान् ने स्वयं कहा है "चेतानाहं भिक्खवे कम्मं वदामि" अर्थात् “भिक्षुओ! चेतना को ही मैं कर्म कहता हूँ ।" इस बुद्ध-वचन से ही समझा जा सकता है कि अभिधम्म में चेतना का इतना सूक्ष्म विश्लेषण क्यों किया गया है। कर्म के शुभ, अशुभ स्वरूपों का चेतना से घनिष्ठ संबंध है, अतः उसका विश्लेषण प्रत्येक पूर्ण आचरण-दर्शन के लिए आवश्यक है । धम्मसंगणि के निर्देशानुसार चित्त की चार भूमियाँ हैं, जिन पर अग्रसर होता हुआ वह इस बहिर्जगत् की चंचलताओं से ऊपर उठकर निर्वाण की ओर अभिमुख होता है। इन चार भूमियों के नाम हैं, कामावचर-भूमि, रूपावचर-भूमि, अरूपावचर-भूनि और लोकोत्तरभूमि ।जिस जीवन और जगत् में हमारा सामान्य-जीवन-प्रवाह चलना है वह कामनाओं का लोक है। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं । एक कामना दूसरी कामना को जन्म देती है और अन्त में अतृप्त कामनाओं के सम्बल को लेकर ही हम दूसरे जन्म में प्रवेश कर जाते हैं। चित्त की समता यहाँ नहीं मिलती। यही चित्त की कामावचर (कामनाओं में विचरण करने वाली) भूमि है। चित्त की दूसरी भूमि रूपावचर है । रूपावचरभूमि से तात्पर्य है ध्यान-भूमि पर स्थित चित्त । रूपावचर शब्द ध्यान के अर्थ में पालि-साहित्य में रूढ़ हो गया है। चित्त की इस अवस्था में ध्यान का विषय या 'कर्मस्थान' रूपवान् पदार्थ या बाह्य जगत् का कोई दृश्य पदार्थ ही होता है, अतः इसे रूप-संबंधी चित्त का ध्यान ही कहना चाहिए । चित्त की तीसरी अवस्था में बाह्य दृश्य -पदार्थ के चिन्तन से हटकर चित्त आन्तरिक और किसी रूप-रहित आलम्बन (कर्मस्थान) का चिन्तन करने लगता है, जैसे आकाश की अनन्तता, ज्ञान की अनन्तता, अकिंचनता की अनन्तता या अन्त में ऐसी सूक्ष्म अवस्था जिसमें चेतना के भी होने या न होने का निर्धारण न किया जा सके । यही चित्त की अरूपावचर भूमि है, अर्थात् अरूप-संबंधी चित्त का ध्यान ! यहां रूप का सर्वथा अस्तंगमन हो जाता