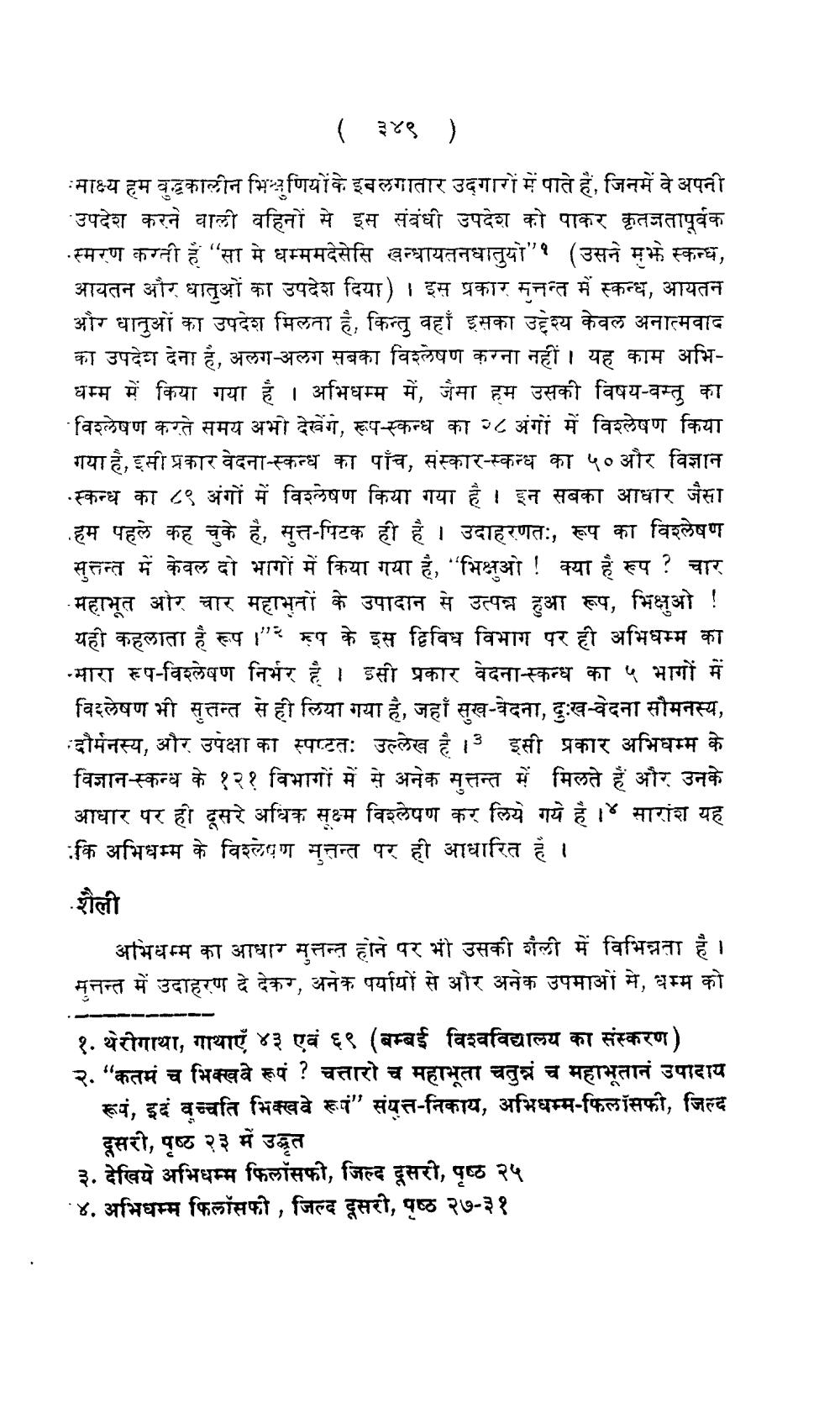________________
( ३४९ )
• साक्ष्य हम बुद्धकालीन भिक्षुणियों के इबलगातार उद्गारों में पाते हैं, जिनमें वे अपनी उपदेश करने वाली वहिनों से इस संबंधी उपदेश को पाकर कृतज्ञतापूर्वक · स्मरण करती हैं “सा मे धम्ममदेसेसि खन्धायतनधातुयो” १ ( उसने मुझे स्कन्ध, आयतन और धातुओं का उपदेश दिया ) । इस प्रकार सुत्तन्त में स्कन्ध, आयतन और धातुओं का उपदेश मिलता है, किन्तु वहाँ इसका उद्देश्य केवल अनात्मवाद का उपदेश देना है, अलग-अलग सबका विश्लेषण करना नहीं । यह काम अभिधम्म में किया गया है । अभिधम्म में, जैसा हम उसकी विषय-वस्तु का - विश्लेषण करते समय अभी देखेंगे, रूप-स्कन्ध का २८ अंगों में विश्लेषण किया गया है, इसी प्रकार वेदना स्कन्ध का पाँच, संस्कार-स्कन्ध का ५० और विज्ञान · स्कन्ध का ८९ अंगों में विश्लेषण किया गया है । इन सबका आधार जैसा 1. हम पहले कह चुके है, सुत्त-पिटक ही है । उदाहरणतः, रूप का विश्लेषण सुतन्त में केवल दो भागों में किया गया है, “भिक्षुओ ! क्या है रूप ? चार - महाभूत ओर चार महाभूतों के उपादान से उत्पन्न हुआ रूप, भिक्षुओ ! यही कहलाता है रूप ।२ रूप के इस द्विविध विभाग पर ही अभिधम्म का - मारा रूप-विश्लेषण निर्भर है । इसी प्रकार वेदना-स्कन्ध का ५ भागों में विश्लेषण भी सुत्तन्त से ही लिया गया है, जहाँ सुख - वेदना, दु:ख वेदना सौमनस्य, दौर्मनस्य, और उपेक्षा का स्पष्टतः उल्लेख है । इसी प्रकार अभिधम्म के विज्ञान-स्कन्ध के १२१ विभागों में से अनेक मुत्तन्त में मिलते हैं और उनके आधार पर ही दूसरे अधिक सूक्ष्म विश्लेषण कर लिये गये है । सारांश यह fe अभिधम्म के विश्लेषण मुत्तन्त पर ही आधारित है ।
- शैली
अभिधम्म का आधार मुत्तन्त होने पर भी उसकी शैली में विभिन्नता है । सुनन्त में उदाहरण दे देकर, अनेक पर्यायों से और अनेक उपमाओं में, धम्म को
१. थेरीगाथा, गाथाएँ ४३ एवं ६९ ( बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण) २. " कतमं च भिक्खवे रूपं ? चत्तारो च महाभूता चतुनं च महाभूतानं उपादाय रूपं, इदं वृच्चति भिक्खवे रूपं" संयुत्त निकाय, अभिधम्म-फिलॉसफी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २३ में
उद्धृत
३. देखिये अभिधम्म फिलॉसफी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २५
४. अभिधम्म फिलॉसफी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २७-३१