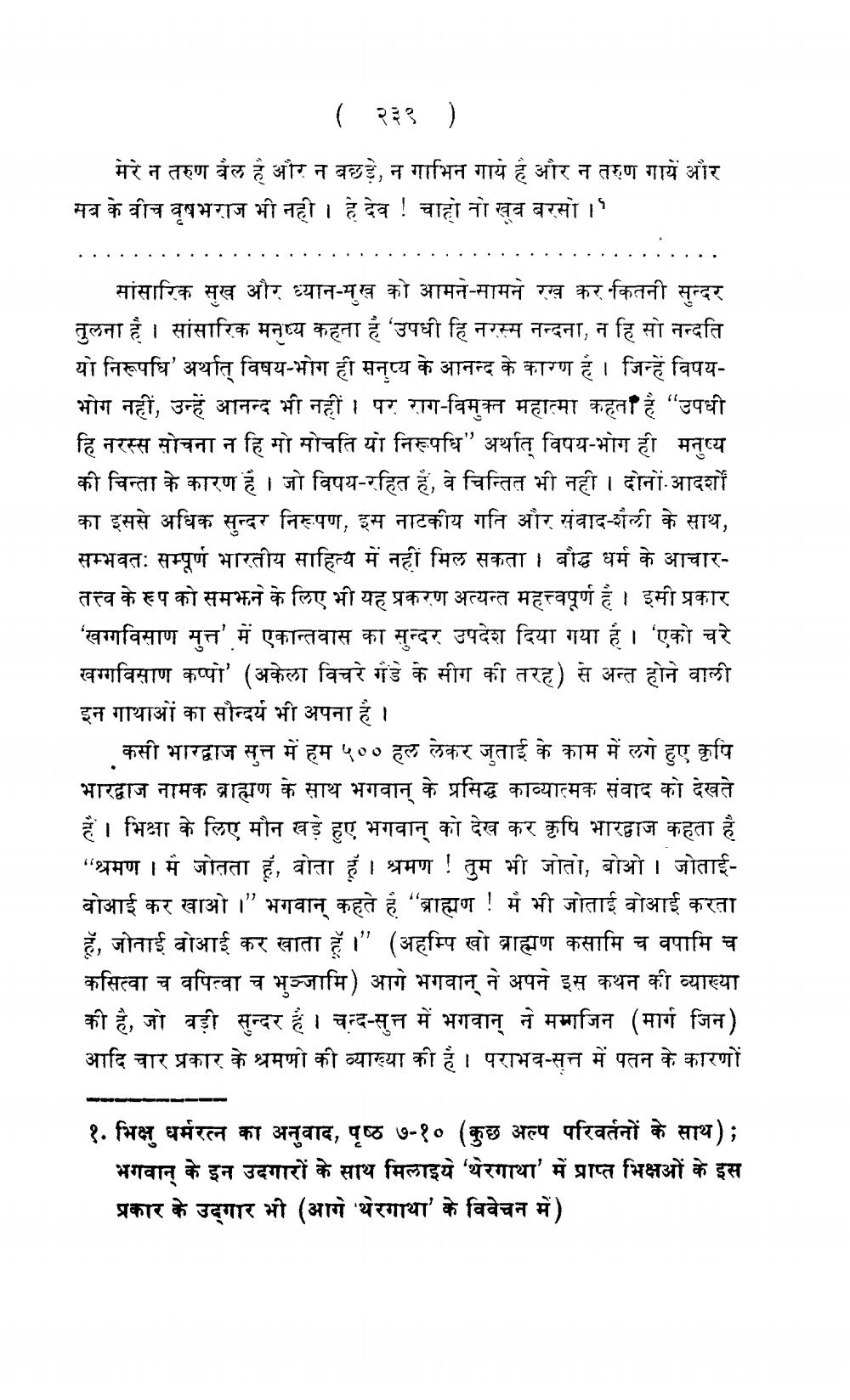________________
( २३९ )
मेरे न तरुण बैल है और न बछड़े, न गाभिन गाय है और न तरुण गायें और मब के बीच वृषभराज भी नहीं। हे देव ! चाहो तो खूब बरसो।
सांसारिक सुख और ध्यान-सुख को आमने-सामने रख कर कितनी सुन्दर तुलना है। सांसारिक मनध्य कहता है 'उपधी हि नरम्म नन्दना, न हि सो नन्दति यो निरूपधि' अर्थात् विषय-भोग ही सनुप्य के आनन्द के कारण है । जिन्हें विपयभोग नहीं, उन्हें आनन्द भी नहीं। पर राग-विमुक्त महात्मा कहता है "उपधी हि नरस्स सोचना न हि मो सोचति यो निरूपधि' अर्थात् विपय-भोग ही मनुष्य की चिन्ता के कारण है । जो विषय-रहित हैं, वे चिन्तित भी नहीं । दोनों आदर्शों का इससे अधिक सुन्दर निरूपण, इस नाटकीय गति और संवाद-शैली के साथ, सम्भवतः सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में नहीं मिल सकता । बौद्ध धर्म के आचारतत्त्व के रूप को समझने के लिए भी यह प्रकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार 'खग्गविसाण मुत्त' में एकान्तवास का सुन्दर उपदेश दिया गया है । ‘एको चरे खग्गविसाण कप्पो' (अकेला विचरे गडे के सीग की तरह) से अन्त होने वाली इन गाथाओं का सौन्दर्य भी अपना है।
कसी भारद्वाज सुत्त में हम ५०० हल लेकर जताई के काम में लगे हए कृषि भारद्वाज नामक ब्राह्मण के साथ भगवान् के प्रसिद्ध काव्यात्मक संवाद को देखते है। भिक्षा के लिए मौन खड़े हुए भगवान् को देख कर कृषि भारद्वाज कहता है "श्रमण । मैं जोतता हूँ, वोता हूँ। श्रमण ! तुम भी जोतो, बोओ। जोताईबोआई कर खाओ।" भगवान् कहते है "ब्राह्मण ! मै भी जोताई बोआई करता हूँ, जोताई बोआई कर खाता हूँ।" (अहम्पि खो ब्राह्मण कसामि च वपामि च कसित्वा च वपित्वा च भुञामि) आगे भगवान ने अपने इस कथन की व्याख्या की है, जो बड़ी सुन्दर है। चन्द-सुत्न में भगवान् ने मजिन (मार्ग जिन) आदि चार प्रकार के श्रमणो की व्याख्या की है। पराभव-सत्त में पतन के कारणों
१. भिक्षु धर्मरत्न का अनुवाद, पृष्ठ ७-१० (कुछ अल्प परिवर्तनों के साथ);
भगवान् के इन उदगारों के साथ मिलाइये 'थेरगाथा' में प्राप्त भिक्षओं के इस प्रकार के उद्गार भी (आगे 'थेरगाथा' के विवेचन में)