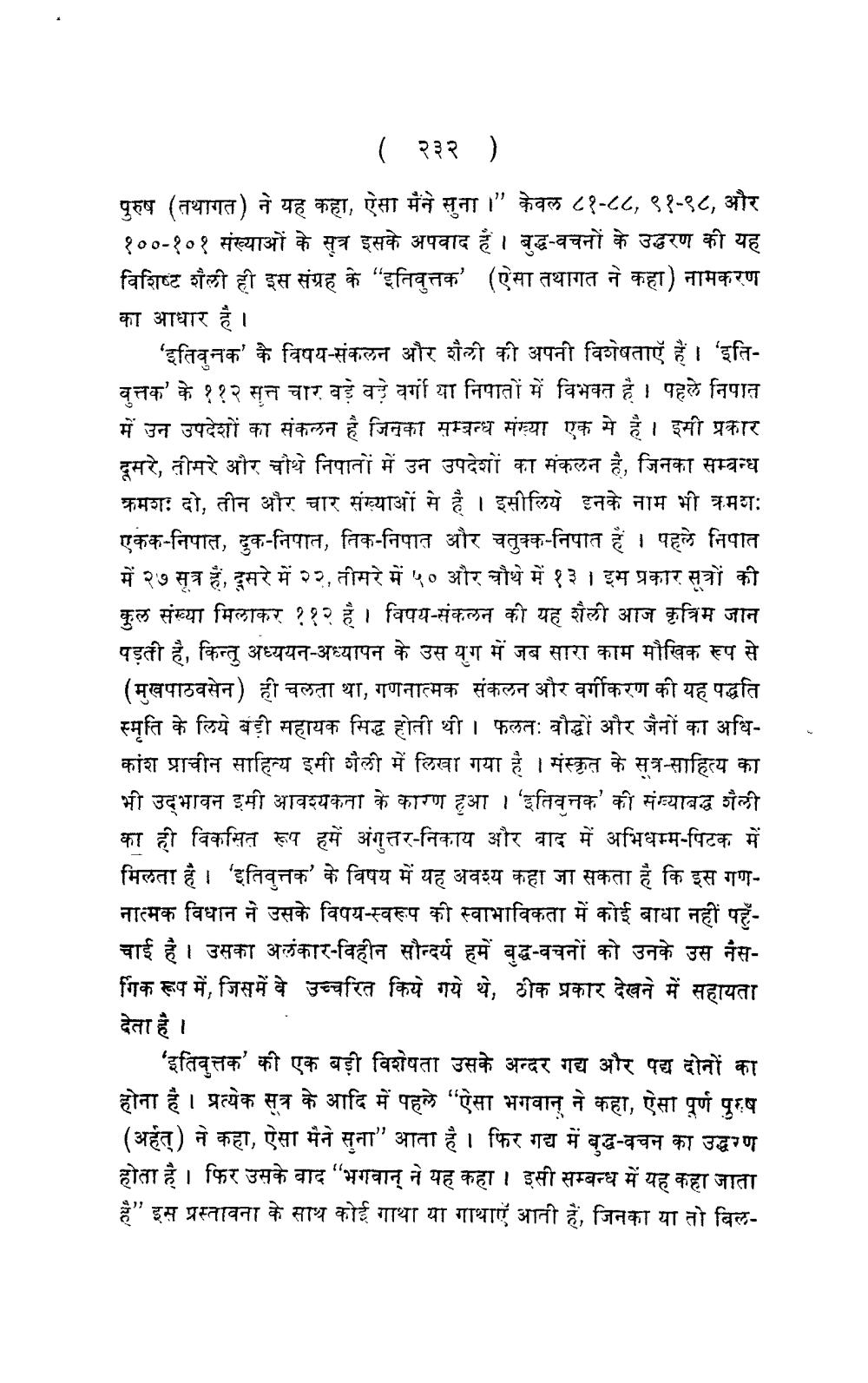________________
( २३२ )
पुरुष ( तथागत ) ने यह कहा, ऐसा मैंने सुना ।” केवल ८१-८८, ९१-९८, और १००-१०१ संख्याओं के सूत्र इसके अपवाद हैं । बुद्ध वचनों के उद्धरण की यह विशिष्ट शैली ही इस संग्रह के "इतिवृत्तक' ( ऐसा तथागत ने कहा ) नामकरण का आधार है ।
'इतिgar' के विषय - संकलन और शैली की अपनी विशेषताएँ हैं । 'इतिबुत्तक' के ११२ सुत्त चार बड़े बड़े वर्गों या निपातों में विभक्त है। पहले निपात में उन उपदेशों का संकलन है जिनका सम्बन्ध संख्या एक से है । इसी प्रकार दूसरे, तीसरे और चौथे निपातों में उन उपदेशों का संकलन है, जिनका सम्बन्ध क्रमशः दो, तीन और चार संख्याओं से है । इसीलिये इनके नाम भी क्रमशः एकक-निपात, दुक निपात, तिक-निपात और चतुक्क निपात हैं । पहले निपात में २७ सूत्र हैं, दूसरे में २२, तीमरे में ५० और चौथे में १३ । इस प्रकार सूत्रों की कुल संख्या मिलाकर ११२ है । विषय-संकलन की यह शैली आज कृत्रिम जान पड़ती है, किन्तु अध्ययन-अध्यापन के उस युग में जब सारा काम मौखिक रूप से ( मुखपाठवसेन) ही चलता था, गणनात्मक संकलन और वर्गीकरण की यह पद्धति स्मृति के लिये बड़ी सहायक सिद्ध होती थी । फलतः बौद्धों और जैनों का अधिकांश प्राचीन साहित्य इमी शैली में लिखा गया है । संस्कृत के सूत्र - साहित्य का भी उद्भावन इसी आवश्यकता के कारण हुआ । 'इतिवृत्तक' की संख्याबद्ध शैली का ही विकसित रूप हमें अंगुत्तरनिकाय और बाद में अभिधम्मपिटक में मिलता है । 'इतिवृत्तक' के विषय में यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस गणनात्मक विधान ने उसके विषय स्वरूप की स्वाभाविकता में कोई बाधा नहीं पहुँचाई है । उसका अलंकार- विहीन सौन्दर्य हमें बुद्ध वचनों को उनके उस नसगिक रूप में, जिसमें वे उच्चरित किये गये थे, ठीक प्रकार देखने में सहायता देता है ।
'इतिवृत्तक' की एक बड़ी विशेषता उसके अन्दर गद्य और पद्य दोनों का होना है । प्रत्येक सूत्र के आदि में पहले "ऐसा भगवान् ने कहा, ऐसा पूर्ण पुरुष ( अर्हत् ) ने कहा, ऐसा मैने सुना" आता है । फिर गद्य में बुद्ध वचन का उद्धरण होता है । फिर उसके बाद "भगवान् ने यह कहा । इसी सम्बन्ध में यह कहा जाता है" इस प्रस्तावना के साथ कोई गाथा या गाथाएँ आती हैं, जिनका या तो बिल