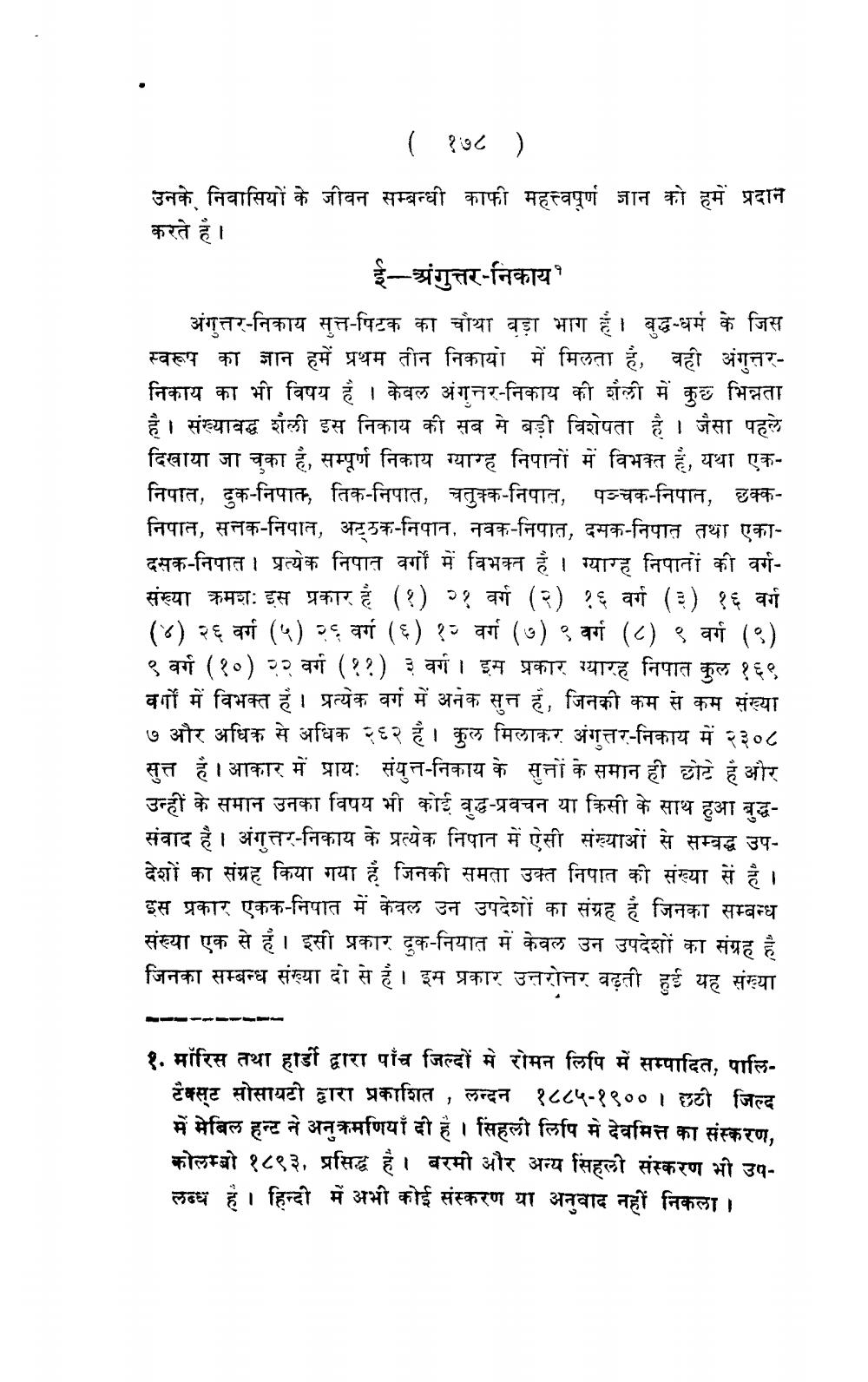________________
(
१७८
)
उनके निवासियों के जीवन सम्बन्धी काफी महत्त्वपूर्ण ज्ञान को हमें प्रदान करते है।
ई-अंगुत्तर-निकाय' अंगुत्तर-निकाय सुत्त-पिटक का चौथा बड़ा भाग है। बुद्ध-धर्म के जिस स्वरूप का ज्ञान हमें प्रथम तीन निकायों में मिलता है, वही अंगुत्तरनिकाय का भी विषय है । केवल अंगनर-निकाय की शैली में कुछ भिन्नता है। संख्याबद्ध शैली इस निकाय की सब से बड़ी विशेषता है । जैसा पहले दिखाया जा चुका है, सम्पूर्ण निकाय ग्यारह निपातों में विभक्त है, यथा एकनिपात, दुक-निपात, तिक-निपात, चतुक्क-निपात, पञ्चक-निपात, छक्कनिपात, सनक-निपात, अट्ठक-निपात, नवक-निपात, दमक-निपात तथा एकादसक-निपात। प्रत्येक निपात वर्गों में विभक्त है । ग्यारह निपातों की वर्गसंख्या क्रमश: इस प्रकार है (१) २१ वर्ग (२) १६ वर्ग (३) १६ वर्ग (४) २६ वर्ग (५) २६ वर्ग (६) १२ वर्ग (७) ९ वर्ग (८) ९ वर्ग (९) ९ वर्ग (१०) २२ वर्ग (११) ३ वर्ग। इस प्रकार ग्यारह निपात कुल १६९ वर्गों में विभक्त है। प्रत्येक वर्ग में अनेक सुत्त है, जिनकी कम से कम संख्या ७ और अधिक से अधिक २६२ है। कुल मिलाकर अंगुत्तर-निकाय में २३०८ सुत्त है। आकार में प्रायः संयुत्त-निकाय के सुत्तों के समान ही छोटे है और उन्हीं के समान उनका विषय भी कोई बुद्ध-प्रवचन या किसी के साथ हुआ बुद्धसंवाद है। अंगुत्तर-निकाय के प्रत्येक निपान में ऐसी संख्याओं से सम्बद्ध उपदेशों का संग्रह किया गया है जिनकी समता उक्त निपात की संख्या में है। इस प्रकार एकक-निपात में केवल उन उपदेशों का संग्रह है जिनका सम्बन्ध संख्या एक से हैं। इसी प्रकार दुक-नियात में केवल उन उपदेशों का संग्रह है जिनका सम्बन्ध संख्या दो से है। इस प्रकार उत्तरोतर बढ़ती हुई यह संख्या
१. मॉरिस तथा हार्डी द्वारा पाँच जिल्दों में रोमन लिपि में सम्पादित, पालि
टैक्स्ट सोसायटी द्वारा प्रकाशित , लन्दन १८८५-१९०० । छठी जिल्द में मेबिल हन्ट ने अनुक्रमणियाँ दी है । सिंहली लिपि मे देवमित्त का संस्करण, कोलम्बो १८९३, प्रसिद्ध है। बरमी और अन्य सिंहली संस्करण भी उपलब्ध है। हिन्दी में अभी कोई संस्करण या अनुवाद नहीं निकला।