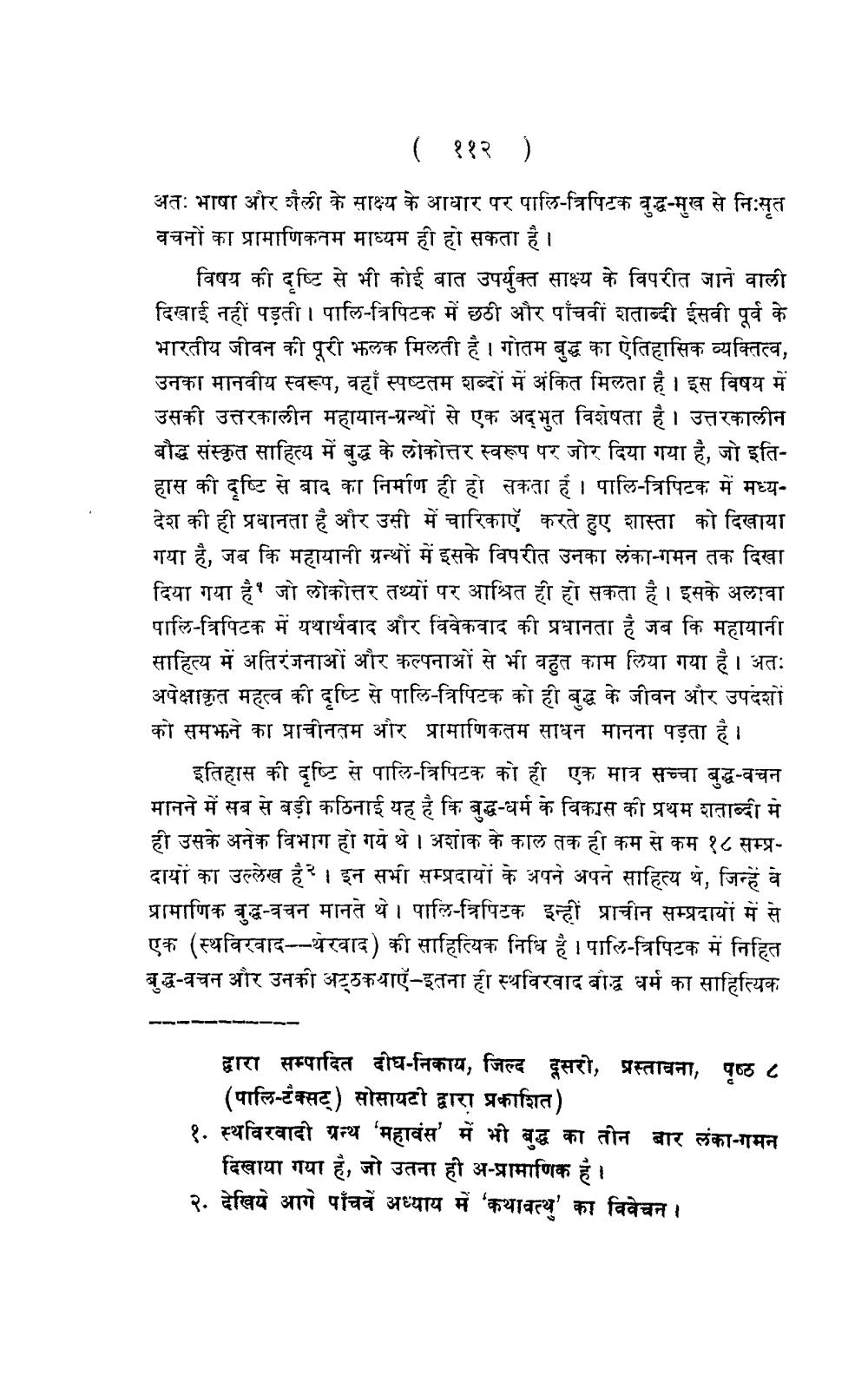________________
( ११२ )
अतः भाषा और शैली के साक्ष्य के आधार पर पालि-त्रिपिटक बुद्ध-मुख से निःसृत वचनों का प्रामाणिकतम माध्यम ही हो सकता है ।
विषय की दृष्टि से भी कोई बात उपर्युक्त साक्ष्य के विपरीत जाने वाली दिखाई नहीं पड़ती । पालि-त्रिपिटक में छठी और पाँचवीं शताब्दी ईसवी पूर्व के भारतीय जीवन की पूरी झलक मिलती है । गोतम बुद्ध का ऐतिहासिक व्यक्तित्व, उनका मानवीय स्वरूप, वहाँ स्पष्टतम शब्दों में अंकित मिलता है । इस विषय में उसकी उत्तरकालीन महायान ग्रन्थों से एक अद्भुत विशेषता है । उत्तरकालीन बौद्ध संस्कृत साहित्य में बुद्ध के लोकोत्तर स्वरूप पर जोर दिया गया है, जो इतिहास की दृष्टि से बाद का निर्माण ही हो सकता हैं । पालि-त्रिपिटक में मध्यदेश की ही प्रधानता है और उसी में चारिकाएँ करते हुए शास्ता को दिखाया गया है, जब कि महायानी ग्रन्थों में इसके विपरीत उनका लंका-गमन तक दिखा दिया गया है जो लोकोत्तर तथ्यों पर आश्रित ही हो सकता है । इसके अलावा पालि-त्रिपिटक में यथार्थवाद और विवेकवाद की प्रधानता है जब कि महायानी साहित्य में अतिरंजनाओं और कल्पनाओं से भी बहुत काम लिया गया है । अतः अपेक्षाकृत महत्व की दृष्टि से पालि- त्रिपिटक को ही बुद्ध के जीवन और उपदेशों को समझने का प्राचीनतम और प्रामाणिकतम साधन मानना पड़ता है ।
इतिहास की दृष्टि से पालि- त्रिपिटक को ही एक मात्र सच्चा बुद्ध वचन मानने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बुद्ध धर्म के विकास की प्रथम शताब्दी में ही उसके अनेक विभाग हो गये थे । अशोक के काल तक ही कम से कम १८ सम्प्रदायों का उल्लेख है । इन सभी सम्प्रदायों के अपने अपने साहित्य थे, जिन्हें वे प्रामाणिक बुद्ध वचन मानते थे । पालि- त्रिपिटक इन्हीं प्राचीन सम्प्रदायों में से एक ( स्थविरवाद - - थेरवाद) की साहित्यिक निधि है । पालि-त्रिपिटक में निहित बुद्ध वचन और उनकी अट्ठकथाएँ - इतना ही स्थविरवाद बौद्ध धर्म का साहित्यिक
द्वारा सम्पादित दीघ - निकाय, जिल्द दूसरो प्रस्तावना, पृष्ठ ८ ( पालि- टैक्सट् ) सोसायटी द्वारा प्रकाशित )
१. स्थविरवादी ग्रन्थ 'महावंस' में भी बुद्ध का तीन बार लंका-गमन दिखाया गया है, जो उतना ही अ-प्रामाणिक है ।
२. देखिये आगे पाँचवें अध्याय में 'कथावत्थु' का विवेचन ।