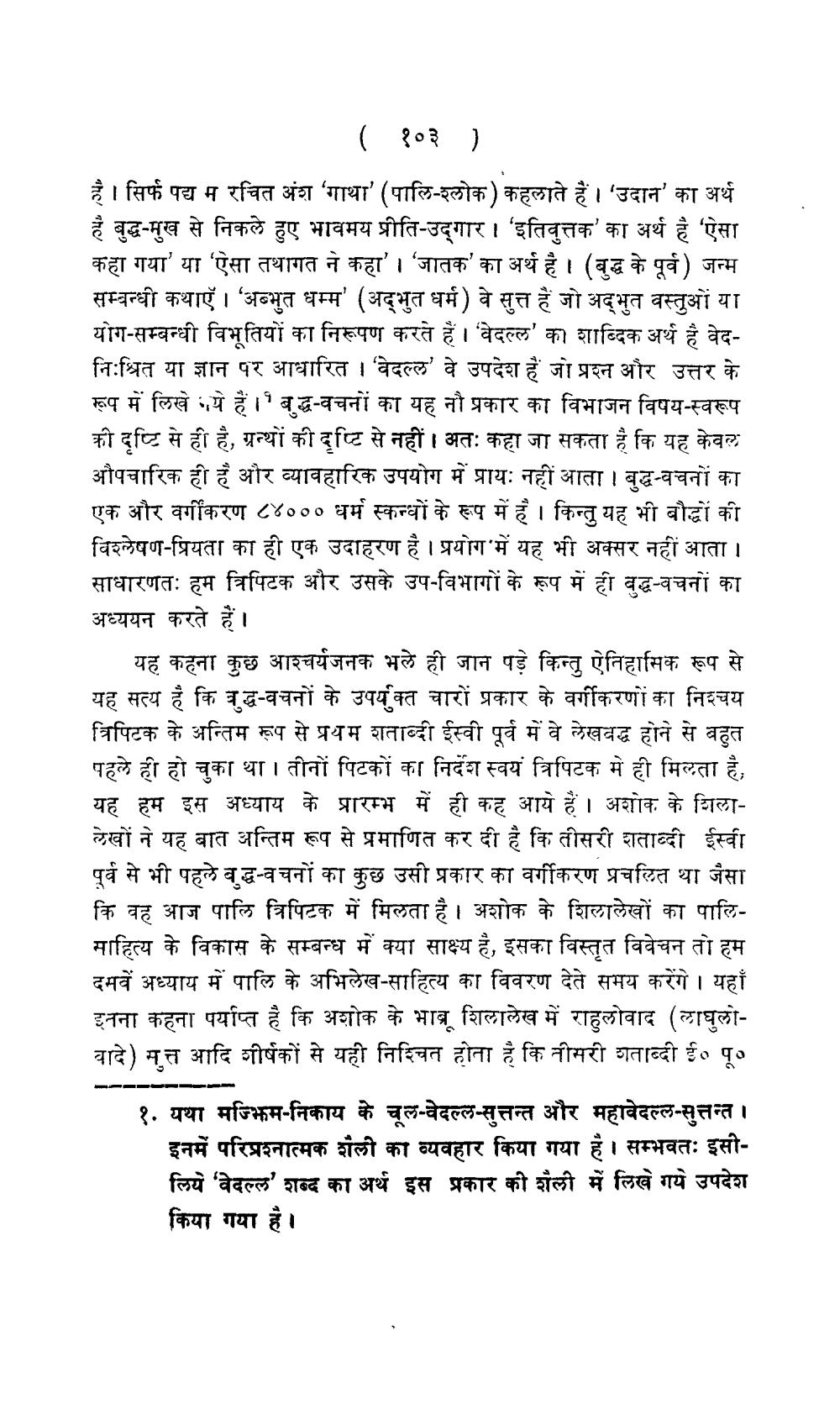________________
( १०३ ) है। सिर्फ पद्य म रचित अंश 'गाथा' (पालि-श्लोक) कहलाते हैं। 'उदान' का अर्थ है बुद्ध-मुख से निकले हुए भावमय प्रीति-उद्गार । 'इतिवृत्तक' का अर्थ है ‘ऐसा कहा गया' या 'ऐसा तथागत ने कहा' । 'जातक' का अर्थ है । (बुद्ध के पूर्व) जन्म सम्बन्धी कथाएँ । 'अब्भुत धम्म' (अद्भुत धर्म) वे सुत्त हैं जो अद्भुत वस्तुओं या योग-सम्बन्धी विभूतियों का निरूपण करते हैं । वेदल्ल' का शाब्दिक अर्थ है वेदनिःश्रित या ज्ञान पर आधारित । 'वेदल्ल' वे उपदेश हैं जो प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखे गये हैं।' बुद्ध-वचनों का यह नौ प्रकार का विभाजन विषय-स्वरूप की दृष्टि से ही है, ग्रन्थों की दृष्टि से नहीं। अतः कहा जा सकता है कि यह केवल औपचारिक ही है और व्यावहारिक उपयोग में प्रायः नहीं आता। बुद्ध-वचनों का एक और वर्गीकरण ८४००० धर्म स्कन्धों के रूप में है । किन्तु यह भी बौद्धों की विश्लेषण-प्रियता का ही एक उदाहरण है । प्रयोग में यह भी अक्सर नहीं आता। साधारणतः हम त्रिपिटक और उसके उप-विभागों के रूप में ही बुद्ध-वचनों का अध्ययन करते हैं।
यह कहना कुछ आश्चर्यजनक भले ही जान पड़े किन्तु ऐतिहासिक रूप से यह सत्य है कि बुद्ध-वचनों के उपर्युक्त चारों प्रकार के वर्गीकरणों का निश्चय त्रिपिटक के अन्तिम रूप से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में वे लेखबद्ध होने से बहुत पहले ही हो चुका था। तीनों पिटकों का निर्देश स्वयं त्रिपिटक मे ही मिलता है, यह हम इस अध्याय के प्रारम्भ में ही कह आये हैं। अशोक के शिलालेखों ने यह बात अन्तिम रूप से प्रमाणित कर दी है कि तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से भी पहले बुद्ध-वचनों का कुछ उसी प्रकार का वर्गीकरण प्रचलित था जैसा कि वह आज पालि त्रिपिटक में मिलता है। अशोक के शिलालेखों का पालिमाहित्य के विकास के सम्बन्ध में क्या साक्ष्य है, इसका विस्तृत विवेचन तो हम दमवें अध्याय में पालि के अभिलेख-साहित्य का विवरण देते समय करेंगे। यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि अशोक के भाव शिलालेख में राहुलोवाद (लाघुलोवादे) मृत्त आदि शीर्षकों से यही निश्चित होता है कि तीसरी शताब्दी ई० पू०
१. यथा मज्झिम-निकाय के चूल-वेदल्ल-सुत्तन्त और महावेदल्ल-सुत्तन्त ।
इनमें परिप्रश्नात्मक शैली का व्यवहार किया गया है। सम्भवतः इसीलिये 'वेदल्ल' शब्द का अर्थ इस प्रकार की शैली में लिखे गये उपदेश किया गया है।