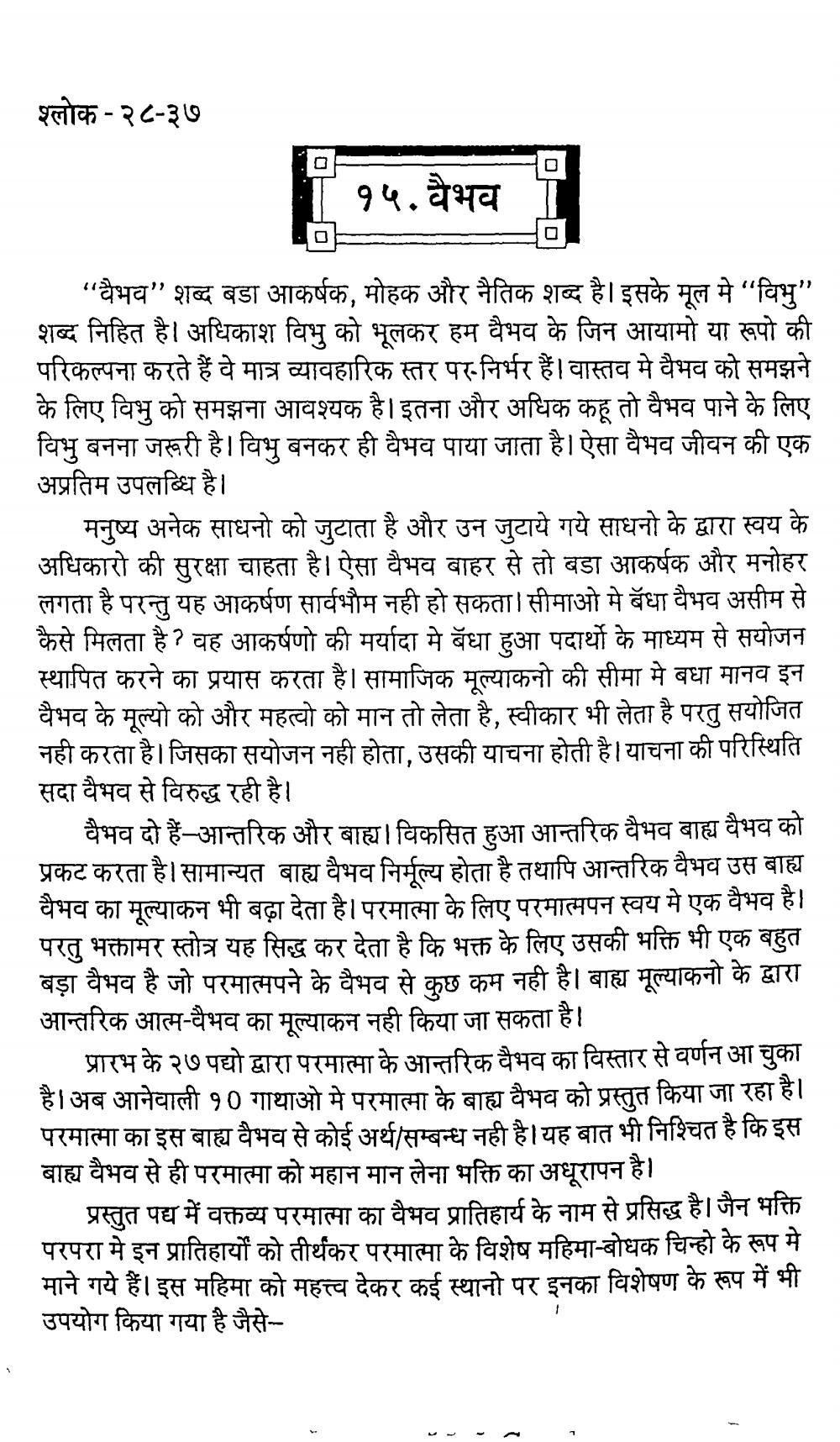________________
श्लोक-२८-३७
O
O
१५. वैभव
•
O
"वैभव" शब्द बड़ा आकर्षक, मोहक और नैतिक शब्द है। इसके मूल मे "विभु" शब्द निहित है। अधिकाश विभु को भूलकर हम वैभव के जिन आयामो या रूपो की परिकल्पना करते हैं वे मात्र व्यावहारिक स्तर पर निर्भर हैं। वास्तव मे वैभव को समझने के लिए विभु को समझना आवश्यक है । इतना और अधिक कहू तो वैभव पाने के लिए विभु बनना जरूरी है। विभु बनकर ही वैभव पाया जाता है। ऐसा वैभव जीवन की एक अप्रतिम उपलब्धि है।
मनुष्य अनेक साधनो को जुटाता है और उन जुटाये गये साधनो के द्वारा स्वय के अधिकारो की सुरक्षा चाहता है। ऐसा वैभव बाहर से तो बडा आकर्षक और मनोहर लगता है परन्तु यह आकर्षण सार्वभौम नही हो सकता। सीमाओ मे बँधा वैभव असीम से कैसे मिलता है ? वह आकर्षणो की मर्यादा मे बँधा हुआ पदार्थो के माध्यम से सयोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। सामाजिक मूल्याकनो की सीमा मे बधा मानव इन वैभव के मूल्यो को और महत्वो को मान तो लेता है, स्वीकार भी लेता है परंतु सयोजित करता है। जिसका सयोजन नही होता, उसकी याचना होती है । याचना की परिस्थिति सदा वैभव से विरुद्ध रही है।
वैभव दो हैं - आन्तरिक और बाह्य । विकसित हुआ आन्तरिक वैभव बाह्य वैभव को प्रकट करता है। सामान्यत बाह्य वैभव निर्मूल्य होता है तथापि आन्तरिक वैभव उस बाह्य वैभव का मूल्याकन भी बढ़ा देता है। परमात्मा के लिए परमात्मपन स्वय मे एक वैभव है। परतु भक्तामर स्तोत्र यह सिद्ध कर देता है कि भक्त के लिए उसकी भक्ति भी एक बहुत बड़ा वैभव है जो परमात्मपने के वैभव से कुछ कम नही है । बाह्य मूल्याकनो के द्वारा आन्तरिक आत्म-वैभव का मूल्याकन नही किया जा सकता है।
प्रारभ के २७ पद्यो द्वारा परमात्मा के आन्तरिक वैभव का विस्तार से वर्णन आ चुका है। अब आनेवाली १० गाथाओ मे परमात्मा के बाह्य वैभव को प्रस्तुत किया जा रहा है। परमात्मा का इस बाह्य वैभव से कोई अर्थ / सम्बन्ध नही है । यह बात भी निश्चित है कि इस बाह्य वैभव से ही परमात्मा को महान मान लेना भक्ति का अधूरापन है।
ܐ
प्रस्तुत पद्य में वक्तव्य परमात्मा का वैभव प्रातिहार्य के नाम से प्रसिद्ध है। जैन भक्ति परपरा मे इन प्रातिहार्यों को तीर्थंकर परमात्मा के विशेष महिमा-बोधक चिन्हो के रूप मे माने गये हैं। इस महिमा को महत्त्व देकर कई स्थानो पर इनका विशेषण के रूप में भी उपयोग किया गया है जैसे
'
C