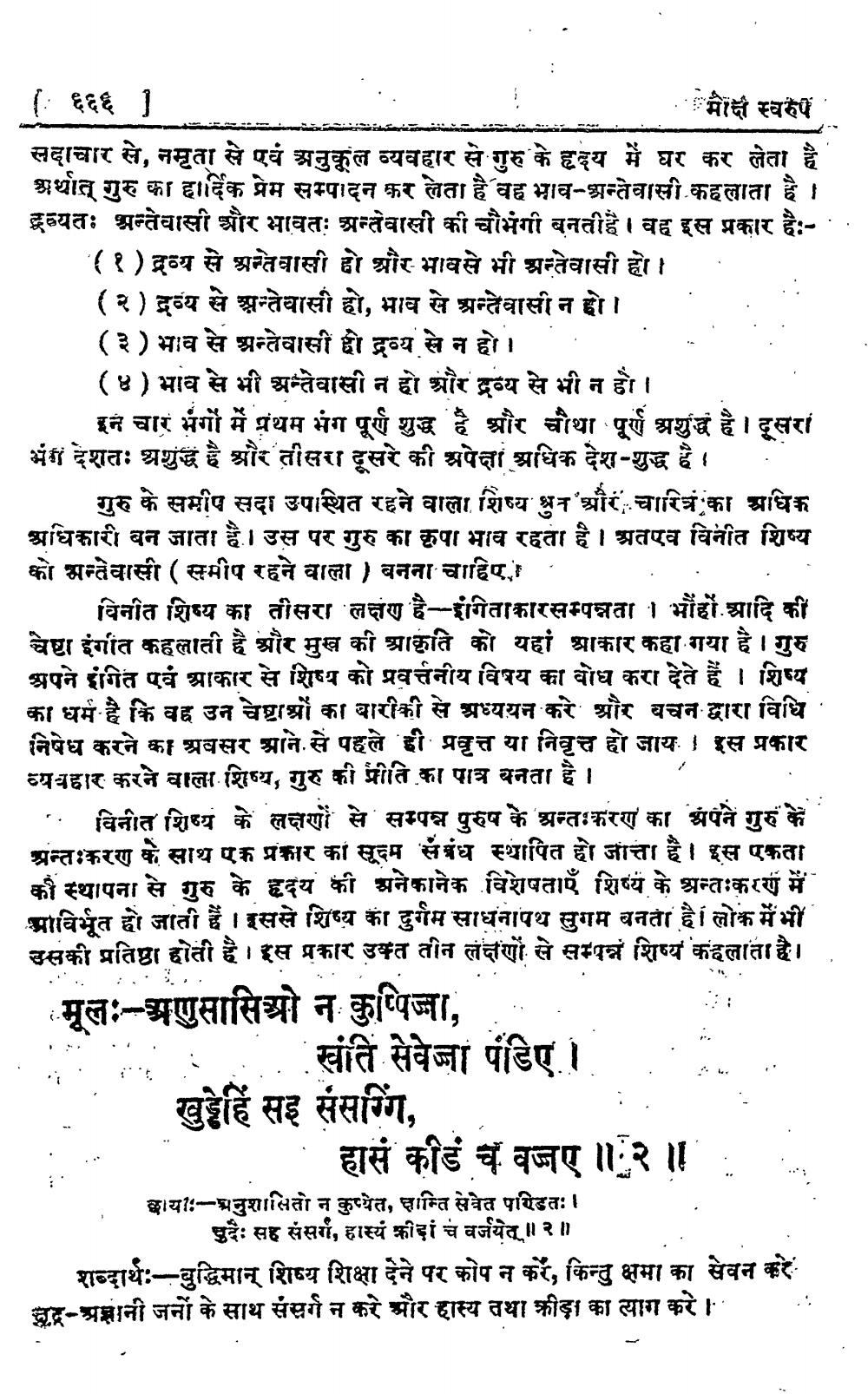________________
मोक्ष स्वरु लदाचार से, नमृता से एवं अनुकूल व्यवहार से गुरु के हृदय में घर कर लेता है अर्थात् गुरु का हार्दिक प्रेम सम्पादन कर लेता है वह भाव-अन्तेवासी कहलाता है। व्यतः अन्तेवासी और भावतः अन्तवाली की चौभंगी बनतीहै। वह इस प्रकार है:
(१) द्रव्य से अन्तवासी हो और भावसे भी अन्तेवासी हो। (२) द्रव्य से अन्तेवासी हो, भाव से अन्तेवासी न हो। (३) भाव से अन्तेवासी ही द्रव्य से न हो। (४) भाव से भी अन्तेवासी न हो और द्रव्य से भी न हो।
इन चार भगों में प्रथम भंग पूर्ण शुद्ध है और चौथा पूर्ण अर्युद्ध है । दूसरा भंग देशतः श्रशुद्ध है और तीसरा दूसरे की अपेक्षा अधिक देश-शुद्ध है।
गुरु के समीप सदा उपस्थित रहने वाला शिष्य श्रुत्र और चारित्रं का अधिक अधिकारी बन जाता है। उस पर गुरु का कृपा भाव रहता है। अतएव विनीत शिष्य को अन्तेवासी ( समीप रहने वाला ) बनना चाहिए ।
विनीत शिष्य का तीसरा लक्षण है-इंगिताकारसम्पन्नता । भौंहों.आदि की चेष्टा इंगांत कहलाती है और मुख की प्राकृति को यहां श्राकार कहा गया है। गुरु अपने इंगित एवं प्राकार से शिष्य को प्रवर्तनीय विषय का वोध करा देते हैं । शिष्य का धर्म है कि वह उन चेष्टाओं का बारीकी से अध्ययन करे और बचन द्वारा विधि : निषेध करने का अवसर आने से पहले ही प्रवृत्त या निवृत्त हो जायः । इस प्रकार व्यवहार करने वाला शिष्य, गुरु की प्रीति का पात्र बनता है। '. विनीत शिष्य के लक्षणों से सम्पन्न पुरुष के अन्तःकरण का अपने गुरु के अन्तःकरण के साथ एक प्रकार का सूक्ष्म संबंध स्थापित हो जाता है। इस एकता की स्थापना से गुरु के हृदय की अनेकानेक विशेषताएँ शिष्य के अन्तःकरण में प्राविर्भत हो जाती हैं । इससे शिष्य का दुर्गम साधनापथ सुगम बनता है। लोक में भी उसकी प्रतिष्ठा होती है। इस प्रकार उक्त तीन लक्षणों से सम्पन्न शिष्य कहलाता है। . मूल:-अणुसासिनो न कुप्पिजा, .. .. .
खंति सेवेना पंडिए । . खुड्डेहि सइ संसग्गिं,
' हासं कोडं च वजए ॥२॥ .. छाया:-अनुशासितो न कुप्येत, शान्ति सेवेत पण्डितः ।
धुदैः सह संसर्ग, हास्य क्रीडां च वर्जयेत् ॥२॥ शब्दार्थ:-बुद्धिमान् शिष्य शिक्षा देने पर कोप न करें, किन्तु क्षमा का सेवन करें क्षुद्र-अज्ञानी जनों के साथ संसर्ग न करे और हास्य तथा क्रीड़ा का त्याग करे।