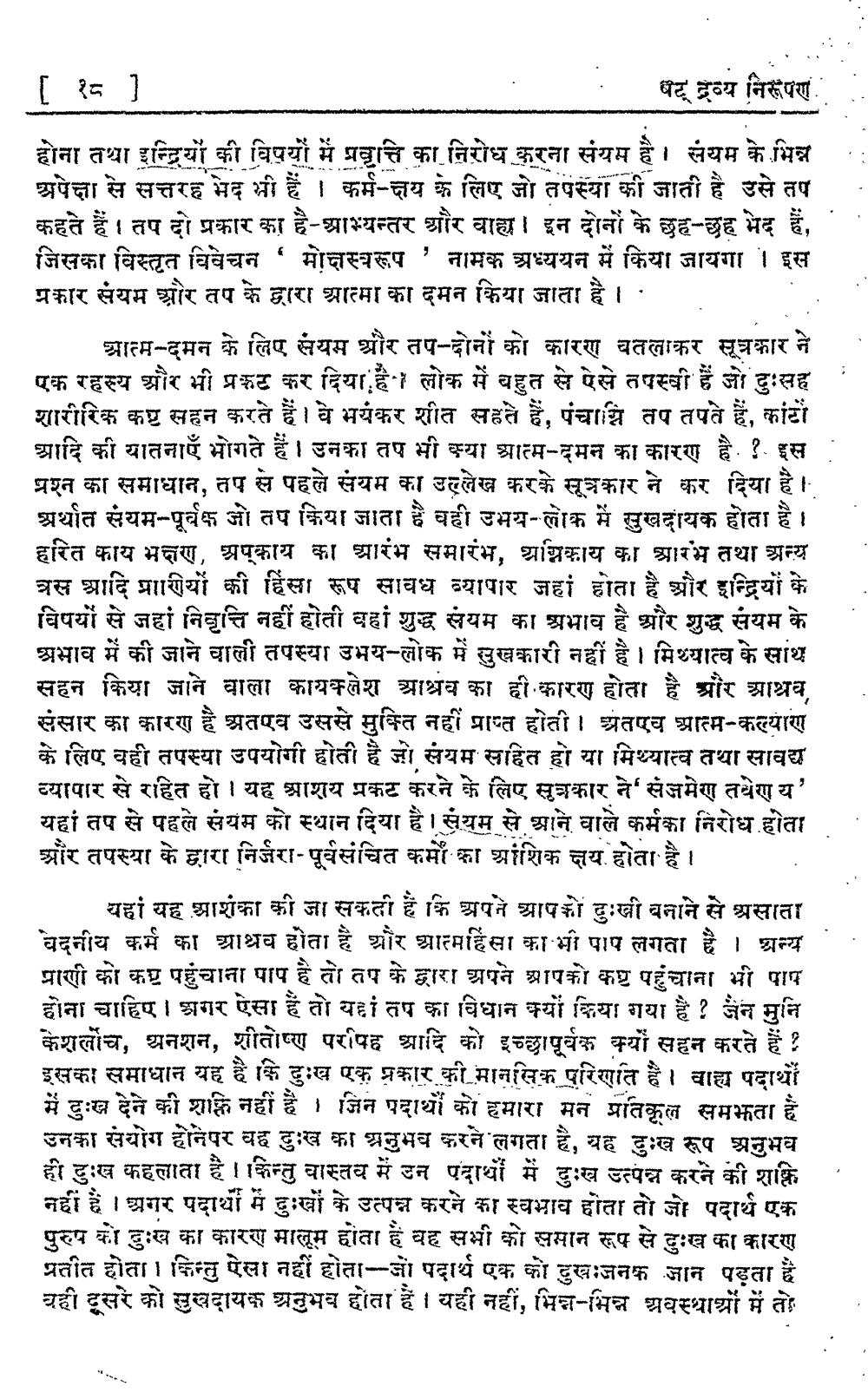________________
[ २८ ]
बंद द्रव्य निरूपण. होना तथा इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति का निरोध करना संयम है। संयम के भिन्न अपेक्षा से सत्तरह भेद भी हैं । कर्म-क्षय के लिए जो तपस्या की जाती है उसे तप कहते हैं । तप दो प्रकार का है - श्राभ्यन्तर और वाह्य । इन दोनों के छह-छह भेद हैं, जिसका विस्तृत विवेचन ' मोक्षस्वरूप ' नामक अध्ययन में किया जायगा | इस प्रकार संयम और तप के द्वारा श्रात्मा का दमन किया जाता 1:
ने
श्रात्म - दमन के लिए संयम और तप दोनों को कारण बतलाकर सूत्रकार एक रहस्य और भी प्रकट कर दिया है। लोक में बहुत से ऐसे तपस्वी हैं जो दुःसह शारीरिक कष्ट सहन करते हैं । वे भयंकर शीत सहते हैं, पंचाग्नि तप तपते हैं, कांटों आदि की यातनाएँ भोगते हैं। उनका तप भी क्या श्रात्म-दमन का कारण है ? इस प्रश्न का समाधान, तप से पहले संयम का उल्लेख करके सूत्रकार ने कर दिया है । अर्थात संयम-पूर्वक जो तप किया जाता है वही उभय-लोक में सुखदायक होता है । हरित काय भक्षण, अप्काय का प्रारंभ समारंभ, अग्निकाय का आरंभ तथा अन्य त्र आदि प्राणियों की हिंसा रूप सावध व्यापार जहां होता है और इन्द्रियों के विषयों से जहां निवृत्ति नहीं होती वहां शुद्ध संयम का अभाव है और शुद्ध संयम के अभाव में की जाने वाली तपस्या उभय-लोक में सुखकारी नहीं है । मिथ्यात्व के साथ सहन किया जाने वाला कायक्लेश आश्रय का ही कारण होता है और आव संसार का कारण है अतएव उससे मुक्ति नहीं प्राप्त होती । श्रतएव आत्म-कल्याण के लिए वही तपस्या उपयोगी होती है जो संयम सहित हो या मिथ्यात्व तथा सावद्य व्यापार से रहित हो । यह श्राशय प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने ' संजमेण तथेण य' यहां तप से पहले संयम को स्थान दिया है। संयम से आने वाले कर्मका निरोध होता और तपस्या के द्वारा निर्जरा- पूर्वसंचित कर्मों का अांशिक क्षय होता है ।
यहां यह आशंका की जा सकती हैं कि अपने आपको दुःखी बनाने से श्रसाता "वेदनीय कर्म का ग्राव होता है और आत्महिंसा का भी पाप लगता है । अन्य प्राणी को कष्ट पहुंचाना पाप है तो तप के द्वारा अपने आपको कष्ट पहुंचाना भी पाप होना चाहिए । अगर ऐसा हैं तो यहां तप का विधान क्यों किया गया है ? जैन मुनि केशलोंच, अनशन, शीतोष्ण परपि श्रादि को इच्छापूर्वक क्यों सहन करते हैं ? इसका समाधान यह है कि दुःख एक प्रकार की मानसिक परिणति हैं । वाह्य पदार्थों में दुःख देने की शक्ति नहीं है । जिन पदार्थों को हमारा मन प्रतिकूल समझता है। उनका संयोग होनेपर वह दुःख का अनुभव करने लगता है, यह दुःख रूप अनुभव ही दुःख कहलाता है | किन्तु वास्तव में उन पदार्थों में दुःख उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है । अगर पदार्थों में दुःखों के उत्पन्न करने का स्वभाव होता तो जो पदार्थ एक पुरुष को दुःख का कारण मालूम होता है वह सभी को समान रूप से दुःख का कारण प्रतीत होता । किन्तु ऐसा नहीं होता - जो पदार्थ एक को दुखःजनक जान पड़ता है वही दूसरे को सुखदायक अनुभव होता है। यही नहीं, भिन्न-भिन्न अवस्थार्थी में तो
P