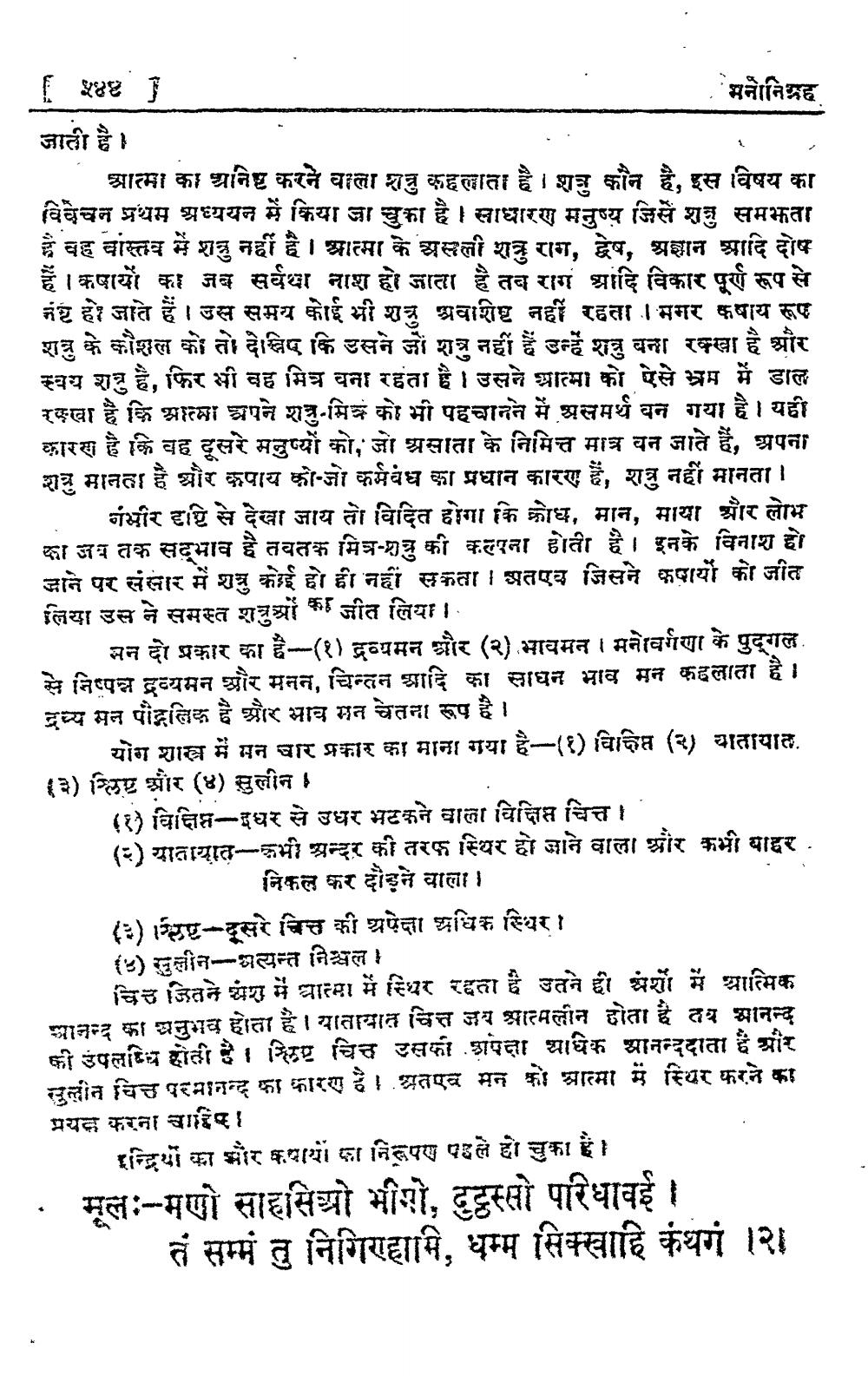________________
५४४
जाती है।
आत्मा का श्रनिष्ट करने वाला शत्रु कहलाता है । शत्रु कौन है, इस विषय का विवेचन प्रथम अध्ययन में किया जा चुका है । साधारण मनुष्य जिसे शत्रु समझता है वह वास्तव में शत्रु नहीं है । आत्मा के असली शत्रु राग, द्वेष, अज्ञान आदि दोष | कषायों का जब सर्वथा नाश हो जाता है तब राग श्रादि विकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं । उस समय कोई भी शत्रु अवशिष्ट नहीं रहता । मगर कषाय रूप शत्रु के कौशल को तो देखिए कि उसने जो शत्रु नहीं हैं उन्हें शत्रु बना रक्खा है और स्वय शत्रु है, फिर भी वह मित्र बना रहता है। उसने श्रात्मा को ऐसे भ्रम में डाल रक्खा है कि श्रात्मा अपने शत्रु-मित्र को भी पहचानने में असमर्थ बन गया है । यही कारण है कि वह दूसरे मनुष्यों को, जो श्रसाता के निमित्त मात्र वन जाते हैं, अपना शत्रु मानता है और रूपाय को-जो कर्मबंध का प्रधान कारण हैं, शत्रु नहीं मानता ।
मनोनिग्रह
गंभीर दृष्टि से देखा जाय तो विदित होगा कि क्रोध, मान, माया और लोभ का जब तक सद्भाव है तबतक मित्र शत्रु की कल्पना होती है । इनके विनाश हो जाने पर संसार में शत्रु कोई हो ही नहीं सकता । अतएव जिसने कपायों को जीत लिया उस ने समस्त शत्रुओं का जीत लिया।
जन दो प्रकार का है - (१) द्रव्यमन और (२) भावमन । मनोवर्गणा के पुद्गल. से निष्पन्न द्रव्यमन और मनन, चिन्तन आदि का साधन भाव मन कहलाता है । द्रव्य मन पौगलिक है और भाव मन चेतना रूप है ।
योग शास्त्र में मन चार प्रकार का माना गया है- (१) विक्षिप्त ( २ ) यातायात. (३) लिष्ट और (४) सुलीन ।
(१) विक्षिप्त - इधर से उधर भटकने वाला विक्षिप्त चित्त ।
(२) यातायात - कभी अन्दर की तरफ स्थिर हो जाने वाला और कभी बाहर निकल कर दौड़ने वाला ।
(३) लिए दूसरे चित्त की अपेक्षा अधिक स्थिर ।
(४) सुलीन अत्यन्त निश्चल ।
चिच जितने अंश में श्रात्मा में स्थिर रहता है उतने ही शो में श्रात्मिक आनन्द का अनुभव होता है । यातायात चित्त जय आत्मलीन होता है तब आनन्द की उपलब्धि होती है। लिए चित्त उसकी अपेक्षा अधिक श्रानन्ददाता हैं और सुन चित्त परमानन्द का कारण है। अतएव मन को आत्मा में स्थिर करने का प्रयक्ष करना चाहिए।
इन्द्रियों का और कषायों का निरूपण पहले हो चुका है।
मूल:- मणो साहसियो भीगो दुट्टस्सो परिधावई ।
तं सम्मं तु निगिरहामि, धम्म सिक्खाहि कंथगं |२|