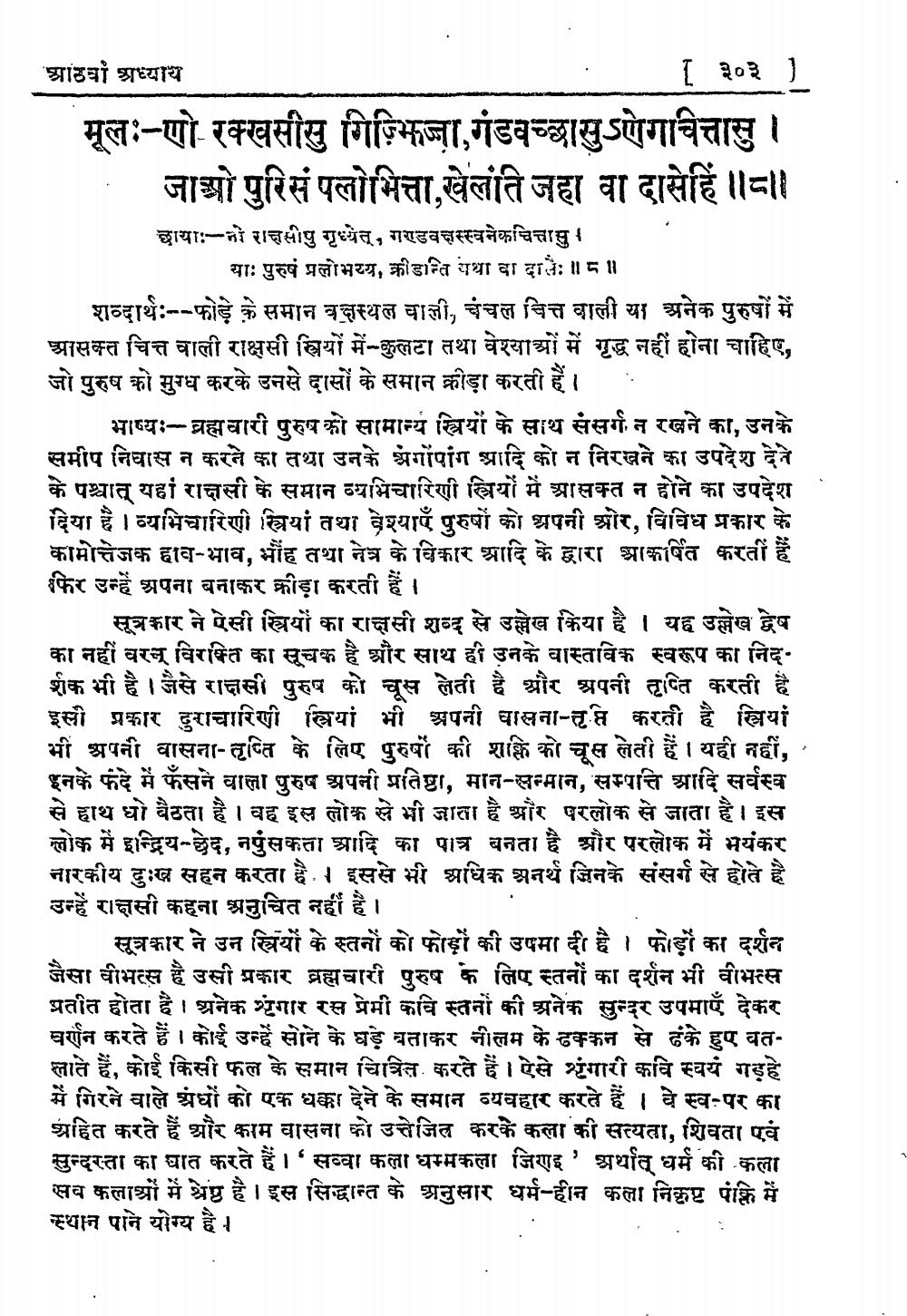________________
आठवां अध्याय
___[ ३०३ ) मूलः-णो रक्खसीसु गिझिजा,गंडवच्छासुऽणेगचित्तासु ।
जाओ पुरिसंपलोभित्ता,खेलति जहा वा दासेहिं ॥८॥ छाया:-नो राक्षसीपु गृध्येत् , गण्डवक्षस्स्वनेकचित्तासु
याः पुरुषं प्रलोभय्य, क्रीडान्ति पथा वा दालः ॥ ८ ॥ शव्दार्थः--फोड़े के समान वक्षस्थल वाली, चंचल चित्त वाली या अनेक पुरुषों में आसक्त चित्त वाली राक्षसी स्त्रियों में-कुलटा तथा वेश्याओं में गृद्ध नहीं होना चाहिए, जो पुरुष को मुग्ध करके उनसे दासों के समान क्रीड़ा करती हैं।
भाष्यः-ब्रह्मवारी पुरुष को सामान्य स्त्रियों के साथ संसर्ग न रखने का, उनके समीप निवास न करने का तथा उनके अंगोपांग श्रादि को न निरखने का उपदेश देने के पश्चात् यहां राक्षली के समान व्यभिचारिणी स्त्रियों में आसक्त न होने का उपदेश दिया है । व्यभिचारिणी स्त्रियां तथा वेश्याएँ पुरुषों को अपनी ओर, विविध प्रकार के कामोत्तेजक हाव-भाव, भौंह तथा नेत्र के विकार आदि के द्वारा आकर्षित करती है फिर उन्हें अपना बनाकर क्रीड़ा करती हैं।
सूत्रकार ने ऐसी स्त्रियों का राक्षसी शब्द से उल्लेख किया है । यह उल्लेख द्वेष का नहीं वरन् विरक्ति का सूचक है और साथ ही उनके वास्तविक स्वरूप का निद. शक भी है । जैसे राक्षसी पुरुष को चूस लेती है और अपनी तृप्ति करती है इसी प्रकार दुराचारिणी स्त्रियां भी अपनी पालना-तृप्त करती है स्त्रियां भी अपनी वासना-तृप्ति के लिए पुरुषों की शक्ति को चूस लेती हैं। यही नहीं, इनके फंदे में फंसने वाला पुरुष अपनी प्रतिष्ठा, मान-सन्मान, सम्पत्ति आदि सर्वस्व से हाथ धो बैठता है । वह इल लोक से भी जाता है और परलोक से जाता है। इस लोक में इन्द्रिय-छेद, नपुंसकता आदि का पात्र बनता है और परलोक में भयंकर नारकीय दुःख सहन करता है । इससे भी अधिक अनर्थ जिनके संसर्ग से होते है उन्हें राक्षसी कहना अनुचित नहीं है।
सूत्रकार ने उन स्त्रियों के स्तनों को फोड़ों की उपमा दी है। फोड़ों का दर्शन जैसा वीभत्स है उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष के लिए स्तनों का दर्शन भी वीभत्स प्रतीत होता है। अनेक श्रृंगार रस प्रेमी कवि स्तनों की अनेक सुन्दर उपमाएँ देकर वर्णन करते हैं। कोई उन्हें सोने के घड़े बताकर नीलम के ढक्कन से ढंके हुए बतलाते हैं, कोई किसी फल के समान चित्रित करते हैं। ऐसे शृंगारी कवि स्वयं गड़हे में गिरने वाले अंधों को एक धका देने के समान व्यवहार करते हैं । वे स्व-पर का श्रहित करते हैं और काम वासना को उत्तेजित करके कला की सत्यता, शिवता एवं सुन्दरता का घात करते हैं। 'सव्वा कला धम्मकला जिणइ' अर्थात् धर्म की कला सब कलाओं में श्रेष्ठ है । इस सिद्धान्त के अनुसार धर्म-हीन कला निकृष्ट पंक्ति में स्थान पाने योग्य है।