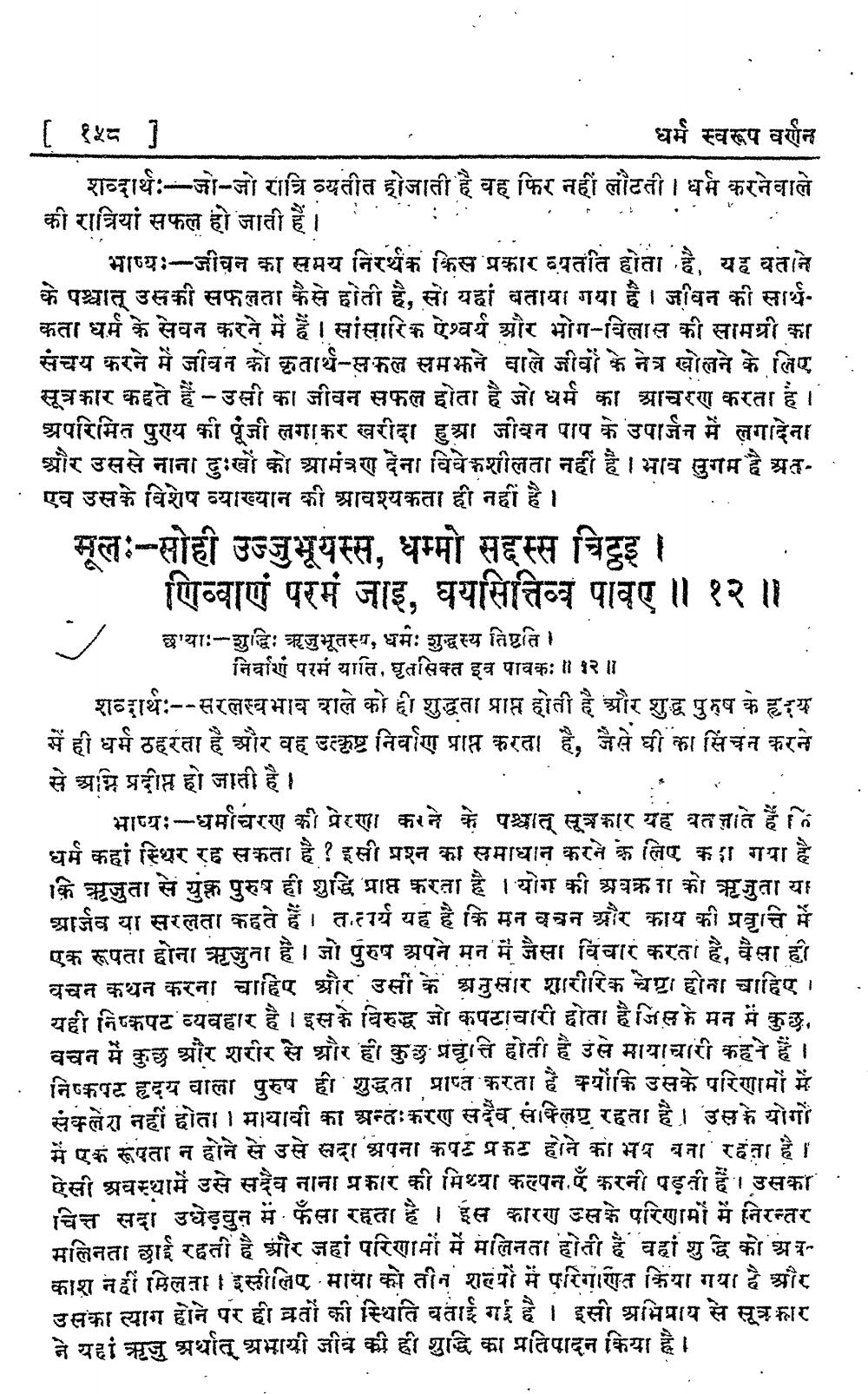________________
[ १५८ ]
धर्म स्वरूप वर्णन
शब्दार्थ : - जो-जो रात्रि व्यतीत होजाती है वह फिर नहीं लौटती । धर्म करनेवाले की रात्रियां सफल हो जाती हैं ।
भाण्यः - जीवन का समय निरर्थक किस प्रकार व्यतति होता है, यह बताने के पश्चात् उसकी सफलता कैसे होती है, सो यहां बताया गया है । जीवन की सार्थकता धर्म के सेवन करने में हैं । सांसारिक ऐश्वर्य और भोग-विलास की सामग्री का संचय करने में जीवन को कृतार्थ- सफल समझने वाले जीवों के नेत्र खोलने के लिए सूत्रकार कहते हैं - उसी का जीवन सफल होता है जो धर्म का आचरण करता है । अपरिमित पुराय की पूंजी लगाकर खरीदा हुआ जीवन पाप के उपार्जन में लगादेना और उससे नाना दुःखों को आमंत्रण देना विवेकशीलता नहीं है । भाव सुगम है ऋतएव उसके विशेष व्याख्यान की आवश्यकता ही नहीं है ।
मूलः - सोही उज्जुभूयस्स, धम्मो सहस्स चिट्ट | व्विाणं परमं जाइ, घयसित्तिव्व पाव ॥ १२ ॥
ン
निर्वाणं परमं याति घृतसिक्त इव पावकः ॥ १२ ॥
शब्दार्थः -- सरलस्वभाव वाले को ही शुद्धता प्राप्त होती है और शुद्ध पुरुष के हृदय
में ही धर्म ठहरता है और वह उत्कृष्ट निर्वाण प्राप्त करता है, जैसे घी का सिंचन करने से अनि प्रदीप्त हो जाती है ।
छया:-शुद्धिः ऋजुभूतस्य, धर्मः शुद्धस्य तिष्ठति ।
भाग्यः -- धर्माचरण की प्रेरणा करने के पश्चात् सूत्रकार यह व
धर्म कहां स्थिर रह सकता है ? इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए कहा गया है कि ऋजुता से युक्त पुरुष ही शुद्धि प्राप्त करता है । योग की अता को ऋजुता या श्रार्जव या सरलता कहते हैं। तत्पर्य यह है कि मन वचन और काय की प्रवृत्ति में एक रूपता होना ऋजुना है । जो पुरुष अपने मन में जैसा विचार करता है, वैसा ही वचन कथन करना चाहिए और उसी के अनुसार शारीरिक चेष्टा होना चाहिए । यही निष्कपट व्यवहार है । इसके विरुद्ध जो कपटाचारी होता है जिसके मन में कुछ, वचन में कुछ और शरीर से और ही कुछ प्रवृत्ति होती है उसे मायाचारी कहते हैं । निष्कपट हृदय वाला पुरुष ही शुद्धता प्राप्त करता है क्योंकि उसके परिणामों में संक्लेरा नहीं होता | मायावी का अन्तःकरण सदैव संक्लिष्ट रहता है । उसके योगों मैं एक रूपता न होने से उसे सदा अपना कपट प्रकट होने का भय बना रहता है । ऐसी अवस्था में उसे सदैव नाना प्रकार की मिथ्या कल्पनाएँ करनी पड़ती है। उसक चित्त सदा उधेड़बुन में फँसा रहता है । इस कारण उसके परिणामों में निरन्तर मलिनता छाई रहती है और जहां परिणामों में मलिनता होती है वहां शुद्वको काश नहीं मिलता। इसीलिए माया को तीन शल्यों में परिगणित किया गया है और उसका त्याग होने पर ही व्रतों की स्थिति बताई गई है । इसी अभिप्राय से सूत्रकार ने यहां ऋजु अर्थात् श्रभायी जीव की ही शुद्धि का प्रतिपादन किया है ।
/