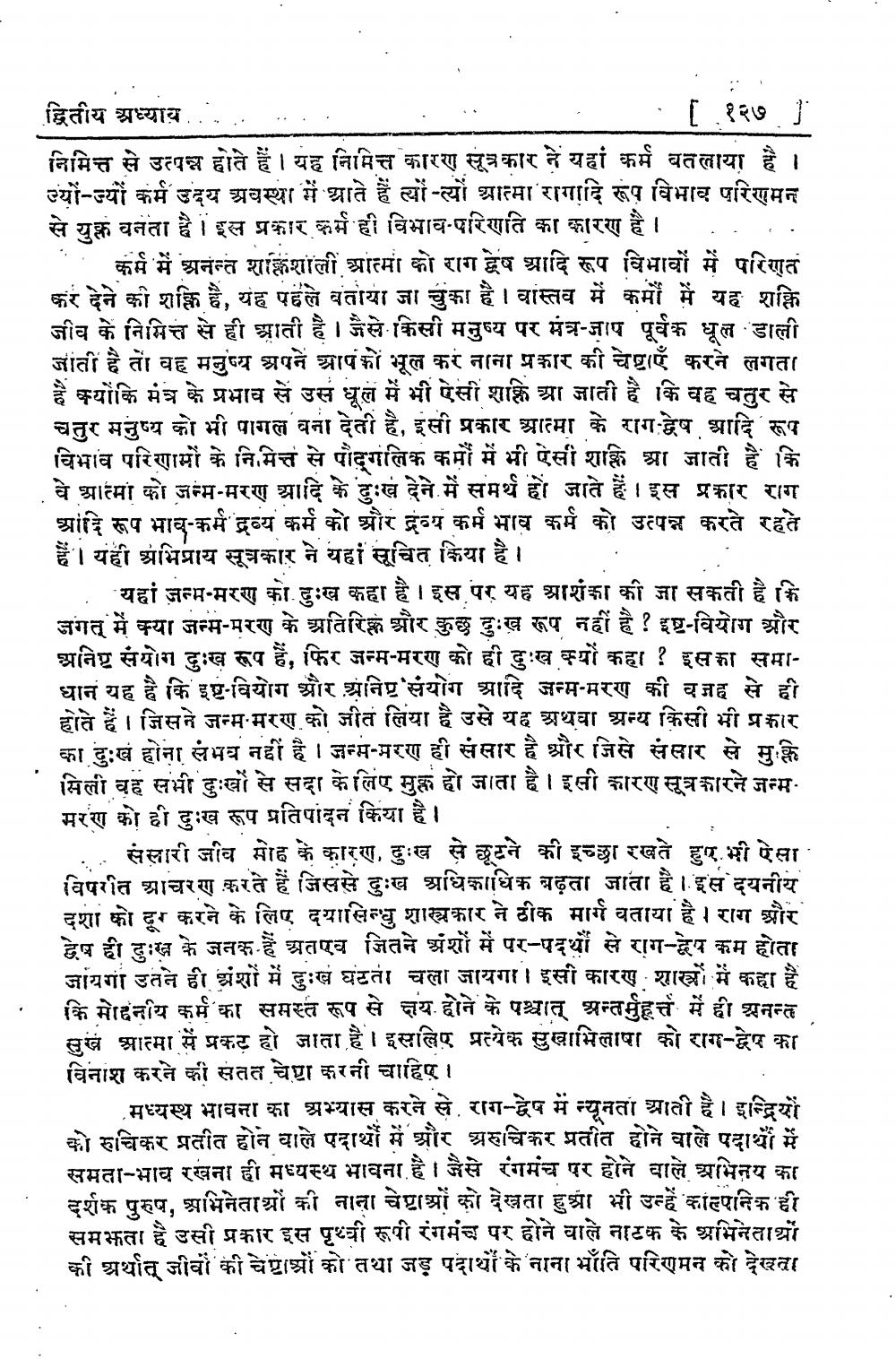________________
द्वितीय अध्याय .. ... ... .
. [ १२७ निमित्त से उत्पन्न होते हैं। यह निमित्त कारण सूत्रकार ने यहां कर्म बतलाया है । ज्यों-ज्यों कर्म उदय अवस्था में आते हैं त्यों-त्यों श्रात्मा रागादि रूप विभाव परिणमन से युक्त बनता है। इस प्रकार कर्म ही विभाव परिणति का कारण है। . . . .
कर्म में अनन्त शक्तिशाली आत्मा को राग द्वेष श्रादि रूप विभावों में परिणत कर देने की शक्ति है, यह पहले बताया जा चुका है । वास्तव में कर्मों में यह शक्ति जीव के निमित्त से ही आती है । जैसे किसी मनुष्य पर मंत्र-जाप पूर्वक धूल डाली जाती है तो वह मनुष्य अपने आप को भूल कर नाना प्रकार की चेष्टाएँ करने लगता है क्योंकि मंत्र के प्रभाव से उस धूल में भी ऐसी शक्ति पा जाती है कि वह चतुर से चतुर मनुष्य को भी पागल बना देती है, इसी प्रकार श्रात्मा के राग द्वेष आदि रूप विभाव परिणामों के निमित्त से पौद्गलिक कर्मों में भी ऐसी शक्ति पा जाती हैं कि वे आत्मा को जन्म-मरण आदि के दुःख देने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार राग
आदि रूप भाव-कर्म द्रव्य कर्म को और द्रव्य कर्म भाव कर्म को उत्पन्न करते रहते हैं। यही अभिप्राय सूत्रकार ने यहां सूचित किया है।
... यहां जन्म-मरण को. दुःख कहा है । इस पर यह आशंका की जा सकती है कि जगत् में क्या जन्म-मरण के अतिरिक्त और कुछ दुःख रूप नहीं है ? इष्ट-वियोग और अनिष्ट संयोग दुःख रूप हैं, फिर जन्म-मरण को ही दुःख क्यों कहा ? इसका समाधान यह है कि इष्ट-वियोग और अनिष्ट संयोग आदि जन्म-मरण की वजह से ही होते हैं। जिसने जन्म-मरण को जीत लिया है उसे यह अथवा अन्य किसी भी प्रकार का दुःखं होना संभव नहीं है । जन्म-मरण ही संसार है और जिसे संसार से मकि मिली वह सभी दुःखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसी कारण सूत्रकारने जन्म मरण को ही दुःख रूप प्रतिपादन किया है।
संसारी जीव मोह के कारण, दुःख से छूटने की इच्छा रखते हुए भी ऐसा विपरीत आचरण करते हैं जिससे दुःख अधिकाधिक बढ़ता जाता है। इस दयनीय दशा को दूर करने के लिए दयासिन्धु शास्त्रकार ने ठीक मार्ग बताया है। राग और द्वेष ही दुःख के जनक है अतएव जितने अंशों में पर-पदों से राग-द्वेष कम होता जायगा उतने ही अंशों में दुःखं घटता चला जायगा। इसी कारण शास्त्रों में कहा हैं कि मोहनीय कर्म का समस्त रूप से क्षय होने के पश्चात् अन्तर्मुहूर्त में ही अनन्त सुखं आत्मा से प्रकट हो जाता है । इसलिए प्रत्येक सुखाभिलाषा को राग-द्वेष का विनाश करने की सतत चेष्टा करनी चाहिए।
मध्यस्थ भावना का अभ्यास करने से राग-द्वेष में न्यूनता पाती है। इन्द्रियों को रुचिकर प्रतीत होने वाले पदार्थों में और अरुचिकर प्रतीत होने वाले पदार्थो में समता-भाव रखना ही मध्यस्थ भावना है । जैसे रंगमंच पर होने वाले अभिनय का दर्शक पुरुष, अभिनेताओं की नाना चेष्टाओं को देखता हुआ भी उन्हें काल्पनिक ही समझता है उसी प्रकार इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर होने वाले नाटक के अभिनेताओं की अर्थात् जीवों की चेष्टाओं को तथा जड़ पदार्थों के नाना भाँति परिणमन को देखता