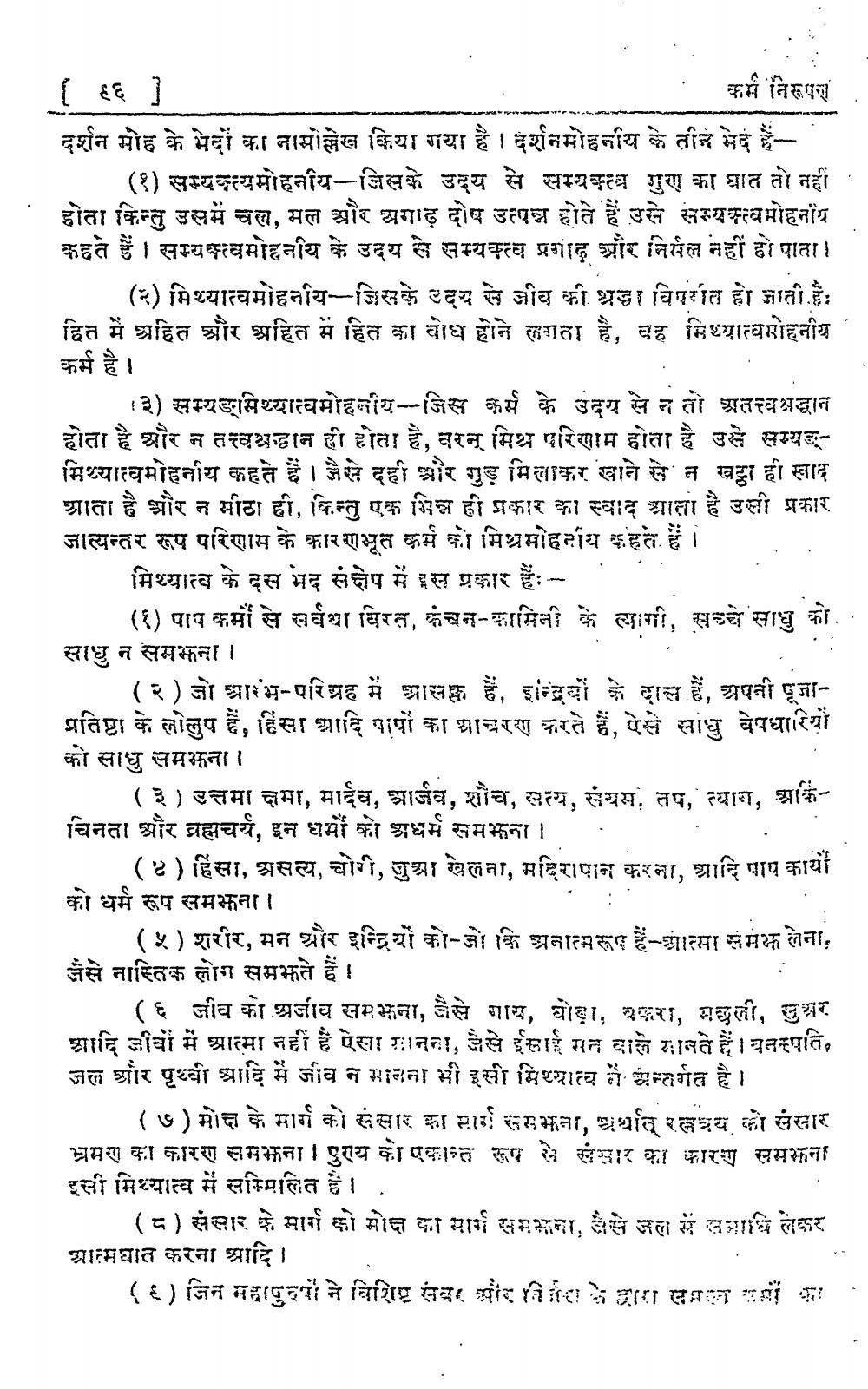________________
[१६]
कर्म निरूपण दर्शन मोह के भेदों का नामोल्लेख किया गया है। दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं
(१) सम्यक्त्यमोहनीय-जिसके उदय से सम्यक्त्व गुण का घात तो नहीं होता किन्तु उसमें चल, मल और अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं उसे सस्यस्त्वमोहनीय कहते हैं । सम्यक्त्वमोहनीय के उदय से सम्यक्त्व प्रगाढ़ और निरल नहीं हो पाता।
(२) मिथ्यात्वमोहनीय-जिसके उदय से जीव की श्रद्धा विपर्शल हो जाती है। हित में अहित और अहित में हित का वोध होने लगता है, वह मिथ्यात्वमोहनीय कर्म है।
३) सम्यमिथ्यात्वमोहनीय-जिस कर्म के उदय से न तो अतत्त्वश्रद्धान होता है और न तत्त्वश्रद्धान ही होता है, वरन् मिश्र परिणाम होता है उसे समयमिथ्यात्वमोहनीय कहते हैं। जैसे दही और गुड़ मिलाकर खाने से न खट्टा ही स्वाद पाता है और न मीठा ही, किन्तु एक मिन ही प्रकार का स्वाद अाता है उसी प्रकार जात्यन्तर रूप परिणाम के कारणभूत कर्म को मिश्रमोहनीय कहते हैं ।
मिथ्यात्व के दस भेद संक्षेप में इस प्रकार हैं:
(१) पाप कर्मों से सर्वथा विरत, कंचन-कामिनी के त्यागी, सच्चे साधु को साधु न समझना।
(२) जो श्रारंभ-परिग्रह में श्रासक हैं, इन्द्रियों के दाल हैं, अपनी पूजाप्रतिष्ठा के लोलुप हैं, हिंसा भादि गापों का प्राचरण करते हैं, ऐसे साधु वेषधारियों को साधु समझना।
(३) उत्तमा क्षमा, मार्दव, प्रार्जव, शौच, लत्य, संयम, तप, त्याग, अर्किचिनता और ब्रह्मचर्य, इन धर्मो को अधर्म समझना ।
(४) हिंसा, असत्य, चोरी, जुआ खेलना, मदिरापान करना, श्रादि पाप कार्यों को धर्म रूप समझना।
(५) शरीर, मन और इन्द्रियों को-जो कि अनात्मरूप हैं-श्रात्सा समझ लेना, जैसे नास्तिक लोग समझते हैं।
(६ जीव को अर्जाच समभना, जैले गाय, घोड़ा, सरा, मछली, सुआर श्रादि जीवों में श्रात्मा नहीं हैं ऐसा मानना, जैसे ईसाई मन बाले मानते हैं । बनस्पति जल और पृथ्वी श्रादि में जीव न मानना भी इसी मिथ्यात्व ने अन्तर्गत है।
(७) मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समभाना, अर्थात् रसत्रय को संसार भ्रमण का कारण समझना । पुण्य को एकान्त रूप से संसार का कारण समझना इसी मिथ्यात्व में सम्मिलित हैं। .
(८) संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझाना, जैसे जल में समाधि लेकर अात्मघात करना आदि।
(६) जिन महापुरषों ने विशिष्ट संकर और निशा के द्वारा सारा करा