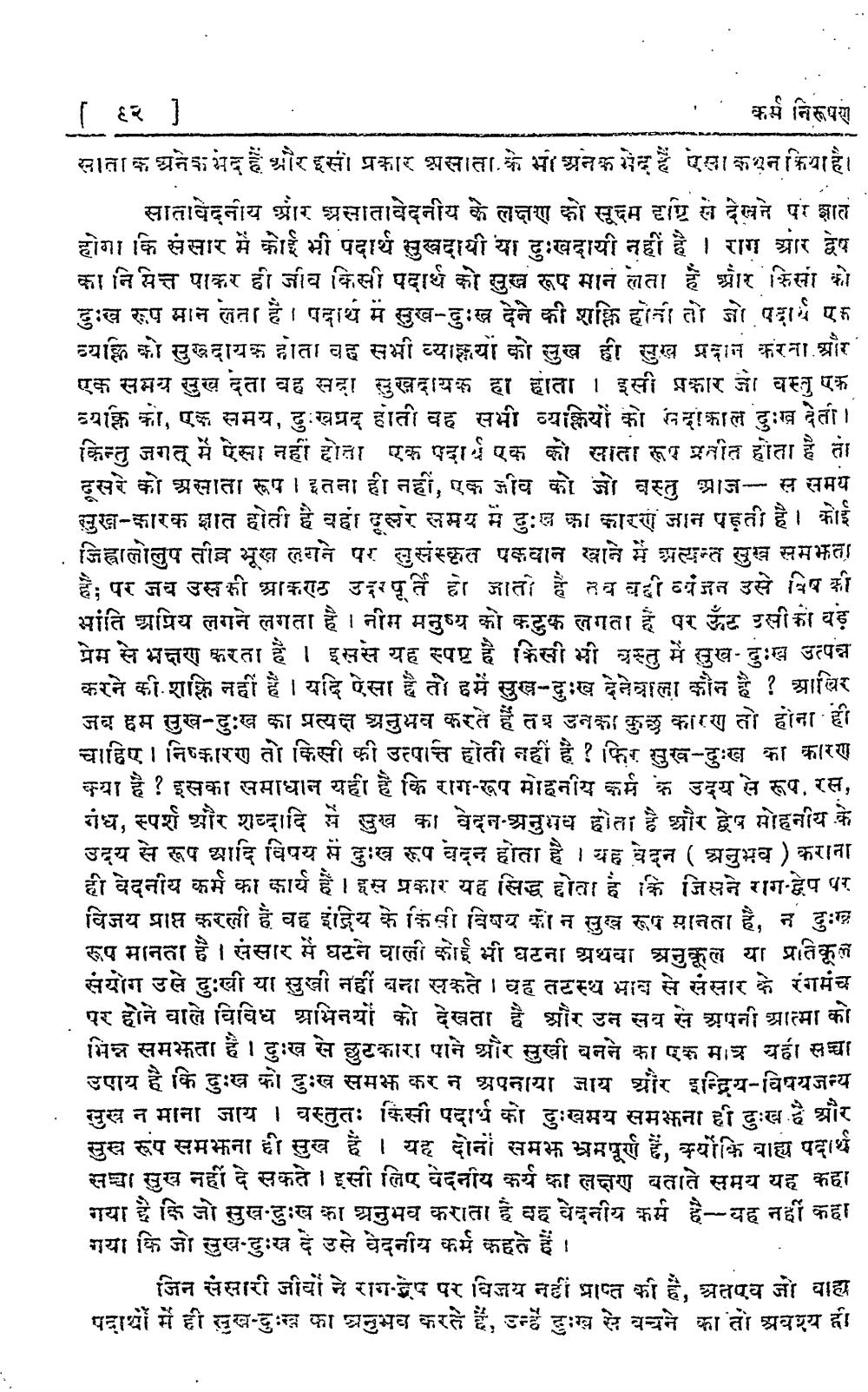________________
[ २ ]
.. कर्म निरूपण साताक अनेक भेद हैं और इसी प्रकार असाता के भी अनक भेद हैं ऐसा कथन किया है।
सातावेदनीय और असातावेदनीय के लक्षण को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ज्ञात होगा कि संसार में कोई भी पदार्थ सुखदायी या दुःखदायी नहीं है । राग और द्वेष का नि सत्त पाकर ही जीव किसी पदार्थ को सुख रूप मान लाता है और किसी को दुःख रूप मान लेता है। पदार्थ में सुख-दुःस्त्र देने की शक्ति होती तो जो पदार्थ एक व्यक्ति को सुखदायक होता वह सभी व्यालयों को सुख ही सुख प्रदान करना और एक समय सुख दता वह सदा सुखदायक हा हाता । इसी प्रकार जो वस्तु एक व्यक्ति को, एक समय, दुःखप्रद होती वह सभी व्यक्तियों को सदाकाल दुःख देती। किन्तु जगत् में ऐसा नहीं होता एक पदार्थ एक को साता रूप प्रतीत होता है तो दूसरे को असाता रूप । इतना ही नहीं, एक जीव को जो वस्तु प्राज- स समय सुख-कारक ज्ञात होती है वही दूलर लमय में दुःख का कारण जान पड़ती है। कोई जिह्वालोलुप तीन भूख लगने पर सुसंस्कृत पकवान खाने में अत्यन्त सुख समझता है; पर जब उसकी प्राकण्ठ उदर पूर्त हो जाती है तब बद्दी व्यंजन उसे विष की भांति अप्रिय लगने लगता है । नीम मनुष्य को कटुक लगता हैं पर ऊँट उसी को बड़ प्रेम से भक्षण करता है। इससे यह स्पष्ट है किसी भी वस्तु में सुख-दुःख उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है । यदि ऐसा है तो हमें सुख-दुःख देनेवाला कौन है ? आखिर जब हम सुख-दुःख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तत्र उनका कुछ कारण तो होना ही चाहिए । निष्कारण तो किसी की उत्पत्ति होती नहीं है ? फिर सुख-दुःख का कारण क्या है ? इसका समाधान यही है कि राग-रूप मोहनीय कर्म के उदय से रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दादि में सुख का वेदन-अनुभव होता है और द्वेष मोहनीय के उदय से रूप श्रादि विषय में दुःख रूप बदन होता है । यह वेदन ( अनुभव ) कराना ही वेदनीय कर्म का कार्य हैं । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जिसने राग-द्वेप पर विजय प्राप्त करली है वह इंद्रिय के किसी विषय को न सुख रूप मानता है, न दुःपन्न रूप मानता है। संसार में घटने वाली कोई भी घटना अथवा अनुकूल या प्रतिकूल संयोग उले दुःखी या सुखी नहीं बना सकते । वह तटस्थ भाव से संसार के रंगमंच पर होने वाले विविध अभिनयों को देखता है और उन सब से अपनी आत्मा को भिन्न समझता है । दुःख से छुटकारा पाने और सुखी बनने का एक मात्र यही सच्चा उपाय है कि दुःख को दुःख समझ कर न अपनाया जाय और इन्द्रिय-विषयजन्य सुख न माना जाय । वस्तुतः किसी पदार्थ को दुःखमय समझना ही दुःख है और सुख रूप समझना ही सुख है । यह दोनों समझ भ्रमपूर्ण है, क्योंकि बाह्य पदार्थ सच्चा सुख नहीं दे सकते । इसी लिए वेदनीय कर्य का लक्षण बताते समय यह कहा गया है कि जो सुख दुःख का अनुभव कराता है वह वेदनीय कर्म है-यह नहीं कहा गया कि जो सुख दुःख दे उसे वेदनीय कर्म कहते हैं।
जिन संसारी जीवों ने राग-द्रेप पर विजय नहीं प्राप्त की है, अतएव जो वाहा पदार्थों में ही सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, उन्हें दुःख से बचने का तो अवश्य ही