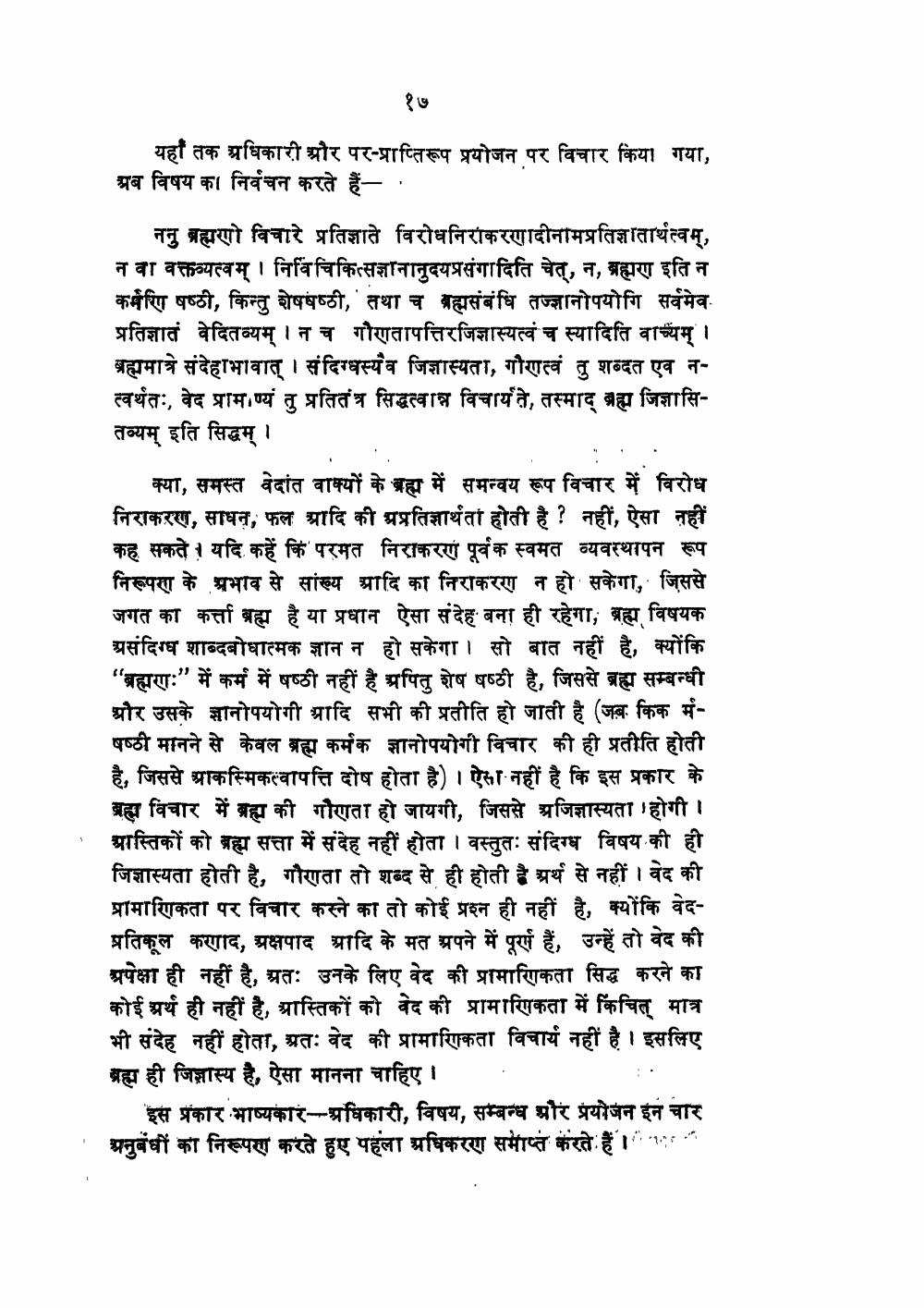________________
यहाँ तक अधिकारी और पर-प्राप्तिरूप प्रयोजन पर विचार किया गया, अब विषय का निर्वचन करते हैं- .
ननु ब्रह्मणो विचारे प्रतिज्ञाते विरोधनिराकरणादीनामप्रतिज्ञातार्थत्वम्, न वा वक्तव्यत्वम् । निवि चिकित्सज्ञानानुदयप्रसंगादिति चेत्, न, ब्रह्मण इति न कर्मरिण षष्ठी, किन्तु शेषषष्ठी, तथा च ब्रह्मसंबंधि तज्ज्ञानोपयोगि सर्वमेवप्रतिज्ञातं वेदितव्यम् । न च गौणतापत्तिरजिज्ञास्यत्वं च स्यादिति वाच्यम् । ब्रह्ममात्रे संदेहाभावात् । संदिग्धस्यैव जिज्ञास्यता, गौणत्वं तु शब्दत एव नत्वर्थतः, वेद प्रामाण्यं तु प्रतितंत्र सिद्धत्वान्न विचार्य ते, तस्माद् ब्रह्म जिज्ञासितव्यम् इति सिद्धम् ।
क्या, समस्त वेदांत वाक्यों के ब्रह्म में समन्वय रूप विचार में विरोध निराकरण, साधन, फल आदि की अप्रतिज्ञार्थता होती है ? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। यदि कहें कि परमत निराकरण पूर्वक स्वमत व्यवस्थापन रूप निरूपण के प्रभाव से सांख्य आदि का निराकरण न हो सकेगा, जिससे जगत का कर्ता ब्रह्म है या प्रधान ऐसा संदेह बना ही रहेगा; ब्रह्म विषयक असंदिग्ध शाब्दबोधात्मक ज्ञान न हो सकेगा। सो बात नहीं है, क्योंकि "ब्रह्मणः" में कर्म में षष्ठी नहीं है अपितु शेष षष्ठी है, जिससे ब्रह्म सम्बन्धी और उसके ज्ञानोपयोगी आदि सभी की प्रतीति हो जाती है (जब किक मंषष्ठी मानने से केवल ब्रह्म कर्मक ज्ञानोपयोगी विचार की ही प्रतीति होती है, जिससे आकस्मिकत्वापत्ति दोष होता है)। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के ब्रह्म विचार में ब्रह्म की गौणता हो जायगी, जिससे अजिज्ञास्यता होगी। आस्तिकों को ब्रह्म सत्ता में संदेह नहीं होता । वस्तुतः संदिग्ध विषय की ही जिज्ञास्यता होती है, गौणता तो शब्द से ही होती है अर्थ से नहीं । वेद की प्रामाणिकता पर विचार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वेदप्रतिकूल कणाद, अक्षपाद आदि के मत अपने में पूर्ण हैं, उन्हें तो वेद की अपेक्षा ही नहीं है, अतः उनके लिए वेद की प्रामाणिकता सिद्ध करने का कोई अर्थ ही नहीं है, आस्तिकों को वेद की प्रामाणिकता में किंचित् मात्र भी संदेह नहीं होता, अतः वेद की प्रामाणिकता विचार्य नहीं है । इसलिए ब्रह्म ही जिज्ञास्य है, ऐसा मानना चाहिए।
इस प्रकार भाष्यकार-अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन इन चार अनुबंधों का निरूपण करते हुए पहला अधिकरण समाप्त करते हैं ।। १