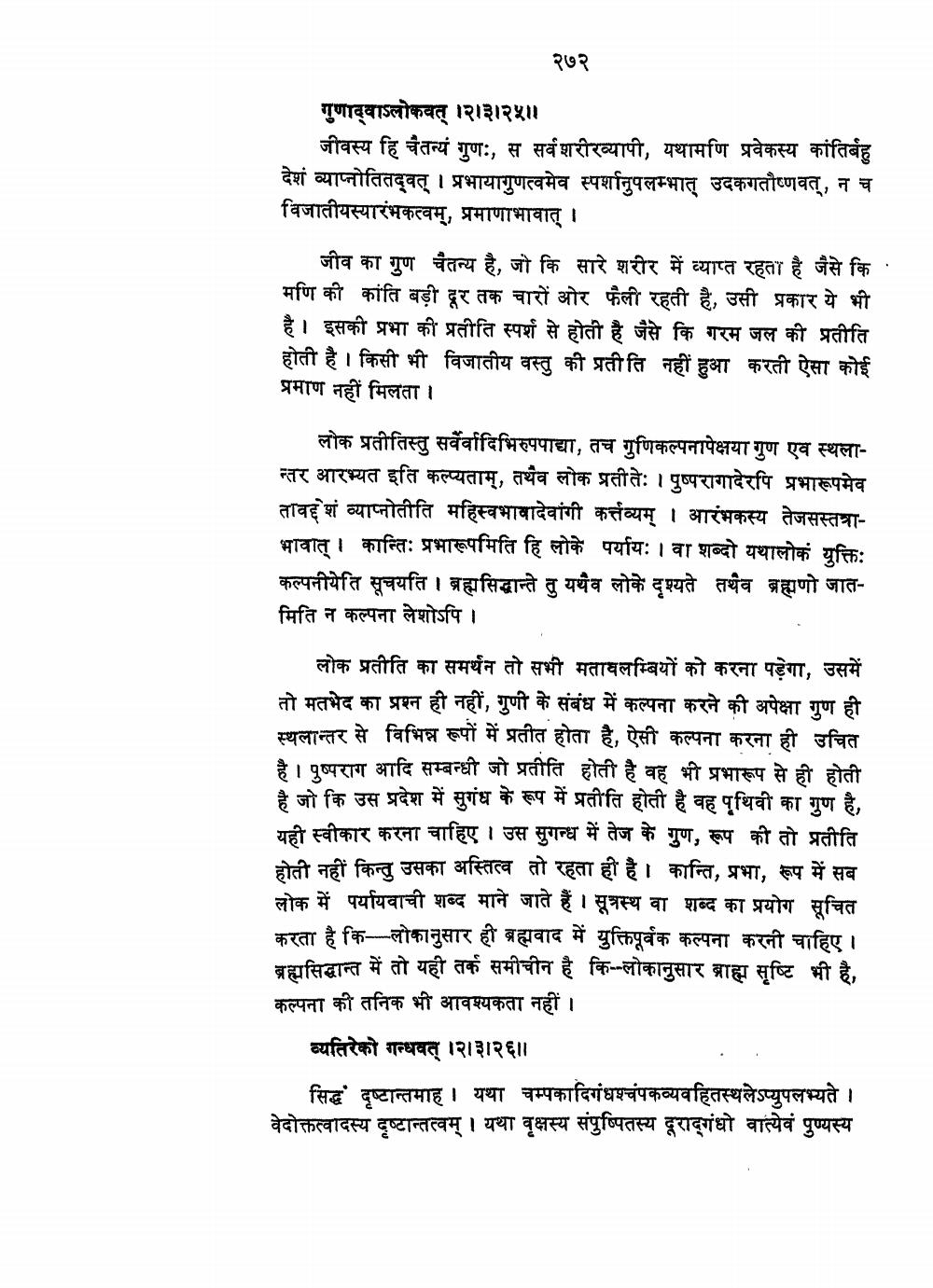________________
२७२
गुणाद्वाऽलोकवत् ॥२॥३॥२५॥
जीवस्य हि चैतन्यं गुणः, स सर्व शरीरव्यापी, यथामणि प्रवेकस्य कांतिर्बहु देशं व्याप्नोतितद्वत् । प्रभायागुणत्वमेव स्पर्शानुपलम्भात् उदकगतोष्णवत्, न च विजातीयस्यारंभकत्वम्, प्रमाणाभावात् ।
जीव का गुण चैतन्य है, जो कि सारे शरीर में व्याप्त रहता है जैसे कि मणि की कांति बड़ी दूर तक चारों ओर फैली रहती है, उसी प्रकार ये भी है। इसकी प्रभा की प्रतीति स्पर्श से होती है जैसे कि गरम जल की प्रतीति होती है। किसी भी विजातीय वस्तु की प्रतीति नहीं हुआ करती ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता।
लोक प्रतीतिस्तु सर्वैर्वादिभिरुपपाद्या, तच गुणिकल्पनापेक्षया गुण एव स्थलान्तर आरभ्यत इति कल्प्यताम्, तथैव लोक प्रतीतेः । पुष्परागादेरपि प्रभारूपमेव तावद्देशं व्याप्नोतीति महिस्वभावादेवांगी कर्त्तव्यम् । आरंभकस्य तेजसस्तत्राभावात् । कान्तिः प्रभारूपमिति हि लोके पर्यायः । वा शब्दो यथालोकं युक्तिः कल्पनीयेति सूचयति । ब्रह्मसिद्धान्ते तु यथैव लोके दृश्यते तथैव ब्रह्मणो जातमिति न कल्पना लेशोऽपि ।
लोक प्रतीति का समर्थन तो सभी मतावलम्बियों को करना पड़ेगा, उसमें तो मतभेद का प्रश्न ही नहीं, गुणी के संबंध में कल्पना करने की अपेक्षा गुण ही स्थलान्तर से विभिन्न रूपों में प्रतीत होता है, ऐसी कल्पना करना ही उचित है। पुष्पराग आदि सम्बन्धी जो प्रतीति होती है वह भी प्रभारूप से ही होती है जो कि उस प्रदेश में सुगंध के रूप में प्रतीति होती है वह पृथिवी का गुण है, यही स्वीकार करना चाहिए। उस सुगन्ध में तेज के गुण, रूप की तो प्रतीति होती नहीं किन्तु उसका अस्तित्व तो रहता ही है। कान्ति, प्रभा, रूप में सब लोक में पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं । सूत्रस्थ वा शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि-लोकानुसार ही ब्रह्मवाद में युक्तिपूर्वक कल्पना करनी चाहिए। ब्रह्मसिद्धान्त में तो यही तर्क समीचीन है कि--लोकानुसार ब्राह्म सृष्टि भी है, कल्पना की तनिक भी आवश्यकता नहीं।
व्यतिरेको गन्धवत् ।२।३।२६॥
सिद्ध दृष्टान्तमाह । यथा चम्पकादिगंधश्चंपकव्यवहितस्थलेऽप्युपलभ्यते । वेदोक्तत्वादस्य दृष्टान्तत्वम् । यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य दूराद्गंधो वात्येवं पुण्यस्य