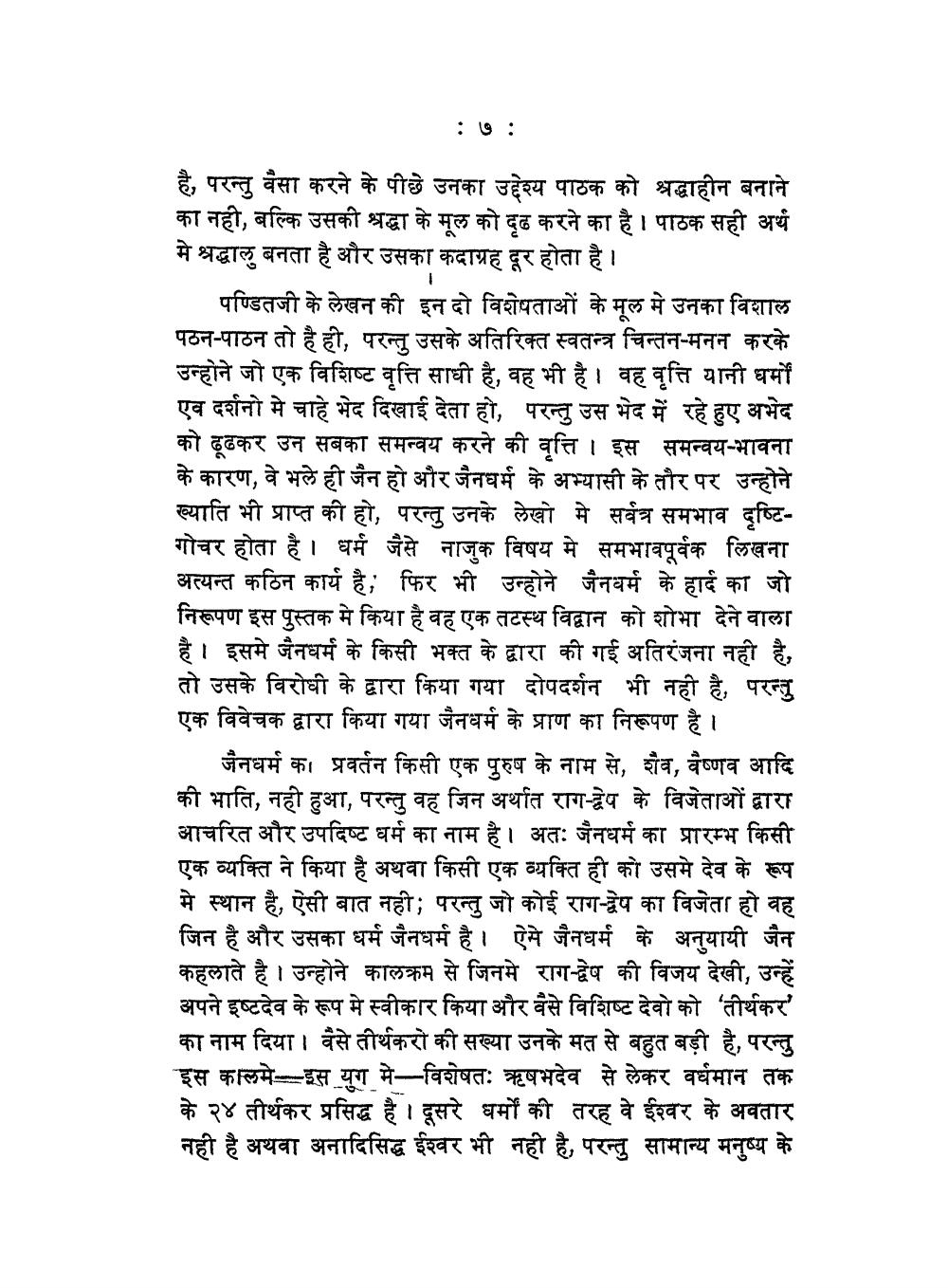________________
है, परन्तु वैसा करने के पीछे उनका उद्देश्य पाठक को श्रद्धाहीन बनाने का नही, बल्कि उसकी श्रद्धा के मूल को दृढ करने का है। पाठक सही अर्थ मे श्रद्धालु बनता है और उसका कदाग्रह दूर होता है।
पण्डितजी के लेखन की इन दो विशेषताओं के मूल मे उनका विशाल पठन-पाठन तो है ही, परन्तु उसके अतिरिक्त स्वतन्त्र चिन्तन-मनन करके उन्होने जो एक विशिष्ट वृत्ति साधी है, वह भी है। वह वृत्ति यानी धर्मों एव दर्शनो मे चाहे भेद दिखाई देता हो, परन्तु उस भेद में रहे हुए अभेद को ढूढकर उन सबका समन्वय करने की वृत्ति । इस समन्वय-भावना के कारण, वे भले ही जैन हो और जैनधर्म के अभ्यासी के तौर पर उन्होने ख्याति भी प्राप्त की हो, परन्तु उनके लेखो मे सर्वत्र समभाव दृष्टिगोचर होता है। धर्म जैसे नाजुक विषय मे समभावपूर्वक लिखना अत्यन्त कठिन कार्य है, फिर भी उन्होने जैनधर्म के हार्द का जो निरूपण इस पुस्तक मे किया है वह एक तटस्थ विद्वान को शोभा देने वाला है। इसमे जैनधर्म के किसी भक्त के द्वारा की गई अतिरंजना नही है, तो उसके विरोधी के द्वारा किया गया दोपदर्शन भी नही है, परन्तु एक विवेचक द्वारा किया गया जैनधर्म के प्राण का निरूपण है।
जैनधर्म का प्रवर्तन किसी एक पुरुष के नाम से, शैव, वैष्णव आदि की भाति, नही हुआ, परन्तु वह जिन अर्थात राग-द्वेष के विजेताओं द्वारा आचरित और उपदिष्ट धर्म का नाम है। अतः जैनधर्म का प्रारम्भ किसी एक व्यक्ति ने किया है अथवा किसी एक व्यक्ति ही को उसमे देव के रूप मे स्थान है, ऐसी बात नही; परन्तु जो कोई राग-द्वेष का विजेता हो वह जिन है और उसका धर्म जैनधर्म है। ऐसे जैनधर्म के अनुयायी जैन कहलाते है । उन्होने कालक्रम से जिनमे राग-द्वेष की विजय देखी, उन्हें अपने इष्टदेव के रूप मे स्वीकार किया और वैसे विशिष्ट देवो को 'तीर्थकर' का नाम दिया। वैसे तीर्थकरो की संख्या उनके मत से बहुत बड़ी है, परन्तु इस कालमे-इस युग मे-विशेषतः ऋषभदेव से लेकर वर्धमान तक के २४ तीर्थकर प्रसिद्ध है । दूसरे धर्मों की तरह वे ईश्वर के अवतार नही है अथवा अनादिसिद्ध ईश्वर भी नही है, परन्तु सामान्य मनुष्य के