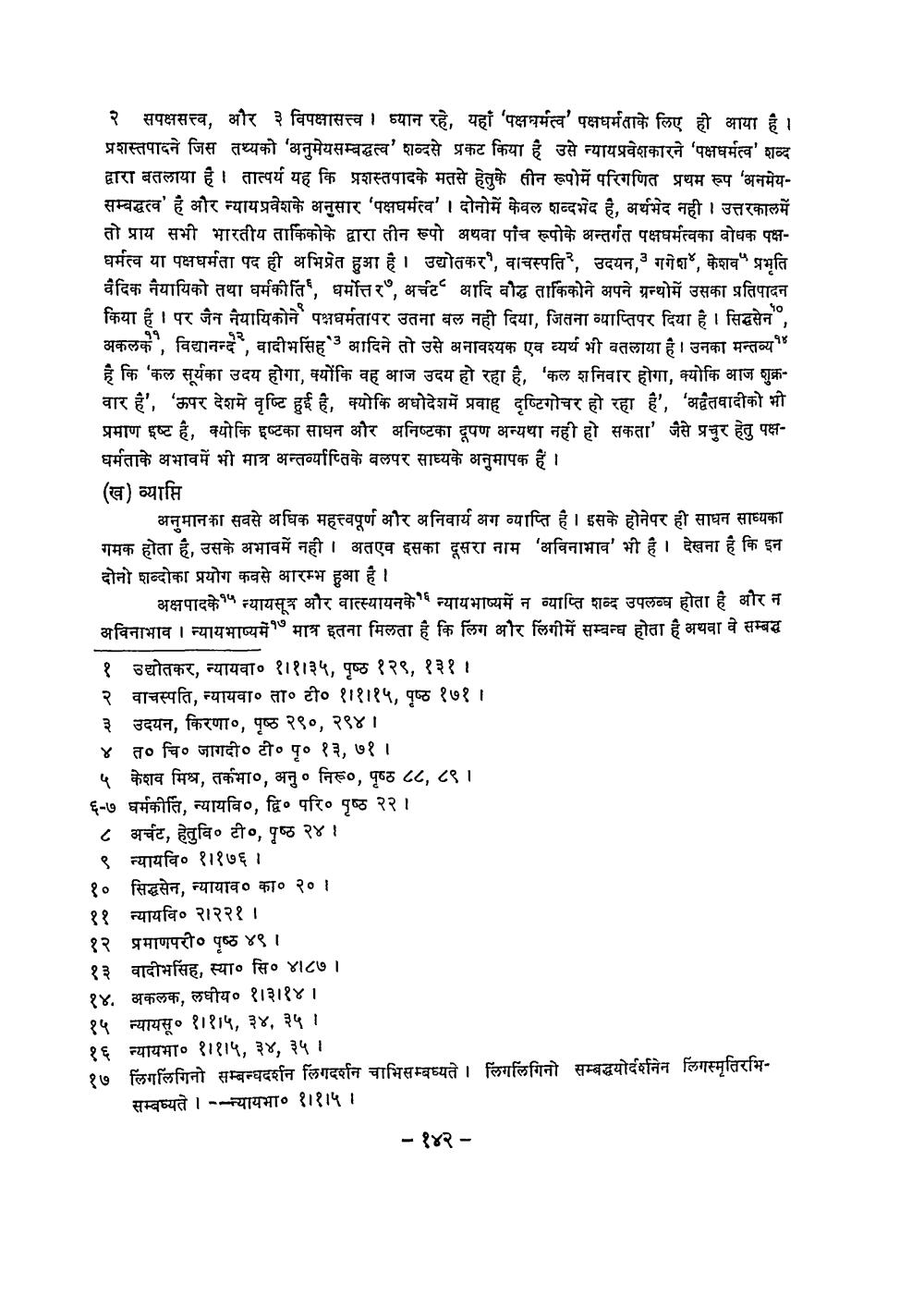________________
२ सपक्षसत्त्व, और ३ विपक्षासत्त्व । ध्यान रहे, यहाँ 'पक्षधर्मत्व' पक्षधर्मताके लिए ही आया है। प्रशस्तपादने जिस तथ्यको 'अनुमयसम्बद्धत्व' शब्दसे प्रकट किया है उसे न्यायप्रवेशकारने 'पक्षधर्मत्व' शब्द द्वारा बतलाया है। तात्पर्य यह कि प्रशस्तपादके मतसे हेतुके तीन रूपोमें परिगणित प्रथम रूप 'अनमेयसम्बद्धत्व' है और न्यायप्रवेशके अनुसार 'पक्षधर्मत्व' । दोनोमें केवल शब्दभेद है, अर्थभेद नही । उत्तरकालमें तो प्राय सभी भारतीय ताकिकोके द्वारा तीन रूपो अथवा पांच रूपोके अन्तर्गत पक्षधर्मत्वका बोधक पक्षधर्मत्व या पक्षधर्मता पद ही अभिप्रेत हुआ है। उद्योतकर', वाचस्पति२, उदयन, गगेश, केशव प्रभृति वैदिक नैयायिको तथा धर्मकीति, धर्मोत्तर, अर्चट आदि बौद्ध ताकिकोने अपने ग्रन्थोमें उसका प्रतिपादन किया है । पर जैन नैयायिकोने पक्षधर्मतापर उतना बल नही दिया, जितना व्याप्तिपर दिया है । सिद्धसेन', अकलक', विद्यानन्द , वादीभसिंह आदिने तो उसे अनावश्यक एव व्यर्थ भी बतलाया है। उनका मन्तव्य है कि 'कल सूर्यका उदय होगा, क्योंकि वह आज उदय हो रहा है, 'कल शनिवार होगा, क्योकि आज शुक्रवार है', 'ऊपर देशमे वृष्टि हुई है, क्योकि अघोदेशमें प्रवाह दृष्टिगोचर हो रहा है', 'अद्वैतवादीको भी प्रमाण इष्ट है, क्योकि इष्टका साधन और अनिष्टका दूपण अन्यथा नही हो सकता' जैसे प्रचुर हेतु पक्षधर्मताके अभावमें भी मात्र अन्तर्व्याप्तिके बलपर साध्यके अनुमापक हैं। (ख) व्याप्ति
अनुमानका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य अग व्याप्ति है। इसके होनेपर ही साधन साध्यका गमक होता है, उसके अभावमें नही। अतएव इसका दूसरा नाम 'अविनाभाव' भी है। देखना है कि इन दोनो शब्दोका प्रयोग कबसे आरम्भ हुआ है।
अक्षपादके १५ न्यायसूत्र और वात्स्यायनके ६ न्यायभाष्यमें न व्याप्ति शब्द उपलब्ध होता है और न अविनाभाव । न्यायभाष्यमें मात्र इतना मिलता है कि लिंग और लिंगीमें सम्बन्ध होता है अथवा वे सम्बद्ध
१ उद्योतकर, न्यायवा० १।१।३५, पृष्ठ १२९, १३१ । २ वाचस्पति, न्यायवा० ता० टी० १११११५, पृष्ठ १७१ । ३ उदयन, किरणा०, पृष्ठ २९०, २९४ । ४ त० चि० जागदी०टी० पृ० १३, ७१ । ५ केशव मिश्र, तर्कभा०, अनु० निरू०, पृष्ठ ८८, ८९ । ६-७ धर्मकीर्ति, न्यायबि०, द्वि० परि० पृष्ठ २२ । ८ अर्चट, हेतुवि० टी०, पृष्ठ २४ । ९ न्यायवि० १११७६ । १० सिद्धसेन, न्यायाव० का० २० । ११ न्यायवि० २।२२१ । १२ प्रमाणपरी० पृष्ठ ४९ । १३ वादीभसिंह, स्या० सि० ४४८७ । १४. अकलक, लघीय० १।३।१४ । १५ न्यायसू० ११११५, ३४, ३५ । १६ न्यायभा० ११११५, ३४, ३५ । १७ लिंगलिंगिनो सम्बन्धदर्शन लिंगदर्शन चाभिसम्बध्यते । लिंगलिंगिनो सम्बद्धयोर्दर्शनेन लिंगस्मृतिरभि
सम्बध्यते । --न्यायभा० १११।५ ।