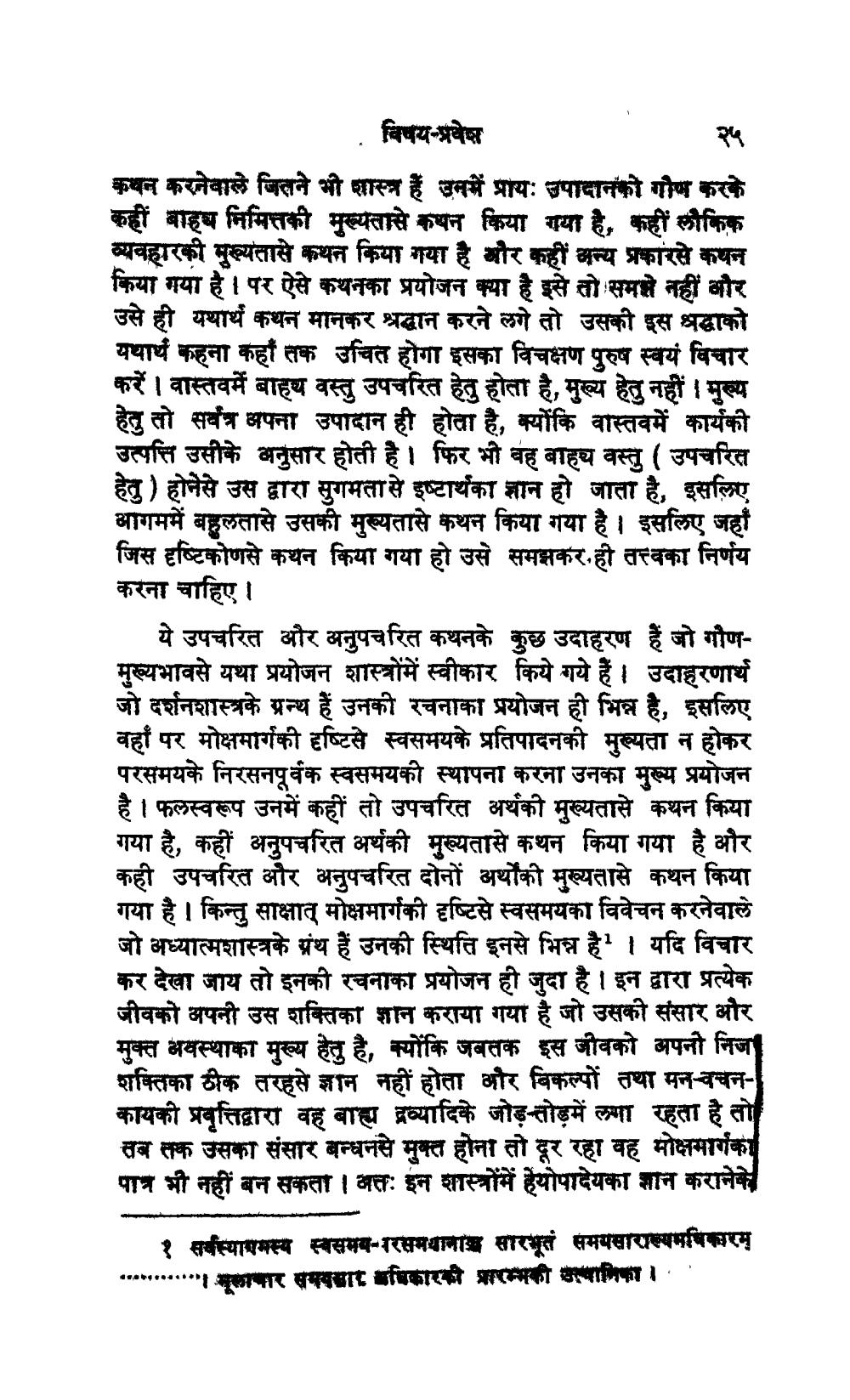________________
विषय-प्रवेश
कथन करनेवाले जितने भी शास्त्र हैं उनमें प्रायः उपादानको गौण करके कहीं बाहय निमित्तकी मुख्यतासे कथन किया गया है, कहीं लौकिक व्यवहारकी मुख्यतासे कथन किया गया है और कहीं अन्य प्रकारसे कथन किया गया है। पर ऐसे कथनका प्रयोजन क्या है इसे तो समझे नहीं और उसे ही यथार्थ कथन मानकर श्रद्धान करने लगे तो उसकी इस श्रद्धाको यथार्थ कहना कहाँ तक उचित होगा इसका विचक्षण पुरुष स्वयं विचार करें। वास्तवमें बाहय वस्तु उपचरित हेतु होता है, मुख्य हेतु नहीं । मुख्य हेतु तो सर्वत्र अपना उपादान ही होता है, क्योंकि वास्तवमें कार्यकी उत्पत्ति उसीके अनुसार होती है। फिर भी वह बाहय वस्तु (उपचरित हेतु) होनेसे उस द्वारा सुगमतासे इष्टार्थका ज्ञान हो जाता है, इसलिए आगममें बहुलतासे उसकी मुख्यतासे कथन किया गया है। इसलिए जहाँ जिस दृष्टिकोणसे कथन किया गया हो उसे समझकर ही तत्त्वका निर्णय करना चाहिए।
ये उपचरित और अनुपचरित कथनके कुछ उदाहरण हैं जो गौणमुख्यभावसे यथा प्रयोजन शास्त्रोंमें स्वीकार किये गये हैं। उदाहरणार्थ जो दर्शनशास्त्रके ग्रन्थ हैं उनकी रचनाका प्रयोजन ही भिन्न है, इसलिए वहाँ पर मोक्षमार्गकी दृष्टिसे स्वसमयके प्रतिपादनकी मुख्यता न होकर परसमयके निरसनपूर्वक स्वसमयकी स्थापना करना उनका मुख्य प्रयोजन है । फलस्वरूप उनमें कहीं तो उपचरित अर्थकी मुख्यतासे कथन किया गया है, कहीं अनुपचारित अर्थकी मुख्यतासे कथन किया गया है और कही उपचरित और अनुपचरित दोनों अर्थोकी मुख्यतासे कथन किया गया है । किन्तु साक्षात् मोक्षमार्गकी दृष्टिसे स्वसमयका विवेचन करनेवाले जो अध्यात्मशास्त्रके ग्रंथ हैं उनकी स्थिति इनसे भिन्न है । यदि विचार कर देखा जाय तो इनकी रचनाका प्रयोजन ही जुदा है । इन द्वारा प्रत्येक जीवको अपनी उस शक्तिका ज्ञान कराया गया है जो उसकी संसार और मुक्त अवस्थाका मुख्य हेतु है, क्योंकि जबतक इस जीवको अपनी निज शक्तिका ठीक तरहसे ज्ञान नहीं होता और विकल्पों तथा मन वचनकायकी प्रवृत्तिद्वारा वह बाह्य द्रव्यादिके जोड़-तोड़में लगा रहता है तो सब तक उसका संसार बन्धनसे मुक्त होना तो दूर रहा वह मोक्षमार्गका पात्र भी नहीं बन सकता । अक्तः इन शास्त्रोंमें हेयोपादेयका ज्ञान कराने के
१ सर्वस्याषमस्व स्वसमव-भरसमयानाश सारभूतं समयसारख्यमधिकारम ...........मलापार समयसार अधिकारको प्रारम्भको अत्यानिका ।