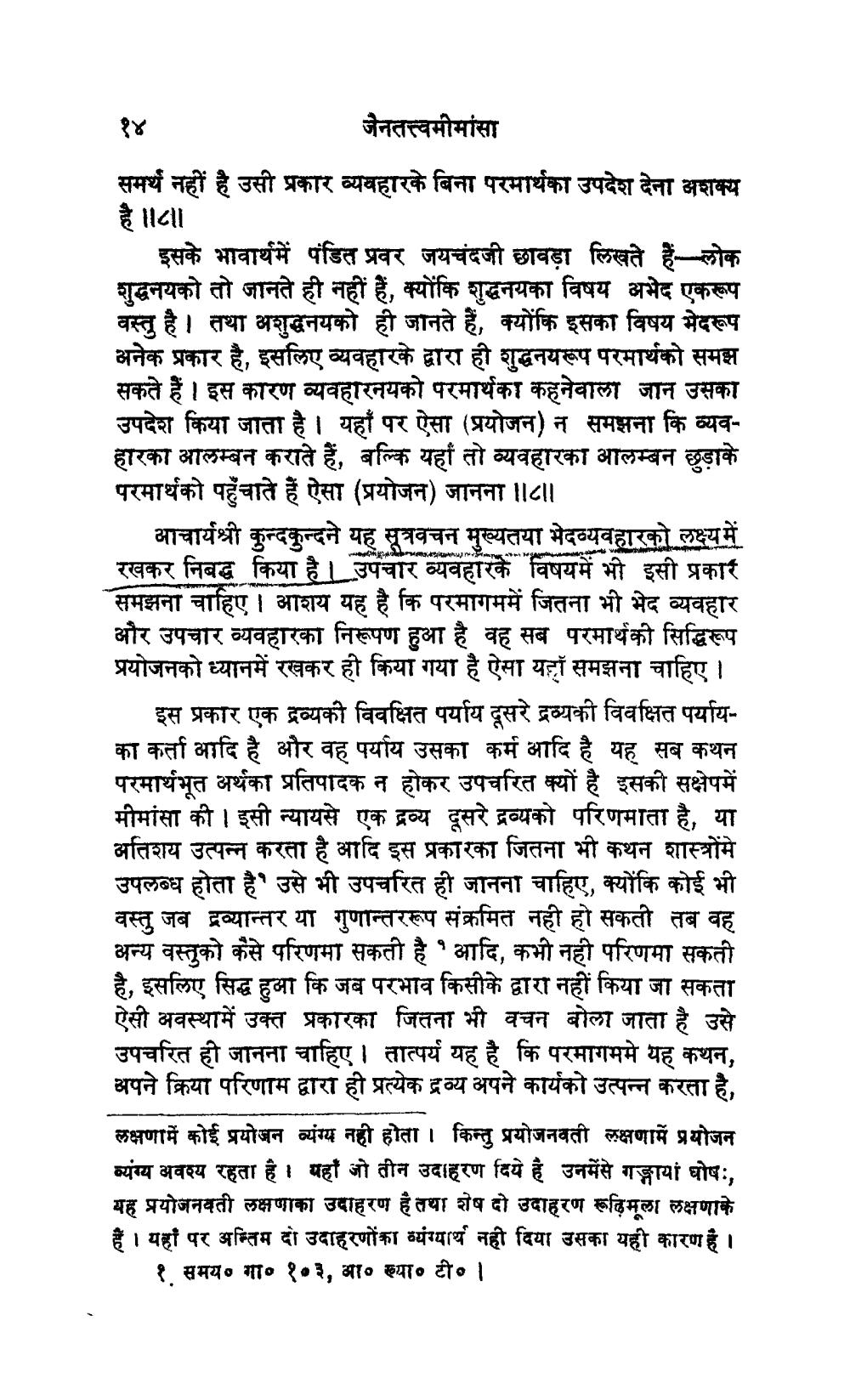________________
wwwdmireoahneemarriagers.
Aamaina
जैनतत्त्वमीमांसा समर्थ नहीं है उसी प्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश देना अशक्य है ॥८॥
इसके भावार्थमें पंडित प्रवर जयचंदजी छावड़ा लिखते हैं-लोक शुद्धनयको तो जानते ही नहीं हैं, क्योंकि शुद्धनयका विषय अभेद एकरूप वस्तु है। तथा अशुद्धनयको ही जानते हैं, क्योंकि इसका विषय भेदरूप अनेक प्रकार है, इसलिए व्यवहारके द्वारा ही शुद्धनयरूप परमार्थको समझ सकते हैं। इस कारण व्यवहारनयको परमार्थका कहनेवाला जान उसका उपदेश किया जाता है। यहाँ पर ऐसा (प्रयोजन) न समझना कि व्यवहारका आलम्बन कराते हैं, बल्कि यहाँ तो व्यवहारका आलम्बन छुड़ाके परमार्थको पहुँचाते हैं ऐसा (प्रयोजन) जानना ।।८।।
आचार्यश्री कुन्दकुन्दने यह सूत्रवचन मुख्यतया भेदव्यवहारको लक्ष्य में रखकर निबद्ध किया है। उपचार व्यवहारके विषय में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। आशय यह है कि परमागममें जितना भी भेद व्यवहार और उपचार व्यवहारका निरूपण हुआ है वह सब परमार्थकी सिद्धिरूप प्रयोजनको ध्यानमें रखकर ही किया गया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।
इस प्रकार एक द्रव्यको विवक्षित पर्याय दूसरे द्रव्यकी विवक्षित पर्यायका कर्ता आदि है और वह पर्याय उसका कर्म आदि है यह सब कथन परमार्थभूत अर्थका प्रतिपादक न होकर उपचरित क्यों है इसकी सक्षेपमें मीमांसा की। इसी न्यायसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको परिणमाता है, या अतिशय उत्पन्न करता है आदि इस प्रकारका जितना भी कथन शास्त्रोंमे उपलब्ध होता है। उसे भी उपचरित ही जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु जब द्रव्यान्तर या गुणान्तररूप संक्रमित नही हो सकती तब वह अन्य वस्तुको कैसे परिणमा सकती है ' आदि, कभी नही परिणमा सकती है, इसलिए सिद्ध हा कि जब परभाव किसीके द्वारा नहीं किया जा सकता ऐसी अवस्थामें उक्त प्रकारका जितना भी वचन बोला जाता है उसे उपचरित ही जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि परमागममे यह कथन, अपने क्रिया परिणाम द्वारा ही प्रत्येक द्रव्य अपने कार्यको उत्पन्न करता है, लक्षणामें कोई प्रयोजन व्यंग्य नहीं होता। किन्तु प्रयोजनवती लक्षणामें प्रयोजन व्यंग्य अवश्य रहता है। यहाँ जो तीन उदाहरण दिये है उनमेंसे गङ्गायां घोषः, यह प्रयोजनवती लक्षणाका उदाहरण है तथा शेष दो उदाहरण रूढिमूला लक्षणाके हैं। यहां पर अन्तिम दो उदाहरणोंका व्यंग्यार्थ नही दिया उसका यही कारण है।
१. समय० गा० १.३, आ० ख्या० टी० ।