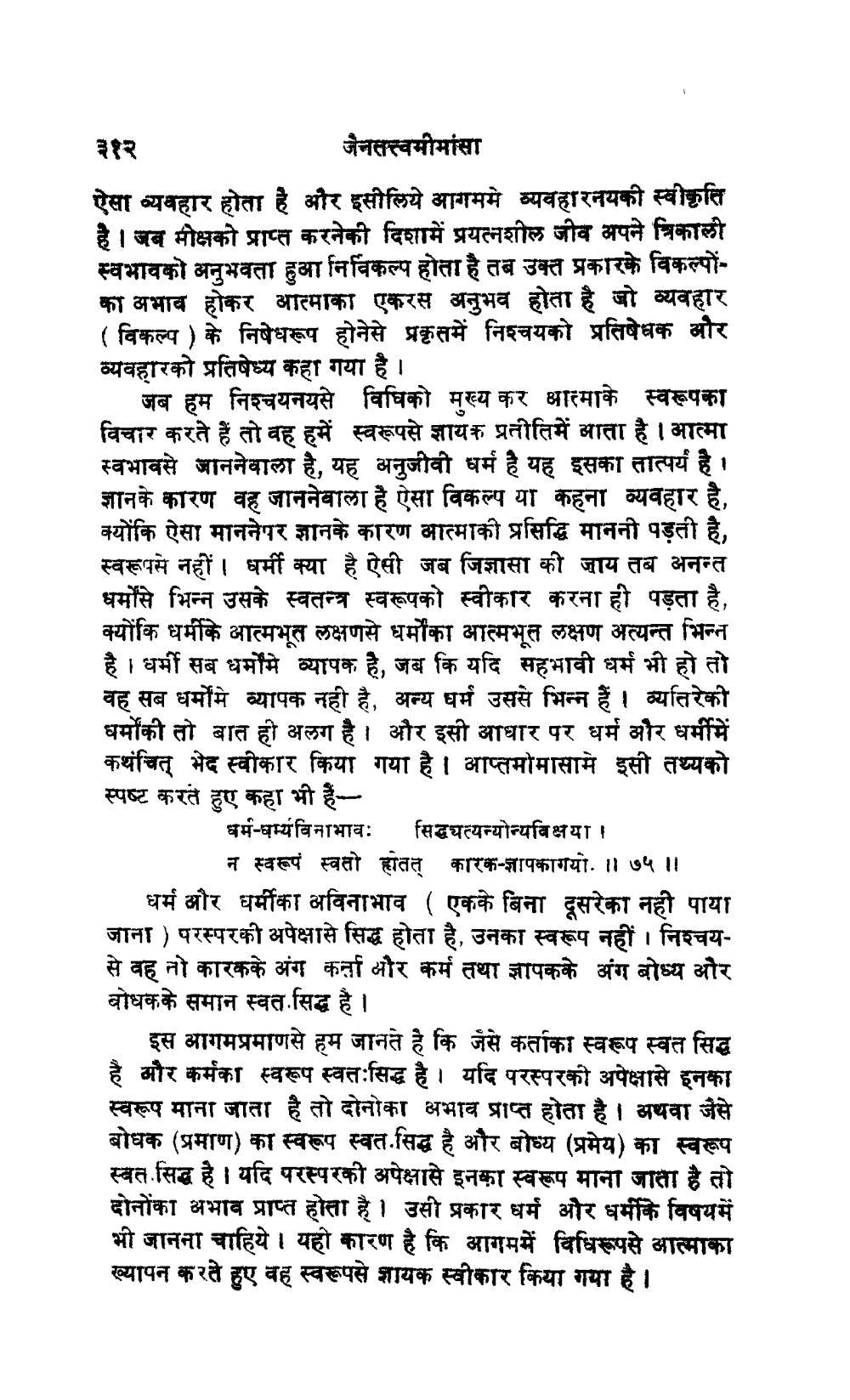________________
३१२
जैनतत्त्वमीमांसा
ऐसा व्यवहार होता है और इसीलिये आगममे व्यवहारनयकी स्वीकृति है । जब मोक्षको प्राप्त करनेकी दिशामें प्रयत्नशील जीव अपने त्रिकाली स्वभावको अनुभवता हुआ निर्विकल्प होता है तब उक्त प्रकारके विकल्पोंका अभाव होकर आत्माका एकरस अनुभव होता है जो व्यवहार ( विकल्प ) के निषेधरूप होनेसे प्रकृतमें निश्चयको प्रतिषेधक और व्यवहारको प्रतिषेध्य कहा गया है।
जब हम निश्चयनयसे विधिको मुख्य कर आत्माके स्वरूपका विचार करते हैं तो वह हमें स्वरूपसे ज्ञायक प्रतीतिमें आता है । आत्मा स्वभावसे जाननेवाला है, यह अनुजीवी धर्म है यह इसका तात्पर्य है । ज्ञान के कारण वह जाननेवाला है ऐसा विकल्प या कहना व्यवहार है, क्योंकि ऐसा माननेपर ज्ञानके कारण आत्माकी प्रसिद्धि माननी पड़ती है, स्वरूपसे नहीं । धर्मी क्या है ऐसी जब जिज्ञासा की जाय तब अनन्त धर्मोसे भिन्न उसके स्वतन्त्र स्वरूपको स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि धर्मी आत्मभूत लक्षणसे धर्मोका आत्मभूत लक्षण अत्यन्त भिन्न है । धर्मी सब धर्मो व्यापक है, जब कि यदि सहभावी धर्म भी हो तो वह सब धर्मो व्यापक नही है, अन्य धर्म उससे भिन्न हैं । व्यतिरेकी धर्मो तो बात ही अलग है । और इसी आधार पर धर्म और धर्मी में कथंचित् भेद स्वीकार किया गया है । आप्तमोमासामे इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा भी हैं
धर्म-विनाभावः
सिद्धयत्यन्योन्यविक्षया ।
न स्वरूपं स्वतो ह्येतत् कारकज्ञापकागयो ।। ७५ ।।
धर्म और धर्मीका अविनाभाव ( एकके बिना दूसरेका नही पाया जाना ) परस्परकी अपेक्षासे सिद्ध होता है, उनका स्वरूप नहीं । निश्चयसे वह तो कारक अंग कर्ता और कर्म तथा ज्ञापकके अंग बोध्य और बोधकके समान स्वत सिद्ध है ।
इस आगमप्रमाणसे हम जानते है कि जैसे कर्ताका स्वरूप स्वत सिद्ध है और कर्मका स्वरूप स्वतः सिद्ध है । यदि परस्परको अपेक्षासे इनका स्वरूप माना जाता है तो दोनोका अभाव प्राप्त होता है । अथवा जैसे बोधक (प्रमाण) का स्वरूप स्वतः सिद्ध है और बोध्य (प्रमेय) का स्वरूप स्वतः सिद्ध है । यदि परस्परकी अपेक्षासे इनका स्वरूप माना जाता है तो दोनोंका अभाव प्राप्त होता है । उसी प्रकार धर्म और धर्मोके विषय में भी जानना चाहिये । यही कारण है कि आगम में विधिरूपसे आत्माका ख्यापन करते हुए वह स्वरूपसे ज्ञायक स्वीकार किया गया है।