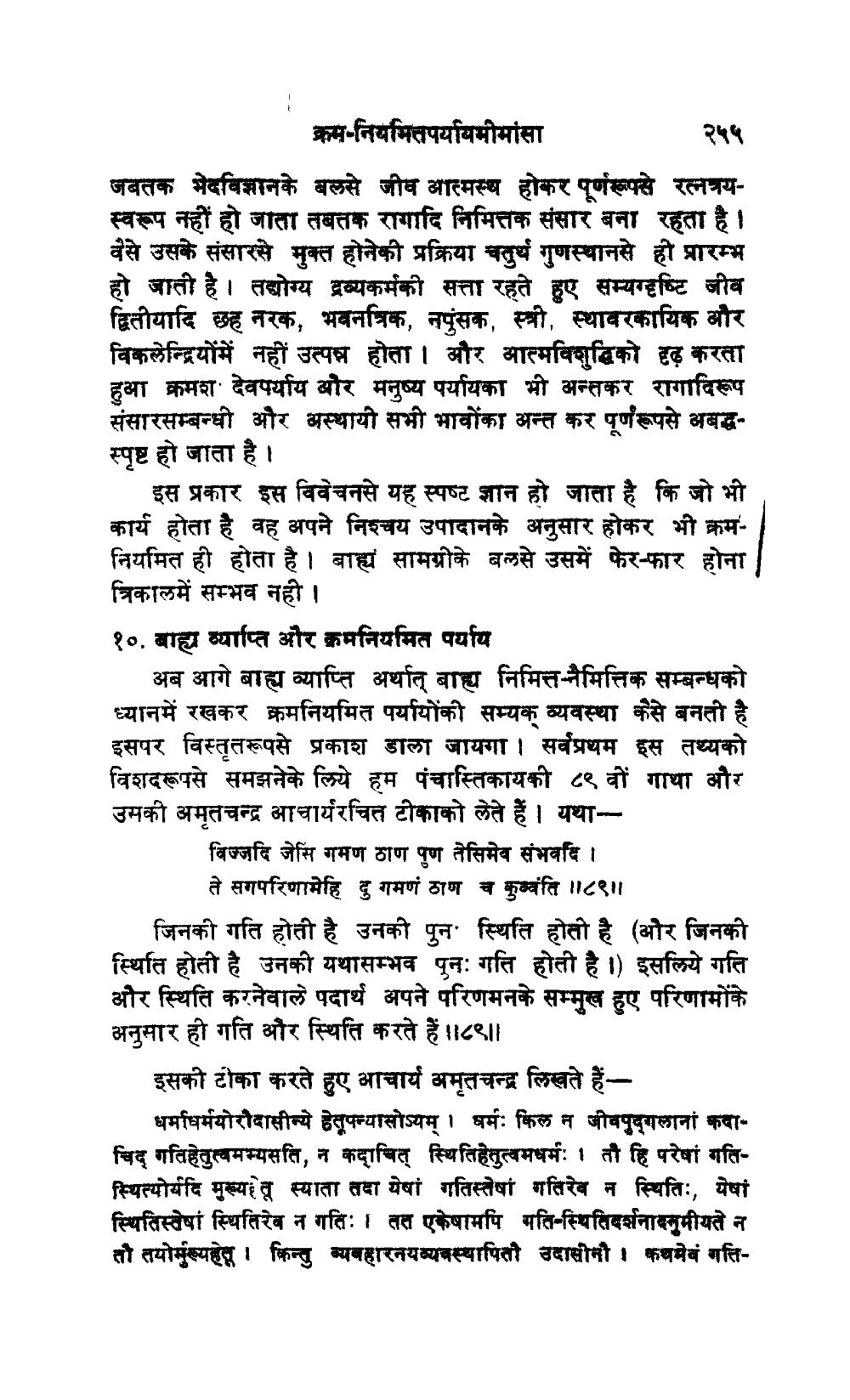________________
क्रम-नियमितपर्यायमीमांसा
२५५ जबतक भेदविज्ञानके बलसे जीव आत्मस्थ होकर पूर्णरूपसे रत्नत्रयस्वरूप नहीं हो जाता तबतक रागादि निमित्तक संसार बना रहता है। वैसे उसके संसारसे मुक्त होनेकी प्रक्रिया चतुर्थ गुणस्थानसे ही प्रारम्भ हो जाती है। तद्योग्य द्रव्यकर्मकी सत्ता रहते हुए सम्यग्दृष्टि जीव द्वितीयादि छह नरक, भवनत्रिक, नपुंसक, स्त्री, स्थावरकायिक और विकलेन्द्रियोंमें नहीं उत्पन्न होता। और आत्मविशुद्धिको दृढ़ करता हुआ क्रमशः देवपर्याय और मनुष्य पर्यायका भी अन्तकर रागादिरूप संसारसम्बन्धी और अस्थायी सभी भावोंका अन्त कर पूर्णरूपसे अबद्धस्पृष्ट हो जाता है। ___ इस प्रकार इस विवेचनसे यह स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि जो भी कार्य होता है वह अपने निश्चय उपादानके अनुसार होकर भी क्रमनियमित ही होता है। बाह्य सामग्रीके बलसे उसमें फेर-फार होना त्रिकालमें सम्भव नही। १०. बाह्य व्याप्ति और क्रमनियमित पर्याय ___ अब आगे बाह्य व्याप्ति अर्थात् बाह्य निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धको ध्यानमें रखकर क्रमनियमित पर्यायोंकी सम्यक व्यवस्था कैसे बनती है इसपर विस्तृतरूपसे प्रकाश डाला जायगा। सर्वप्रथम इस तथ्यको विशदरूपसे समझनेके लिये हम पंचास्तिकायकी ८९ वों गाथा और उमकी अमृतचन्द्र आचार्यरचित टीकाको लेते हैं । यथा
विज्जदि जेसि गमण ठाण पुण तेसिमेव संभवदि ।
ते सगपरिणामेहि दु गमणं ठाण च कुब्वति ॥८९॥ जिनकी गति होती है उनकी पुन स्थिति होती है (और जिनकी स्थिति होती है उनकी यथासम्भव पुनः गति होती है ।) इसलिये गति
और स्थिति करनेवाले पदार्थ अपने परिणमनके सम्मुख हए परिणामोंके अनुसार ही गति और स्थिति करते हैं ।।८।।
इसकी टोका करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं
धर्माधर्मयोरीदासीन्ये हेतपन्यासोऽयम । धर्मः किल न जीवपुदगलानां कदाचिद् गतिहेतुत्वमभ्यसति, न कदाचित् स्थितिहेतुत्वमधर्मः । ती हि परेषां गतिस्थित्योर्यदि मुख्यहेतू स्याता तदा येषां गतिस्तेषां गतिरेव न स्थितिः, येषां स्थितिस्तेषां स्थितिरेव न गतिः । तत एकेषामपि मति-स्थितिदर्शनामुमीयते न तो तयोर्मुल्यहेतू । किन्तु व्यवहारनयव्यवस्थापितो उदासीनी । कयमेवं गति