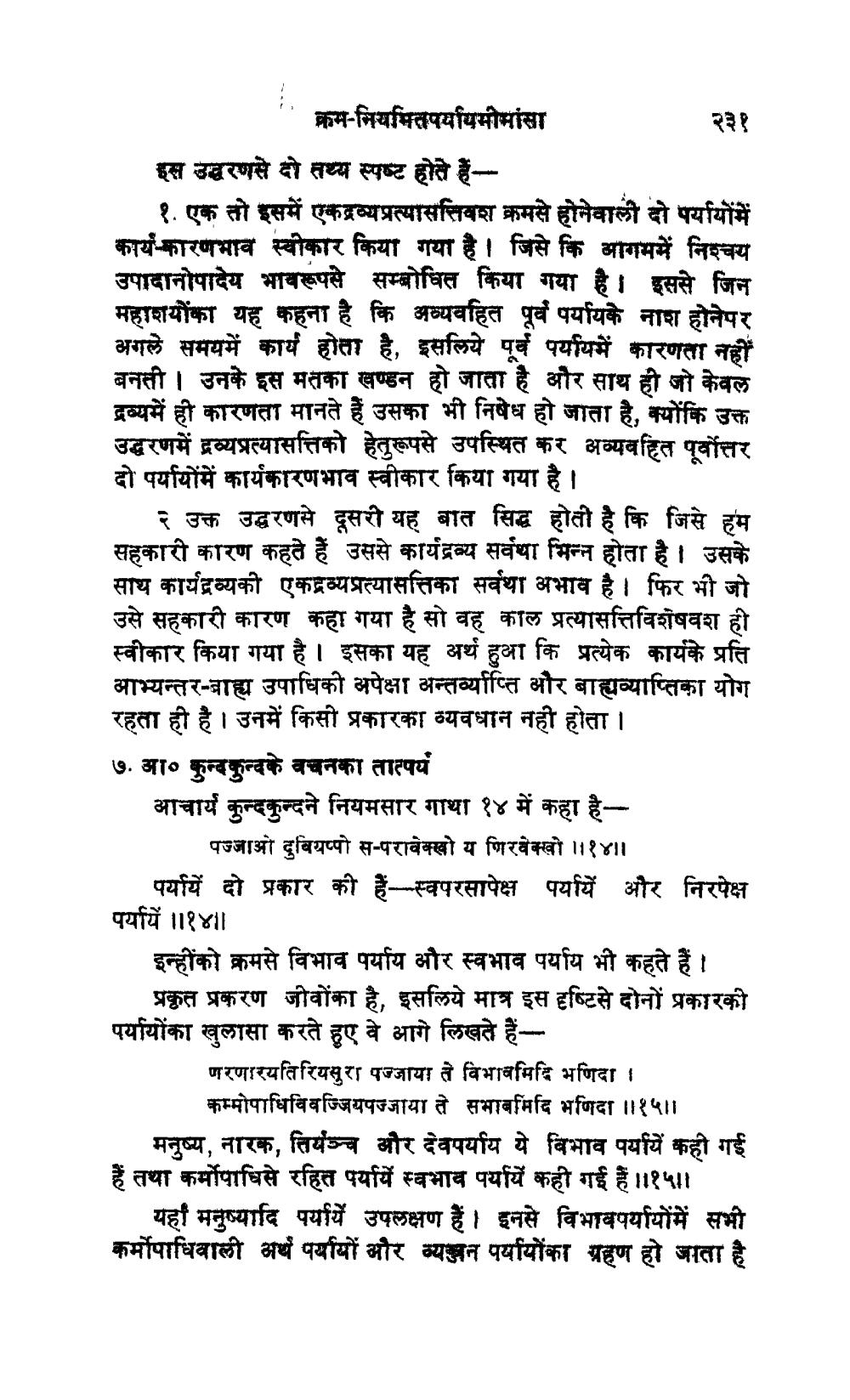________________
क्रम नियमितपर्यायमीमांसा
इस उद्धरणसे दो तथ्य स्पष्ट होते हैं
१. एक तो इसमें एकद्रव्यप्रत्यासत्तिवश क्रमसे होनेवाली दो पर्यायोंमें कार्य-कारणभाव स्वीकार किया गया है। जिसे कि आगममें निश्चय उपादानोपादेय भावरूपसे सम्बोधित किया गया है। इससे जिन महाशयोंका यह कहना है कि अव्यवहित पूर्व पर्यायके नाश होनेपर अगले समय में कार्य होता है, इसलिये पूर्व पर्यायमें कारणता नहीं बनती। उनके इस मतका खण्डन हो जाता है और साथ ही जो केवल द्रव्यमें ही कारणता मानते हैं उसका भी निषेध हो जाता है, क्योंकि उक्त उद्धरणमें द्रव्यप्रत्यासत्तिको हेतुरूपसे उपस्थित कर अव्यवहित पूर्वोत्तर दो पर्यायोंमें कार्यकारणभाव स्वीकार किया गया है।
२३१
२ उक्त उद्धरणसे दूसरी यह बात सिद्ध होती है कि जिसे हम सहकारी कारण कहते हैं उससे कार्यद्रव्य सर्वथा भिन्न होता है । उसके साथ कार्यद्रव्यकी एकद्रव्यप्रत्यासत्तिका सर्वथा अभाव है। फिर भी जो उसे सहकारी कारण कहा गया है सो वह काल प्रत्यासत्तिविशेषवश ही स्वीकार किया गया है । इसका यह अर्थ हुआ कि प्रत्येक कार्यके प्रति आभ्यन्तर बाह्य उपाधिको अपेक्षा अन्तर्व्याप्ति और बाह्यव्याप्तिका योग रहता ही है । उनमें किसी प्रकारका व्यवधान नही होता ।
७. आ० कुन्दकुन्दके वचनका तात्पर्य
आचार्य कुन्दकुन्दने नियमसार गाथा १४ में कहा हैपज्जाओ दुबियप्पो स-परावेक्खो य णिरवेक्खो || १४ ||
पर्यायें दो प्रकार की हैं -स्वपरसापेक्ष पर्यायें और निरपेक्ष पर्यायें ||१४||
इन्हींको क्रमसे विभाव पर्याय और स्वभाव पर्याय भी कहते हैं । प्रकृत प्रकरण जीवोंका है, इसलिये मात्र इस दृष्टिसे दोनों प्रकारकी पर्यायोंका खुलासा करते हुए वे आगे लिखते हैं
णरणारयतिरियसुरा पज्जाया ते विभावमिदि भणिदा । कम्मोपाधिविवज्जियपज्जाया ते सभावमिदि भणिदा || १५ ||
मनुष्य, नारक, तिर्यञ्च और देवपर्याय ये विभाव पर्यायें कही गई हैं तथा कर्मोपाधिसे रहित पर्यायें स्वभाव पर्यायें कही गई हैं ||१५||
यहाँ मनुष्यादि पर्यायें उपलक्षण हैं । इनसे विभावपर्यायोंमें सभी कर्मोपाधिवाली अर्थ पर्यायों और व्यञ्जन पर्यायोंका ग्रहण हो जाता है