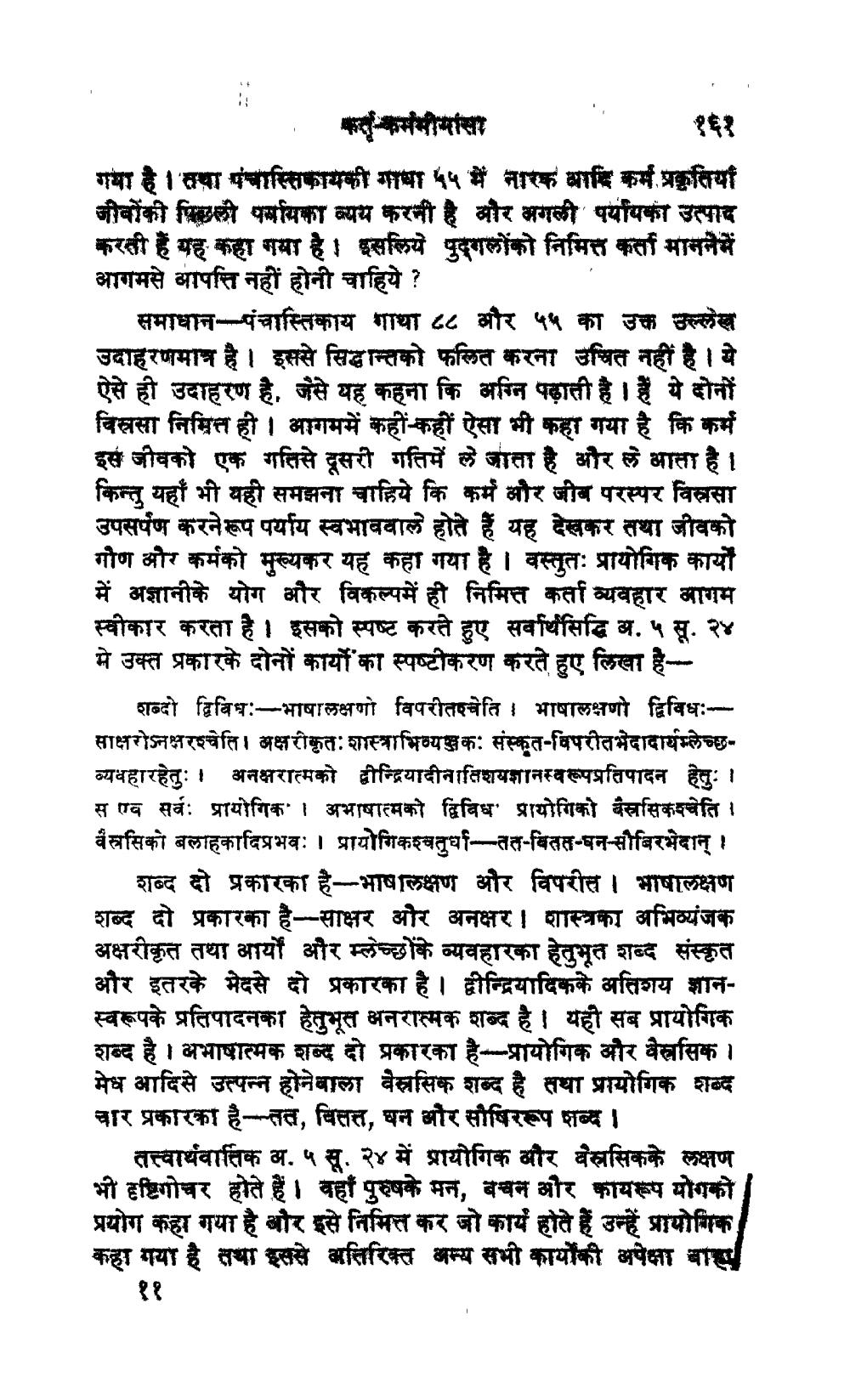________________
कर्तृकर्ममीमांसा
१६१
गया है । तथा पंचास्तिकायकी गाथा ५५ में नारक आदि कर्म प्रकृतियाँ जtaint पिछली पर्यायका व्यय करनी है और अगली पर्यायका उत्पाद करती हैं यह कहा गया है । इसलिये पुद्गलोंको निमित्त कर्ता माननेमें आगमसे आपत्ति नहीं होनी चाहिये ?
समाधान-पंचास्तिकाय गाथा ८८ और ५५ का उत उल्लेख उदाहरणमात्र है । इससे सिद्धान्तको फलित करना उचित नहीं है । ये ऐसे ही उदाहरण है, जैसे यह कहना कि अग्नि पढ़ाती है । हैं ये दोनों famer निमित्त हो । आगममें कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि कर्म इस जीवको एक गतिसे दूसरी गतिमें ले जाता है और ले आता है । किन्तु यहाँ भी यही समझना चाहिये कि कर्म और जीब परस्पर विस्त्रसा उपसर्पण करने रूप पर्याय स्वभाववाले होते हैं यह देखकर तथा जीवको गौण और कर्मको मुख्यकर यह कहा गया है । वस्तुतः प्रायोगिक कार्यो में अज्ञानीके योग और विकल्पमें ही निमित्त कर्ता व्यवहार बागम स्वीकार करता है । इसको स्पष्ट करते हुए सर्वार्थसिद्धि अ. ५ सू. २४ मे उक्त प्रकारके दोनों कार्यों का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है
-
शब्दो द्विविधः -- भाषालक्षणो विपरीतश्चेति । भाषालक्षणो द्विविध:साक्षरोऽनक्षरश्चेति । अक्षरीकृतः शास्त्राभिव्यञ्जकः संस्कृत - विपरीत भेदादार्यम्लेच्छव्यवहारहेतुः । अनक्षरात्मको द्वीन्द्रियादीनातिशयज्ञानस्वरूपप्रतिपादन हेतुः । स एव सर्व प्रायोगिक । अभाषात्मको द्विविध' प्रायोगिको बैासिकश्चेति । afest बलाहकादिप्रभवः । प्रायोगिकश्चतुर्धा - तत- वितत - घन - सौबिरभेदान् ।
शब्द दो प्रकारका है-भाषालक्षण और विपरीत । भाषालक्षण शब्द दो प्रकारका है— साक्षर और अनक्षर । शास्त्रका अभिव्यंजक अक्षरीकृत तथा आर्यों और म्लेच्छोंके व्यवहारका हेतुभूत शब्द संस्कृत और इतरके भेदसे दो प्रकारका है । द्वीन्द्रियादिकके अतिशय ज्ञानस्वरूपके प्रतिपादनका हेतुभूत अनरात्मक शब्द है । यही सब प्रायोगिक शब्द है । अभाषात्मक शब्द दो प्रकारका है - प्रायोगिक और वैनसिक । मेघ आदिसे उत्पन्न होनेवाला वैस्रलिक शब्द है तथा प्रायोगिक शब्द चार प्रकारका है-तत, वित्तत्त, घन और सीषिररूप शब्द |
तत्त्वार्थवार्तिक अ. ५ सू. २४ में प्रायोगिक और वैत्रसिकके लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं । वहाँ पुरुषके मन, बचन और कायरूप योगको प्रयोग कहा गया है और इसे निमित्त कर जो कार्य होते हैं उन्हें प्रायोगिक कहा गया है तथा इससे अतिरिक्त अन्य सभी कार्योंकी अपेक्षा
११