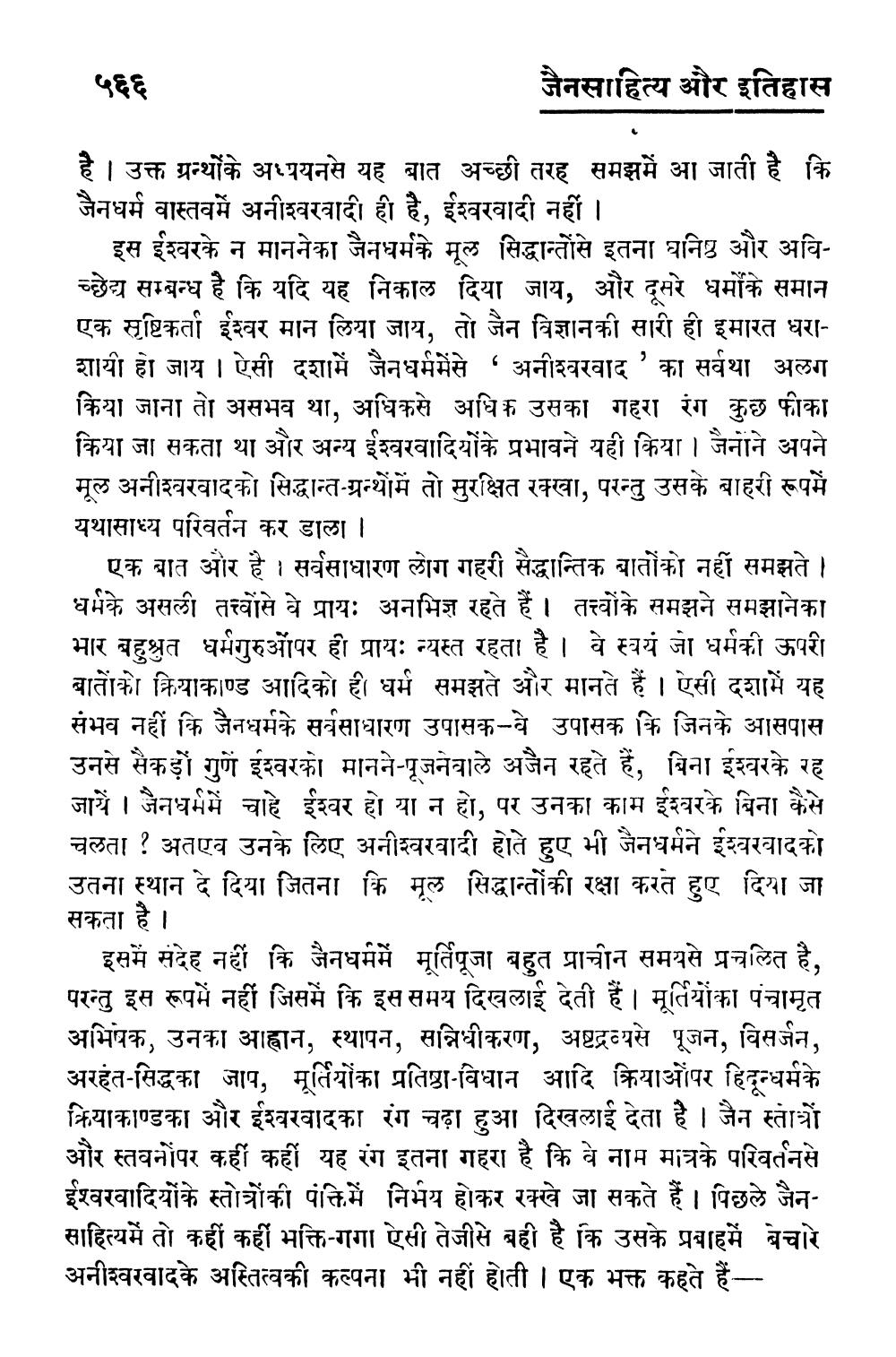________________
जैन साहित्य और इतिहास
५६६
है । उक्त ग्रन्थोंके अध्ययन से यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि जैनधर्म वास्तव में अनीश्वरवादी ही है, ईश्वरवादी नहीं ।
•
इस ईश्वरके न माननेका जैनधर्मके मूल सिद्धान्तोंसे इतना घनिष्ठ और अविच्छेद्य सम्बन्ध है कि यदि यह निकाल दिया जाय, और दूसरे धर्मोंके समान एक सृष्टिकर्ता ईश्वर मान लिया जाय, तो जैन विज्ञानकी सारी ही इमारत धराशायी हो जाय । ऐसी दशा में जैनधर्ममेंसे ' अनीश्वरवाद ' का सर्वथा अलग किया जाना तो असंभव था, अधिक से अधिक उसका गहरा रंग कुछ फीका किया जा सकता था और अन्य ईश्वरवादियोंके प्रभावने यही किया । जैनाने अपने मूल अनीश्वरवादको सिद्धान्त-ग्रन्थों में तो सुरक्षित रक्खा, परन्तु उसके बाहरी रूपमें यथासाध्य परिवर्तन कर डाला ।
एक बात और है । सर्वसाधारण लोग गहरी सैद्धान्तिक बातोंको नहीं समझते । धर्मके असली तत्त्वोंसे वे प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं । तत्त्वों के समझने समझानेका भार बहुश्रुत धर्मगुरुओं पर ही प्रायः न्यस्त रहता है । वे स्वयं जो धर्मकी ऊपरी बातोंको क्रियाकाण्ड आदिको ही धर्म समझते और मानते हैं । ऐसी दशा में यह संभव नहीं कि जैनधर्म के सर्वसाधारण उपासक - वे उपासक कि जिनके आसपास उनसे सैकड़ों गुणे ईश्वरको मानने- पूजनेवाले अजैन रहते हैं, बिना ईश्वरके रह जायें | जैनधर्म में चाहे ईश्वर हो या न हो, पर उनका काम ईश्वरके बिना कैसे चलता ? अतएव उनके लिए अनीश्वरवादी होते हुए भी जैनधर्मने ईश्वरवादको उतना स्थान दे दिया जितना कि मूल सिद्धान्तोंकी रक्षा करते हुए दिया जा सकता है।
इसमें संदेह नहीं कि जैनधर्म में मूर्तिपूजा बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है, परन्तु इस रूपमें नहीं जिसमें कि इस समय दिखलाई देती हैं । मूर्तियों का पंचामृत अभिषेक, उनका आह्वान, स्थापन, सन्निधीकरण, अष्टद्रव्यसे पूजन, विसर्जन, अरहंत-सिद्धका जाप, मूर्तियों का प्रतिष्ठा - विधान आदि क्रियाओंपर हिदून्धर्मके क्रियाकाण्डका और ईश्वरवादका रंग चढ़ा हुआ दिखलाई देता है । जैन स्तात्रों और स्तनोंपर कहीं कहीं यह रंग इतना गहरा है कि वे नाम मात्रके परिवर्तन से ईश्वरवादियों के स्तोत्रों की पंक्ति में निर्भय होकर रक्खे जा सकते हैं । पिछले जैनसाहित्य में तो कहीं कहीं भक्ति-गंगा ऐसी तेजी से बहीं है कि उसके प्रवाह में बेचारे अनीश्वरवादके अस्तित्वकी कल्पना भी नहीं होती । एक भक्त कहते हैं
---