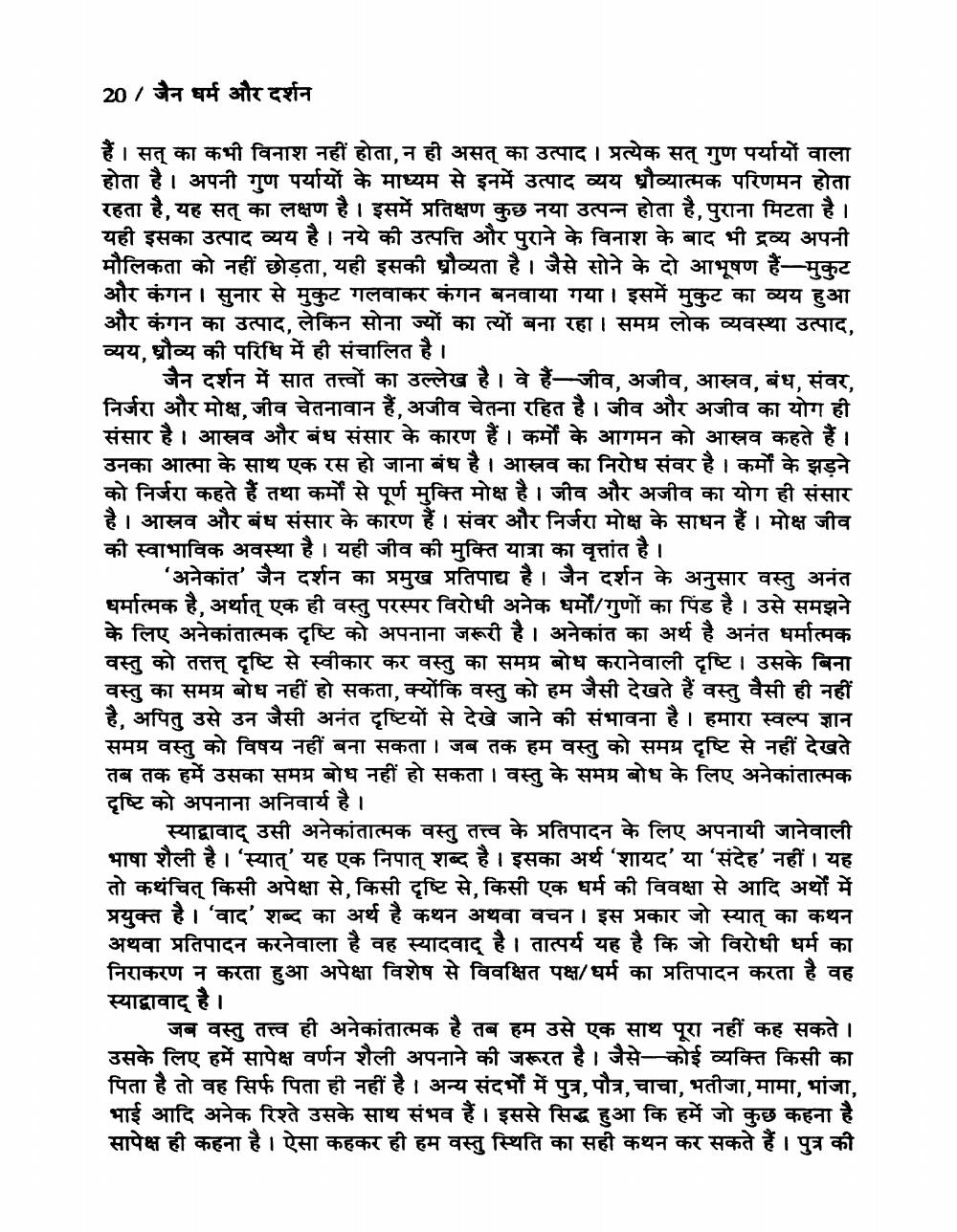________________
20 / जैन धर्म और दर्शन
हैं। सत् का कभी विनाश नहीं होता, न ही असत् का उत्पाद । प्रत्येक सत् गुण पर्यायों वाला होता है। अपनी गुण पर्यायों के माध्यम से इनमें उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक परिणमन होता रहता है, यह सत् का लक्षण है। इसमें प्रतिक्षण कुछ नया उत्पन्न होता है, पुराना मिटता है। यही इसका उत्पाद व्यय है। नये की उत्पत्ति और पुराने के विनाश के बाद भी द्रव्य आ मौलिकता को नहीं छोड़ता, यही इसकी ध्रौव्यता है। जैसे सोने के दो आभूषण हैं-मुकुट और कंगन । सुनार से मुकुट गलवाकर कंगन बनवाया गया। इसमें मुकुट का व्यय हुआ और कंगन का उत्पाद, लेकिन सोना ज्यों का त्यों बना रहा। समग्र लोक व्यवस्था उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य की परिधि में ही संचालित है।
जैन दर्शन में सात तत्त्वों का उल्लेख है। वे हैं-जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष,जीव चेतनावान हैं, अजीव चेतना रहित है। जीव और अजीव का योग ही संसार है। आस्रव और बंध संसार के कारण हैं। कर्मों के आगमन को आस्रव कहते हैं। उनका आत्मा के साथ एक रस हो जाना बंध है। आस्रव का निरोध संवर है। कर्मों के झड़ने को निर्जरा कहते हैं तथा कर्मों से पूर्ण मुक्ति मोक्ष है। जीव और अजीव का योग ही संसार है। आस्रव और बंध संसार के कारण हैं। संवर और निर्जरा मोक्ष के साधन हैं। मोक्ष जीव की स्वाभाविक अवस्था है । यही जीव की मुक्ति यात्रा का वृत्तांत है।
___ 'अनेकांत' जैन दर्शन का प्रमुख प्रतिपाद्य है। जैन दर्शन के अनुसार वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अर्थात् एक ही वस्तु परस्पर विरोधी अनेक धर्मों/गुणों का पिंड है। उसे समझने के लिए अनेकांतात्मक दृष्टि को अपनाना जरूरी है। अनेकांत का अर्थ है अनंत धर्मात्मक वस्तु को तत्तत्त् दृष्टि से स्वीकार कर वस्तु का समय बोध करानेवाली दृष्टि । उसके बिना वस्तु का समग्र बोध नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु को हम जैसी देखते हैं वस्तु वैसी ही नहीं है, अपितु उसे उन जैसी अनंत दृष्टियों से देखे जाने की संभावना है। हमारा स्वल्प ज्ञान समग्र वस्तु को विषय नहीं बना सकता। जब तक हम वस्तु को समग्र दृष्टि से नहीं देखते तब तक हमें उसका समग्र बोध नहीं हो सकता । वस्तु के समग्र बोध के लिए अनेकांतात्मक दृष्टि को अपनाना अनिवार्य है।
स्याद्वावाद् उसी अनेकांतात्मक वस्तु तत्त्व के प्रतिपादन के लिए अपनायी जानेवाली भाषा शैली है । 'स्यात्' यह एक निपात् शब्द है। इसका अर्थ 'शायद' या 'संदेह नहीं। यह तो कथंचित् किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि से, किसी एक धर्म की विवक्षा से आदि अर्थों में प्रयुक्त है। 'वाद' शब्द का अर्थ है कथन अथवा वचन । इस प्रकार जो स्यात् का कथन अथवा प्रतिपादन करनेवाला है वह स्यादवाद् है। तात्पर्य यह है कि जो विरोधी धर्म का निराकरण न करता हुआ अपेक्षा विशेष से विवक्षित पक्ष/धर्म का प्रतिपादन करता है वह स्याद्वावाद् है।
जब वस्तु तत्त्व ही अनेकांतात्मक है तब हम उसे एक साथ पूरा नहीं कह सकते। उसके लिए हमें सापेक्ष वर्णन शैली अपनाने की जरूरत है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का पिता है तो वह सिर्फ पिता ही नहीं है। अन्य संदों में पुत्र,पौत्र, चाचा, भतीजा,मामा, भांजा, भाई आदि अनेक रिश्ते उसके साथ संभव हैं। इससे सिद्ध हुआ कि हमें जो कुछ कहना है सापेक्ष ही कहना है । ऐसा कहकर ही हम वस्तु स्थिति का सही कथन कर सकते हैं । पुत्र की