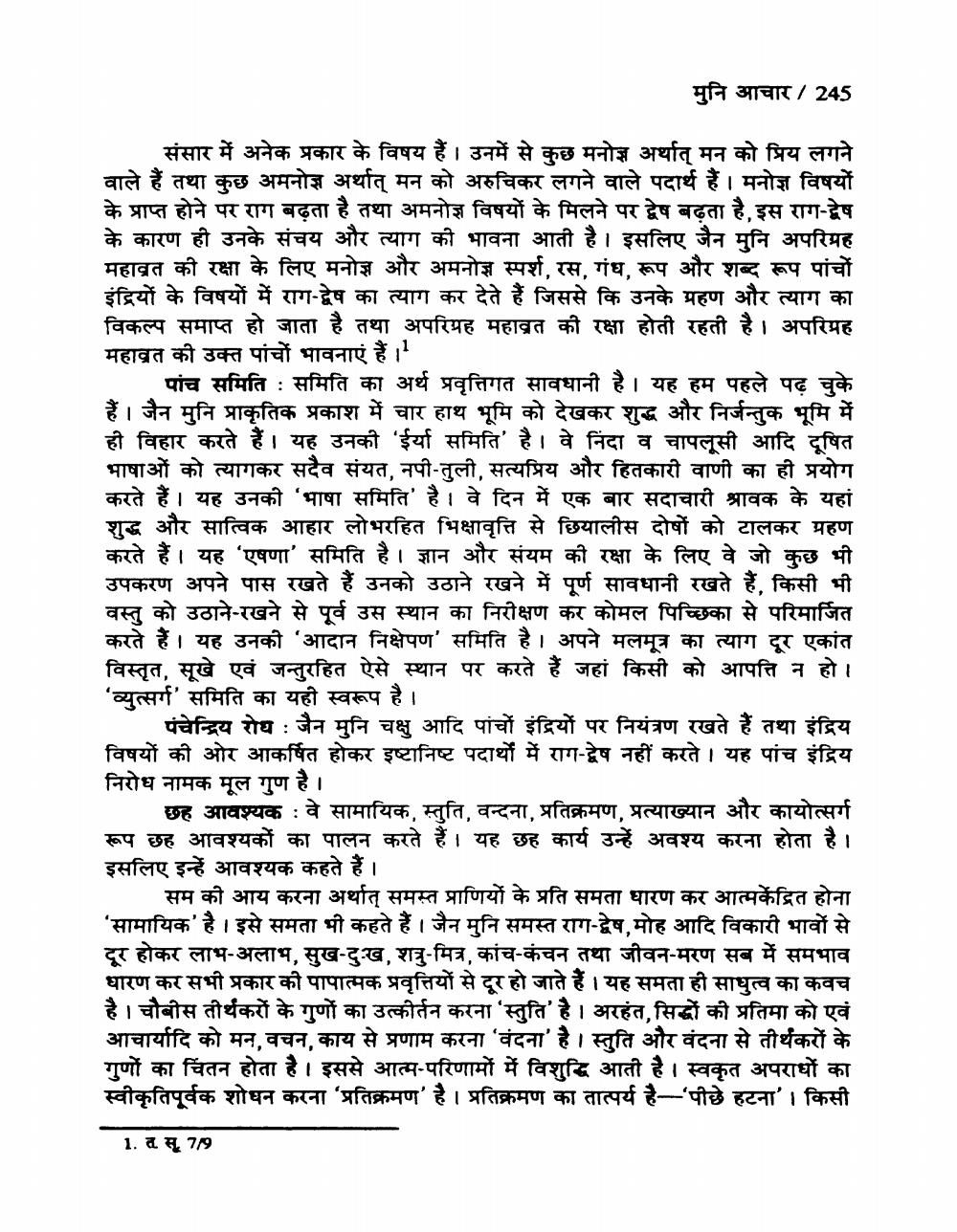________________
मुनि आचार / 245
संसार में अनेक प्रकार के विषय हैं। उनमें से कुछ मनोज्ञ अर्थात् मन को प्रिय लगने वाले हैं तथा कुछ अमनोज्ञ अर्थात् मन को अरुचिकर लगने वाले पदार्थ हैं। मनोज्ञ विषयों के प्राप्त होने पर राग बढ़ता है तथा अमनोज्ञ विषयों के मिलने पर द्वेष बढ़ता है, इस राग-द्वेष के कारण ही उनके संचय और त्याग की भावना आती है। इसलिए जैन मुनि अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा के लिए मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श, रस, गंध,रूप और शब्द रूप पांचों इंद्रियों के विषयों में राग-द्वेष का त्याग कर देते हैं जिससे कि उनके ग्रहण और त्याग का विकल्प समाप्त हो जाता है तथा अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा होती रहती है। अपरिग्रह महाव्रत की उक्त पांचों भावनाएं हैं।
पांच समिति : समिति का अर्थ प्रवृत्तिगत सावधानी है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं। जैन मनि प्राकृतिक प्रकाश में चार हाथ भूमि को देखकर शुद्ध और निर्जन्तुक भूमि में ही विहार करते हैं। यह उनकी 'ईर्या समिति' है। वे निंदा व चापलूसी आदि दूषित भाषाओं को त्यागकर सदैव संयत, नपी-तुली, सत्यप्रिय और हितकारी वाणी का ही प्रयोग करते हैं। यह उनकी 'भाषा समिति' है। वे दिन में एक बार सदाचारी श्रावक के यहां शुद्ध और सात्विक आहार लोभरहित भिक्षावृत्ति से छियालीस दोषों को टालकर ग्रहण करते हैं। यह 'एषणा' समिति है। ज्ञान और संयम की रक्षा के लिए वे जो कुछ भी उपकरण अपने पास रखते हैं उनको उठाने रखने में पूर्ण सावधानी रखते हैं, किसी भी वस्तु को उठाने-रखने से पूर्व उस स्थान का निरीक्षण कर कोमल पिच्छिका से परिमार्जित करते हैं। यह उनकी 'आदान निक्षेपण' समिति है। अपने मलमूत्र का त्याग दूर एकांत विस्तृत, सूखे एवं जन्तुरहित ऐसे स्थान पर करते हैं जहां किसी को आपत्ति न हो। 'व्युत्सर्ग' समिति का यही स्वरूप है।
पंचेन्द्रिय रोध : जैन मुनि चक्षु आदि पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तथा इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होकर इष्टानिष्ट पदार्थों में राग-द्वेष नहीं करते। यह पांच इंद्रिय निरोध नामक मूल गुण है।
छह आवश्यक : वे सामायिक, स्तुति, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग रूप छह आवश्यकों का पालन करते हैं। यह छह कार्य उन्हें अवश्य करना होता है। इसलिए इन्हें आवश्यक कहते हैं।
सम की आय करना अर्थात् समस्त प्राणियों के प्रति समता धारण कर आत्मकेंद्रित होना 'सामायिक' है। इसे समता भी कहते हैं। जैन मनि समस्त राग-द्वेष.मोह आदि विकारी भावों से दूर होकर लाभ-अलाभ, सुख-दुःख,शत्रु-मित्र, कांच-कंचन तथा जीवन-मरण सब में समभाव धारण कर सभी प्रकार की पापात्मक प्रवृत्तियों से दूर हो जाते हैं । यह समता ही साधुत्व का कवच है। चौबीस तीर्थंकरों के गुणों का उत्कीर्तन करना 'स्तुति' है। अरहंत, सिद्धों की प्रतिमा को एवं आचार्यादि को मन, वचन, काय से प्रणाम करना 'वंदना' है। स्तुति और वंदना से तीर्थकरों के गुणों का चिंतन होता है। इससे आत्म-परिणामों में विशुद्धि आती है। स्वकृत अपराधों का स्वीकृतिपूर्वक शोधन करना 'प्रतिक्रमण' है । प्रतिक्रमण का तात्पर्य है-'पीछे हटना' । किसी
1.त. सू.79