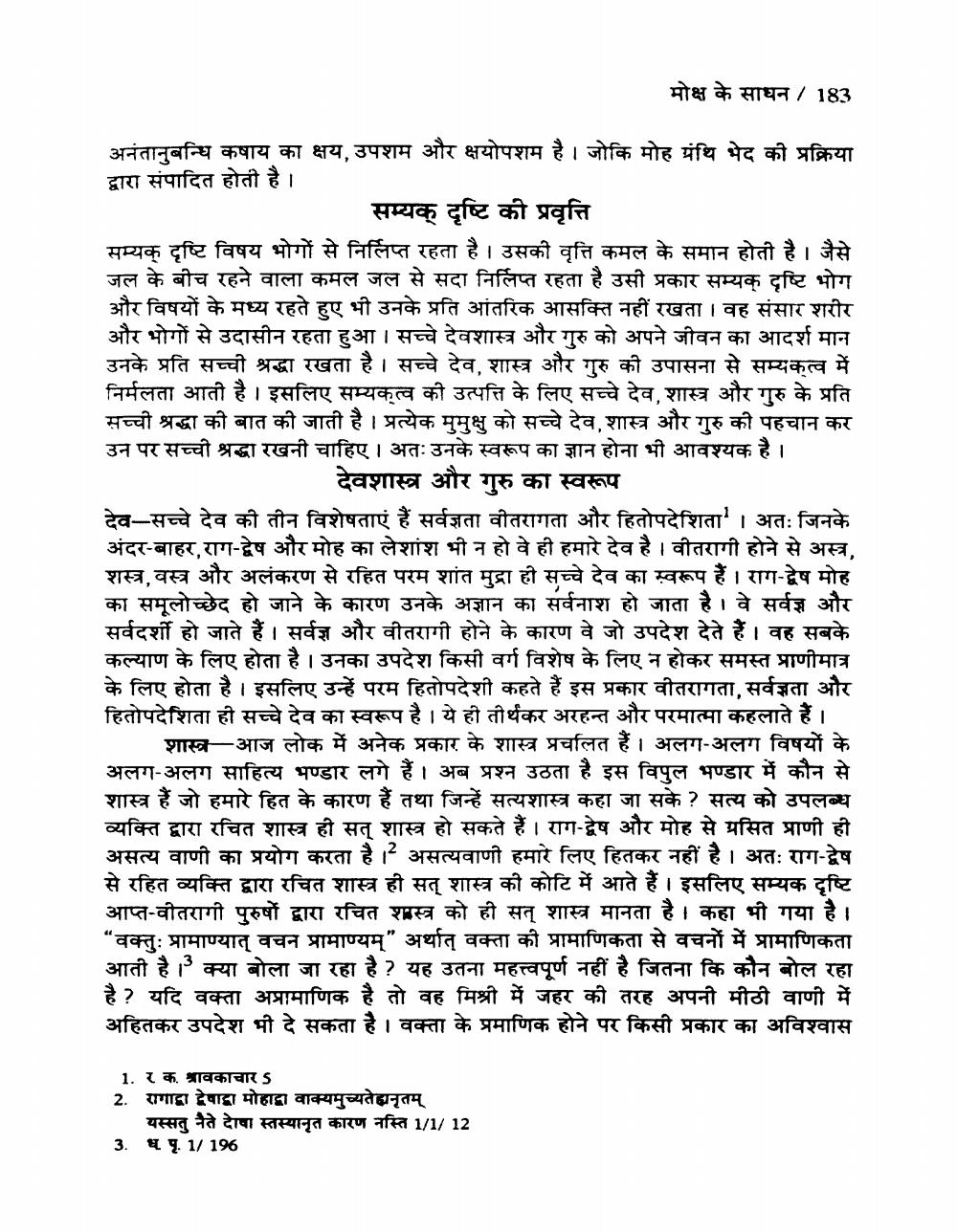________________
मोक्ष के साधन / 183
अनंतानुबन्धि कषाय का क्षय, उपशम और क्षयोपशम है । जोकि मोह ग्रंथि भेद की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है।
सम्यक् दृष्टि की प्रवृत्ति सम्यक दृष्टि विषय भोगों से निर्लिप्त रहता है। उसकी वृत्ति कमल के समान होती है। जैसे जल के बीच रहने वाला कमल जल से सदा निर्लिप्त रहता है उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भोग और विषयों के मध्य रहते हए भी उनके प्रति आंतरिक आसक्ति नहीं रखता। वह संसार शरीर और भोगों से उदासीन रहता हुआ । सच्चे देवशास्त्र और गुरु को अपने जीवन का आदर्श मान उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है। सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की उपासना से सम्यक्त्व में निर्मलता आती है । इसलिए सम्यक्त्व की उत्पत्ति के लिए सच्चे देव,शास्त्र और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा की बात की जाती है। प्रत्येक मुमुक्षु को सच्चे देव,शास्त्र और गुरु की पहचान कर उन पर सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। अतः उनके स्वरूप का ज्ञान होना भी आवश्यक है।
देवशास्त्र और गुरु का स्वरूप देव-सच्चे देव की तीन विशेषताएं हैं सर्वज्ञता वीतरागता और हितोपदेशिता' । अत: जिनके अंदर-बाहर,राग-द्वेष और मोह का लेशांश भी न हो वे ही हमारे देव है । वीतरागी होने से अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र और अलंकरण से रहित परम शांत मुद्रा ही सच्चे देव का स्वरूप हैं । राग-द्वेष मोह का समूलोच्छेद हो जाने के कारण उनके अज्ञान का सर्वनाश हो जाता है। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाते हैं। सर्वज्ञ और वीतरागी होने के कारण वे जो उपदेश देते हैं। वह सबके कल्याण के लिए होता है । उनका उपदेश किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर समस्त प्राणीमात्र के लिए होता है। इसलिए उन्हें परम हितोपदेशी कहते हैं इस प्रकार वीतरागता,सर्वज्ञता और हितोपदेशिता ही सच्चे देव का स्वरूप है। ये ही तीर्थकर अरहन्त और परमात्मा कहलाते हैं।
शास्त्र-आज लोक में अनेक प्रकार के शास्त्र प्रचलित हैं। अलग-अलग विषयों के अलग-अलग साहित्य भण्डार लगे हैं। अब प्रश्न उठता है इस विपुल भण्डार में कौन से शास्त्र हैं जो हमारे हित के कारण हैं तथा जिन्हें सत्यशास्त्र कहा जा सके ? सत्य को उपलब्ध व्यक्ति द्वारा रचित शास्त्र ही सत् शास्त्र हो सकते हैं। राग-द्वेष और मोह से ग्रसित प्राणी ही असत्य वाणी का प्रयोग करता है। असत्यवाणी हमारे लिए हितकर नहीं है। अतः राग-द्वेष से रहित व्यक्ति द्वारा रचित शास्त्र ही सत शास्त्र की कोटि में आते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि आप्त-वीतरागी पुरुषों द्वारा रचित शास्त्र को ही सत् शास्त्र मानता है। कहा भी गया है। “वक्तुः प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम" अर्थात् वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। क्या बोला जा रहा है? यह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि कौन बोल रहा है? यदि वक्ता अप्रामाणिक है तो वह मिश्री में जहर की तरह अपनी मीठी वाणी में अहितकर उपदेश भी दे सकता है । वक्ता के प्रमाणिक होने पर किसी प्रकार का अविश्वास
1. र क. श्रावकाचार 2. रागादा देखादा मोहादा वाक्यमुच्यतेह्यनृतम्
यस्सतु नैते दोषा स्तस्यानृत कारण नस्ति 1/1/ 12 3. ध पृ. 1/196