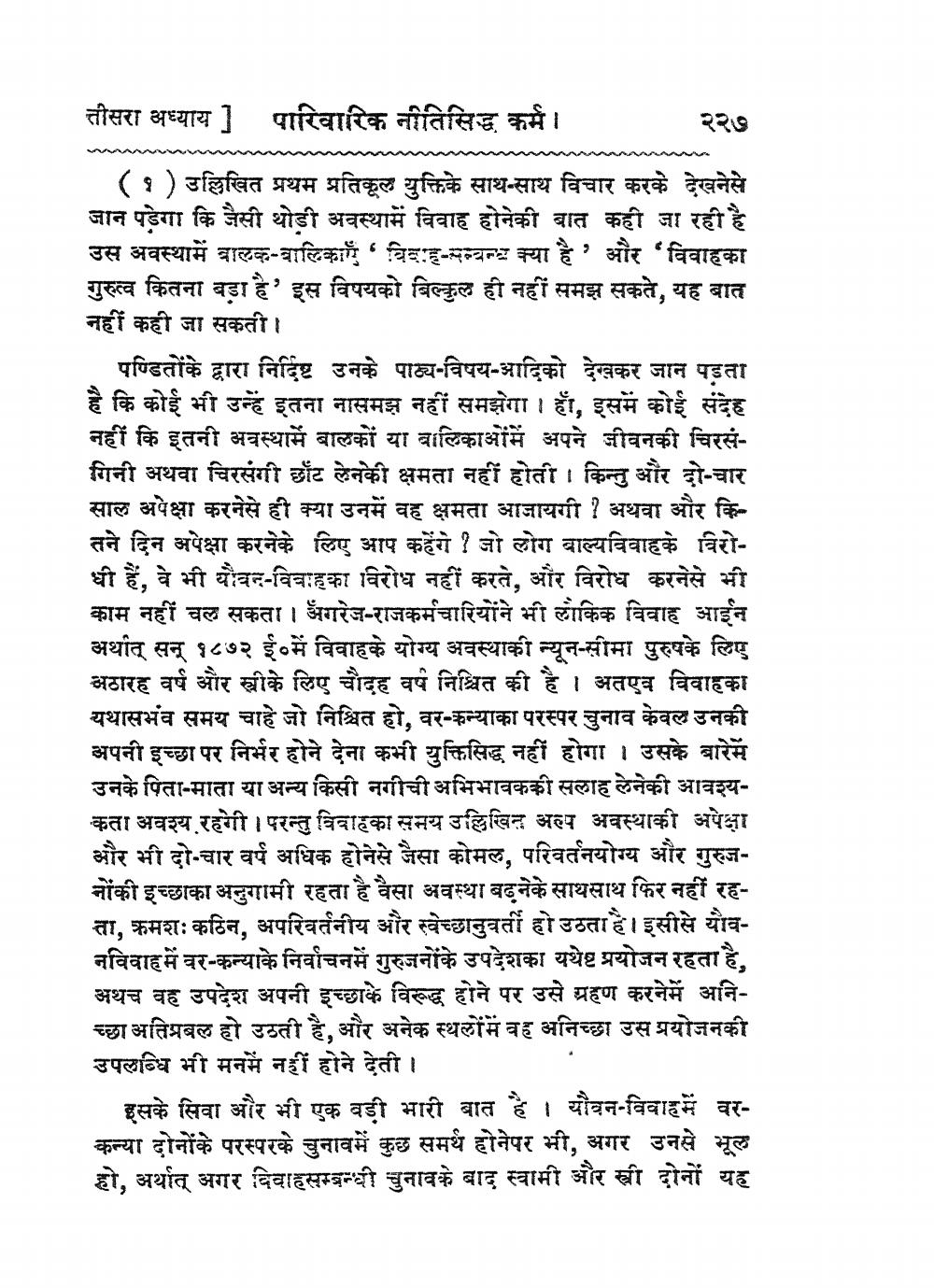________________
तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कर्म।
२२७
(१) उल्लिखित प्रथम प्रतिकूल युक्तिके साथ-साथ विचार करके देखनेसे जान पड़ेगा कि जैसी थोडी अवस्थामें विवाह होनेकी बात कही जा रही है उस अवस्थामें बालक-बालिकाएँ 'विवाह-सन्बन्ध क्या है' और 'विवाहका गुरुत्व कितना बड़ा है' इस विषयको बिल्कुल ही नहीं समझ सकते, यह बात नहीं कही जा सकती।
पण्डितोंके द्वारा निर्दिष्ट उनके पाठ्य-विषय-आदिको देखकर जान पड़ता है कि कोई भी उन्हें इतना नासमझ नहीं समझेगा । हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि इतनी अवस्थामें बालकों या बालिकाओंमें अपने जीवनकी चिरसंगिनी अथवा चिरसंगी छाँट लेनकी क्षमता नहीं होती। किन्तु और दो-चार साल अपेक्षा करनेसे ही क्या उनमें वह क्षमता आजायगी? अथवा और कितने दिन अपेक्षा करनेके लिए आप कहेंगे ? जो लोग बाल्यविवाहके विरोधी हैं, वे भी यौवन-विवाहका विरोध नहीं करते, और विरोध करनेसे भी काम नहीं चल सकता । अंगरेज-राजकर्मचारियों ने भी लौकिक विवाह आईन अर्थात् सन् १८७२ ई में विवाहके योग्य अवस्थाकी न्यून-सीमा पुरुषके लिए अठारह वर्ष और स्त्रीके लिए चौदह वर्ष निश्चित की है । अतएव विवाहका यथासभंव समय चाहे जो निश्चित हो, वर-कन्याका परस्पर चुनाव केवल उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर होने देना कभी युक्तिसिद्ध नहीं होगा। उसके बारेमें उनके पिता-माता या अन्य किसी नगीची अभिभावककी सलाह लेनेकी आवश्यकता अवश्य रहगी। परन्तु विवाहका समय उल्लिखित अल्प अवस्थाकी अपेक्षा और भी दो-चार वर्प अधिक होनेसे जैसा कोमल, परिवर्तनयोग्य और गुरुजनोंकी इच्छाका अनुगामी रहता है वैसा अवस्था बढ़नेके साथसाथ फिर नहीं रहता, क्रमशः कठिन, अपरिवर्तनीय और स्वेच्छानुवर्ती हो उठता है। इसीसे यौवनविवाह में वर-कन्याके निर्वाचनमें गुरुजनोंके उपदेशका यथेष्ट प्रयोजन रहता है, अथच वह उपदेश अपनी इच्छाके विरूद्ध होने पर उसे ग्रहण करनेमें अनिच्छा अतिप्रबल हो उठती है, और अनेक स्थलों में वह अनिच्छा उस प्रयोजनकी उपलब्धि भी मनमें नहीं होने देती।
इसके सिवा और भी एक बड़ी भारी बात है । यौवन-विवाहमें वरकन्या दोनोंके परस्परके चुनावमें कुछ समर्थ होनेपर भी, अगर उनसे भूल हो, अर्थात् अगर विवाहसम्बन्धी चुनाव के बाद स्वामी और स्त्री दोनों यह