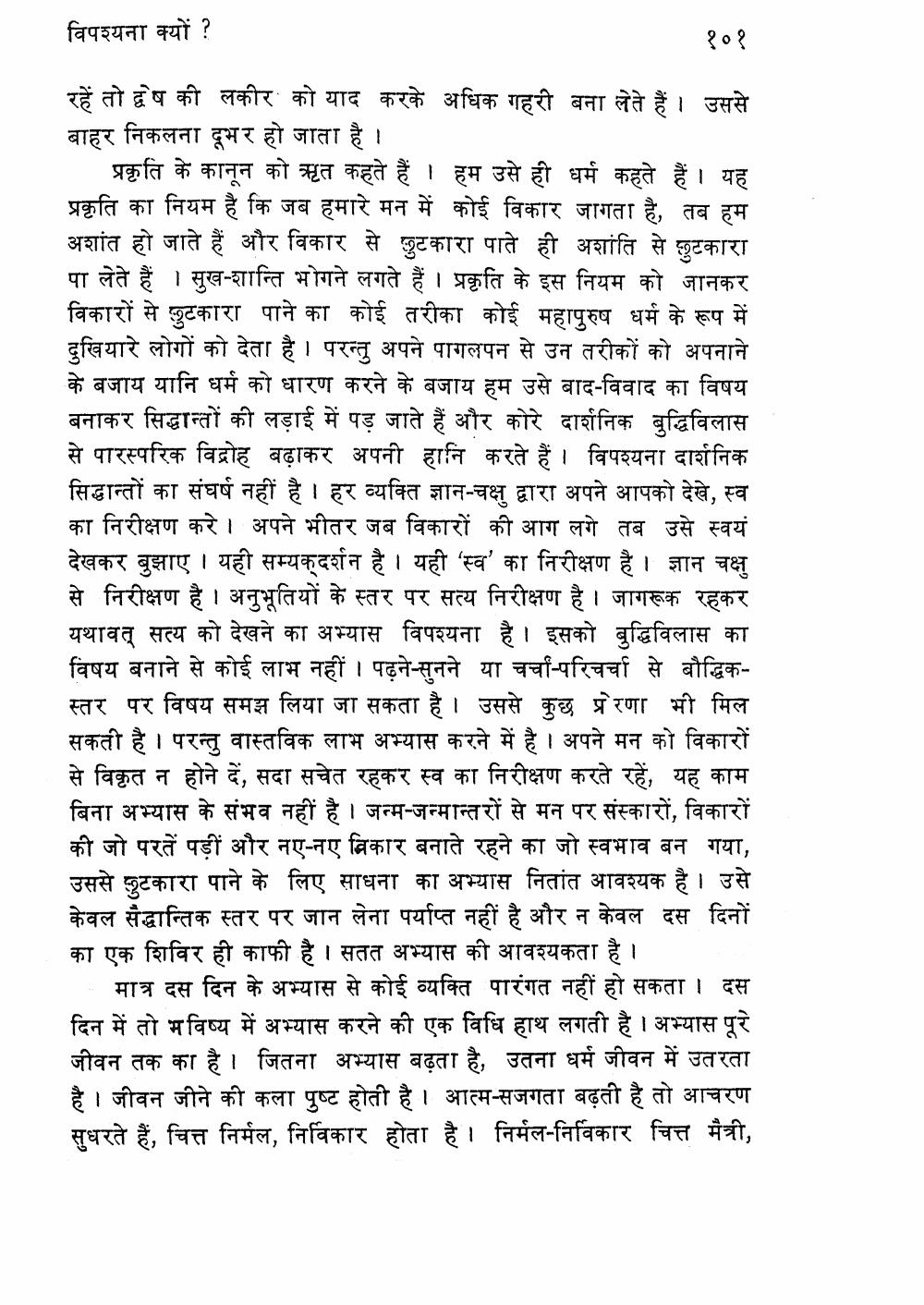________________
विपश्यना क्यों ?
१०१
रहें तो द्वेष की लकीर को याद करके अधिक गहरी बना लेते हैं। उससे बाहर निकलना दूभर हो जाता है ।
प्रकृति के कानून को ऋत कहते हैं । हम उसे ही धर्म कहते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि जब हमारे मन में कोई विकार जागता है, तब हम अशांत हो जाते हैं और विकार से छुटकारा पाते ही अशांति से छुटकारा पा लेते हैं । सुख-शान्ति भोगने लगते हैं । प्रकृति के इस नियम को जानकर विकारों से छुटकारा पाने का कोई तरीका कोई महापुरुष धर्म के रूप में दुखियारे लोगों को देता है। परन्तु अपने पागलपन से उन तरीकों को अपनाने के बजाय यानि धर्म को धारण करने के बजाय हम उसे बाद-विवाद का विषय बनाकर सिद्धान्तों की लड़ाई में पड़ जाते हैं और कोरे दार्शनिक बुद्धिविलास से पारस्परिक विद्रोह बढ़ाकर अपनी हानि करते हैं। विपश्यना दार्शनिक सिद्धान्तों का संघर्ष नहीं है। हर व्यक्ति ज्ञान-चक्षु द्वारा अपने आपको देखे, स्व का निरीक्षण करे। अपने भीतर जब विकारों की आग लगे तब उसे स्वयं देखकर बुझाए । यही सम्यक्दर्शन है । यही 'स्व' का निरीक्षण है। ज्ञान चक्षु से निरीक्षण है । अनुभूतियों के स्तर पर सत्य निरीक्षण है । जागरूक रहकर यथावत् सत्य को देखने का अभ्यास विपश्यना है। इसको बुद्धिविलास का विषय बनाने से कोई लाभ नहीं । पढ़ने-सुनने या चर्चा परिचर्चा से बौद्धिकस्तर पर विषय समझ लिया जा सकता है। उससे कुछ प्रेरणा भी मिल सकती है। परन्तु वास्तविक लाभ अभ्यास करने में है । अपने मन को विकारों से विकृत न होने दें, सदा सचेत रहकर स्व का निरीक्षण करते रहें, यह काम बिना अभ्यास के संभव नहीं है । जन्म-जन्मान्तरों से मन पर संस्कारों, विकारों की जो परतें पड़ी और नए-नए विकार बनाते रहने का जो स्वभाव बन गया, उससे छुटकारा पाने के लिए साधना का अभ्यास नितांत आवश्यक है। उसे केवल सैद्धान्तिक स्तर पर जान लेना पर्याप्त नहीं है और न केवल दस दिनों का एक शिविर ही काफी है । सतत अभ्यास की आवश्यकता है। ____ मात्र दस दिन के अभ्यास से कोई व्यक्ति पारंगत नहीं हो सकता। दस दिन में तो मविष्य में अभ्यास करने की एक विधि हाथ लगती है । अभ्यास पूरे जीवन तक का है। जितना अभ्यास बढ़ता है, उतना धर्म जीवन में उतरता है। जीवन जीने की कला पुष्ट होती है। आत्म-सजगता बढ़ती है तो आचरण सुधरते हैं, चित्त निर्मल, निर्विकार होता है। निर्मल-निर्विकार चित्त मैत्री,