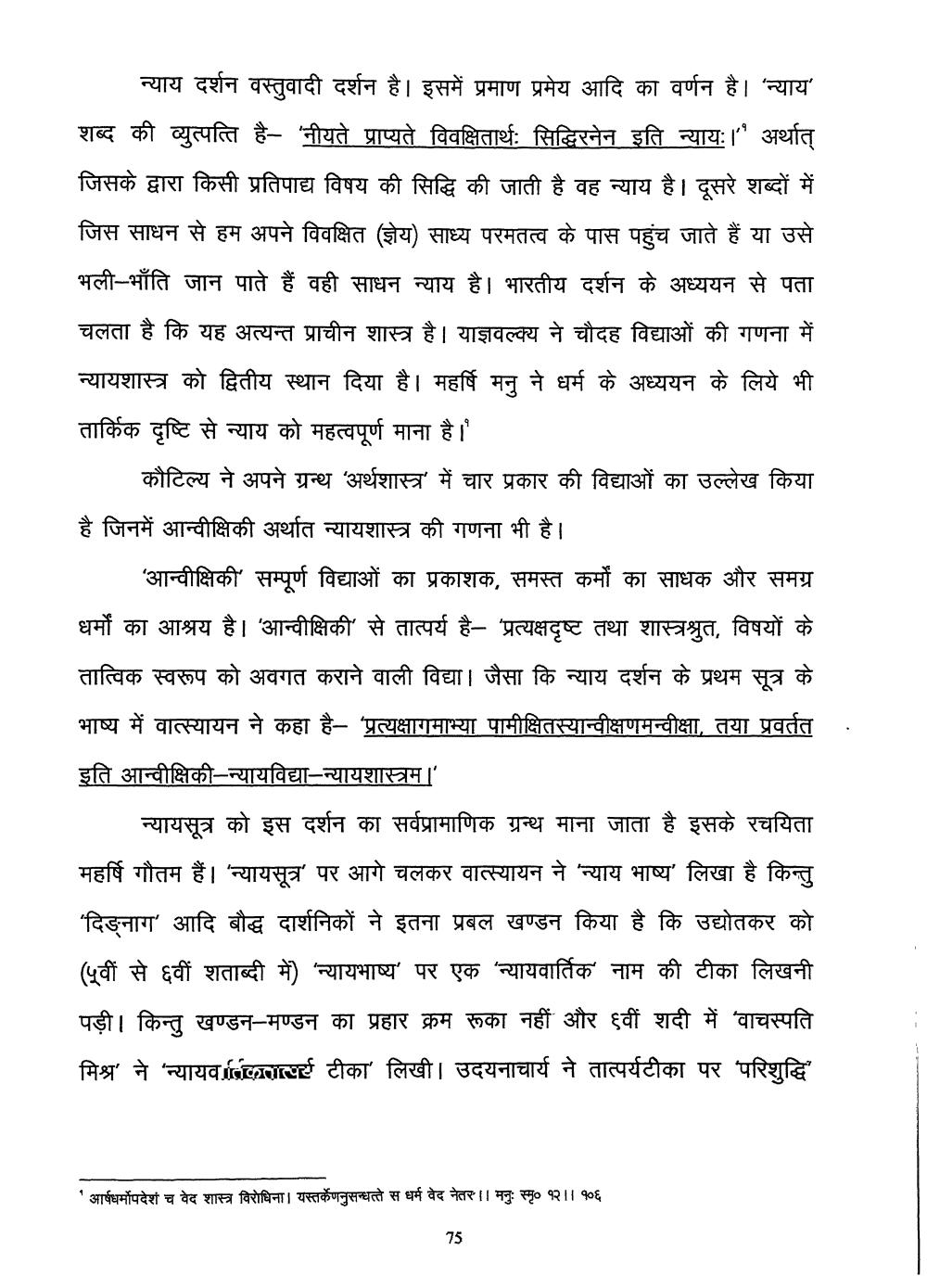________________
न्याय दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। इसमें प्रमाण प्रमेय आदि का वर्णन है। 'न्याय' शब्द की व्युत्पत्ति है- "नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थः सिद्धिरनेन इति न्यायः।" अर्थात् जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि की जाती है वह न्याय है। दूसरे शब्दों में जिस साधन से हम अपने विवक्षित (ज्ञेय) साध्य परमतत्व के पास पहुंच जाते हैं या उसे भली-भाँति जान पाते हैं वही साधन न्याय है। भारतीय दर्शन के अध्ययन से पता चलता है कि यह अत्यन्त प्राचीन शास्त्र है। याज्ञवल्क्य ने चौदह विद्याओं की गणना में न्यायशास्त्र को द्वितीय स्थान दिया है। महर्षि मनु ने धर्म के अध्ययन के लिये भी तार्किक दृष्टि से न्याय को महत्वपूर्ण माना है।'
कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र' में चार प्रकार की विद्याओं का उल्लेख किया है जिनमें आन्वीक्षिकी अर्थात न्यायशास्त्र की गणना भी है।
'आन्वीक्षिकी सम्पूर्ण विद्याओं का प्रकाशक, समस्त कर्मों का साधक और समग्र धर्मों का आश्रय है। 'आन्वीक्षिकी' से तात्पर्य है- 'प्रत्यक्षदृष्ट तथा शास्त्रश्रुत, विषयों के तात्विक स्वरूप को अवगत कराने वाली विद्या। जैसा कि न्याय दर्शन के प्रथम सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन ने कहा है- 'प्रत्यक्षागमाभ्या पामीक्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा, तया प्रवर्तत इति आन्वीक्षिकी-न्यायविद्या-न्यायशास्त्रम।'
न्यायसूत्र को इस दर्शन का सर्वप्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है इसके रचयिता महर्षि गौतम हैं। 'न्यायसूत्र' पर आगे चलकर वात्स्यायन ने 'न्याय भाष्य' लिखा है किन्तु 'दिङ्नाग' आदि बौद्ध दार्शनिकों ने इतना प्रबल खण्डन किया है कि उद्योतकर को (५वीं से ६वीं शताब्दी में) 'न्यायभाष्य' पर एक 'न्यायवार्तिक' नाम की टीका लिखनी पड़ी। किन्तु खण्डन-मण्डन का प्रहार क्रम रूका नहीं और ६वीं शदी में ‘वाचस्पति मिश्र' ने 'न्यायवार्तिकवाट टीका' लिखी। उदयनाचार्य ने तात्पर्यटीका पर 'परिशुद्धि'
'आर्षधर्मोपदेशं च वेद शास्त्र विरोधिना। यस्तणनुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतर ।। मनुः स्मृ० १२ ।। १०६
75