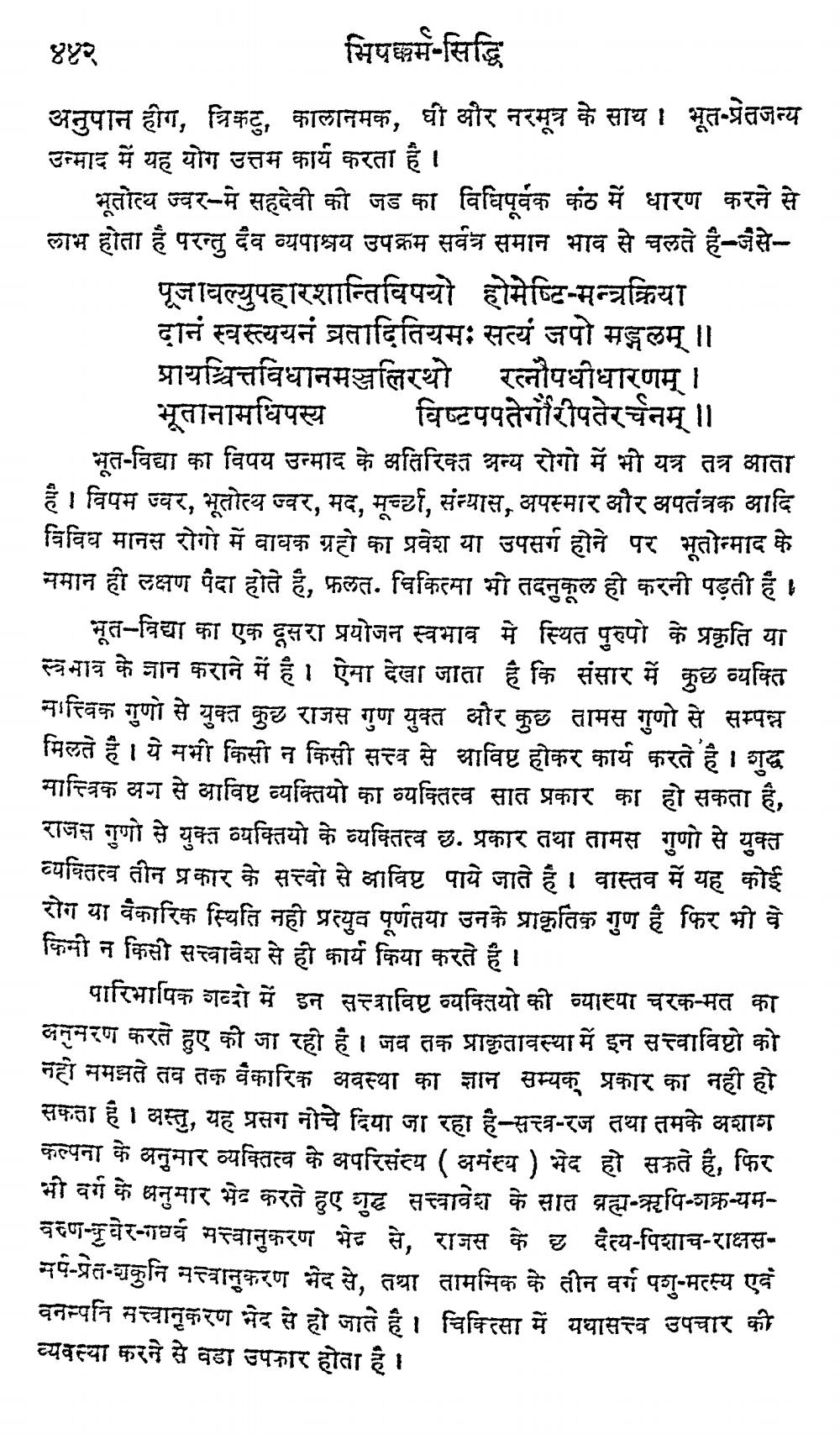________________
४४२
भिपक्षम-सिद्धि अनुपान होग, त्रिकटु, कालानमक, घी और नरमूत्र के साथ । भूत-प्रेतजन्य उन्माद में यह योग उत्तम कार्य करता है ।
भूतोत्य ज्वर-मे सहदेवी को जड का विधिपूर्वक कंठ में धारण करने से लाभ होता है परन्तु दैव व्यपाश्रय उपक्रम सर्वत्र समान भाव से चलते है-जैसे
पूजावल्युपहारशान्तिविपयो होमेष्टि-मन्त्रक्रिया दानं स्वस्त्ययनं व्रतादितियमः सत्यं जपो मङ्गलम् ।। प्रायश्चित्तविधानमञ्जलिरथो रत्नौषधीधारणम् ।
भूतानामधिपस्य विष्टपपतेर्गौरीपतेरचनम् ।। भूत-विद्या का विषय उन्माद के अतिरिक्त अन्य रोगो में भी यत्र तत्र आता है । विषम ज्वर, भूतोत्थ ज्वर, मद, मूर्छा, संन्यास, अपस्मार और अपतंत्रक आदि विविध मानस रोगो में वावक ग्रहो का प्रवेश या उपसर्ग होने पर भूतोन्माद के समान ही लक्षण पैदा होते है, फलत. चिकित्सा भो तदनुकूल हो करनी पड़ती है ।
भूत-विद्या का एक दूसरा प्रयोजन स्वभाव में स्थित पुरुपो के प्रकृति या स्वभाव के ज्ञान कराने में है। ऐमा देखा जाता है कि संसार में कुछ व्यक्ति मात्त्विक गुणो से युक्त कुछ राजस गुण युक्त और कुछ तामस गुणो से सम्पन्न मिलते है। ये मभी किसी न किसी सत्त्व से आविष्ट होकर कार्य करते है । शुद्ध मात्त्विक मग से आविष्ट व्यक्तियो का व्यक्तित्व सात प्रकार का हो सकता है, राजस गुणो से युक्त व्यक्तियो के व्यक्तित्व छ. प्रकार तथा तामस गुणो से युक्त व्यक्तित्व तीन प्रकार के सत्त्वो से आविष्ट पाये जाते है। वास्तव में यह कोई रोग या वैकारिक स्थिति नही प्रत्युव पर्णतया उनके प्राकृतिक गुण है फिर भी वे किमी न किसी सत्त्वावेश से ही कार्य किया करते है।
पारिभाषिक शब्दो में इन सत्त्वाविष्ट व्यक्तियो की व्याख्या चरक-मत का मनमरण करते हुए की जा रही है। जब तक प्राकृतावस्था में इन सत्त्वाविष्टो को नहीं समझते तव तक वैकारिक अवस्था का ज्ञान सम्यक् प्रकार का नही हो सकता है । यस्तु, यह प्रसग नीचे दिया जा रहा है-सत्र-रज तथा तमके अशाश कल्पना के अनुसार व्यक्तित्व के अपरिसंत्य (असंस्य ) भेद हो सकते है, फिर भी वर्ग के अनुमार भेट करते हुए शुद्ध सत्वावेश के सात ब्रह्म-ऋपि-गक्र-यमवक्षण-बेर-गर्व मत्त्वानुकरण भेट से, राजस के छ दैत्य-पिशाच-राक्षसमप-प्रेत-शकुनि सत्त्वानुकरण भेद से, तथा तामनिक के तीन वर्ग पशु-मत्स्य एवं वनस्पति सत्त्वानुकरण भेद से हो जाते है। चिकित्सा में यथासत्त्व उपचार की व्यवस्था करने से बडा उपकार होता है।