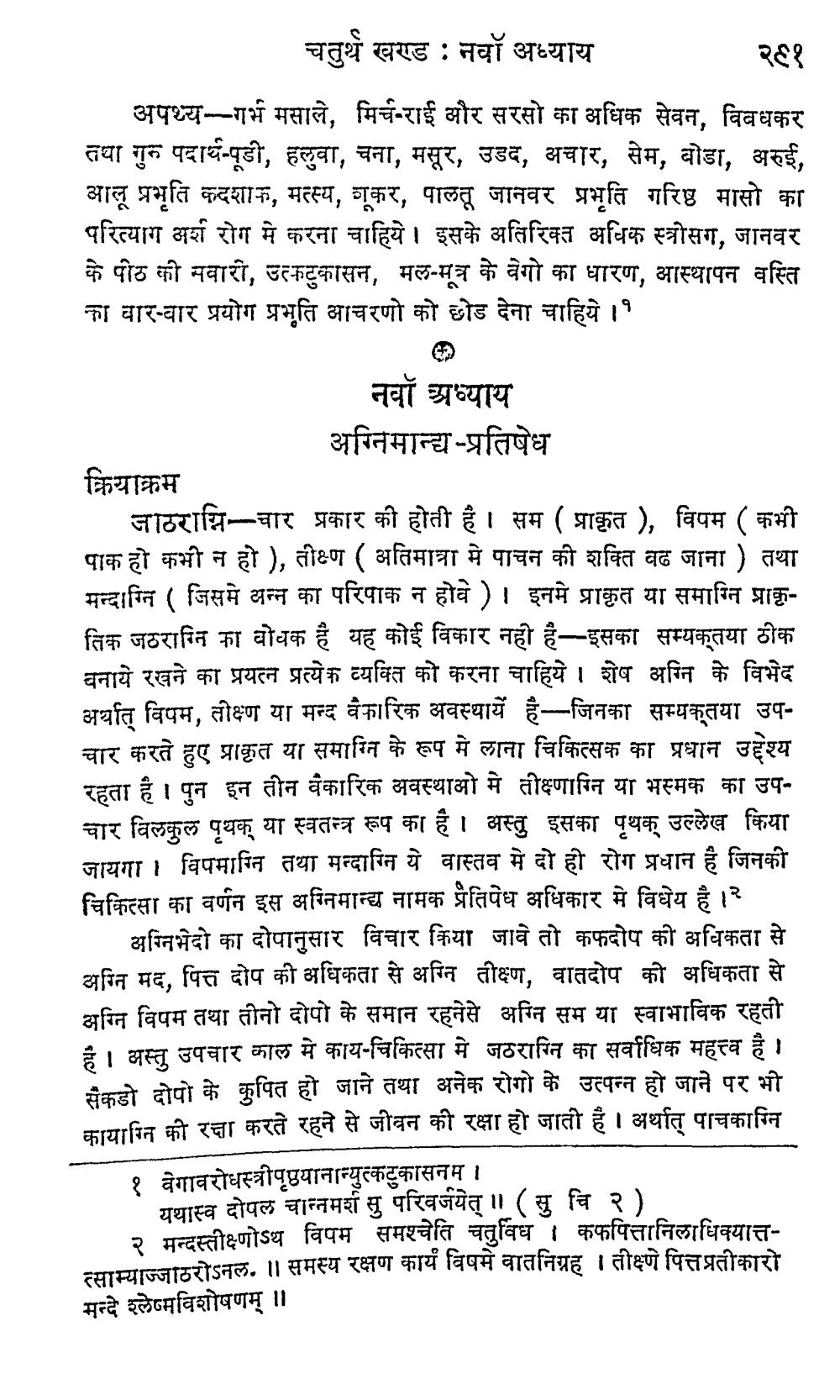________________
त्या गुरू पदार्थ-शाक, मत्स्य, बाहये । इसके अवि का धार
चतुर्थ खण्ड : नवॉ अध्याय
२६१ अपथ्य-गर्भ मसाले, मिर्च-राई और सरसो का अधिक सेवन, विवधकर तथा गुरु पदार्थ-पूडी, हलुवा, चना, मसूर, उडद, अचार, सेम, वोडा, अरुई, आलू प्रभृति कदशाक, मत्स्य, शूकर, पालतू जानवर प्रभृति गरिष्ठ मासो का परित्याग अर्श रोग मे करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अधिक स्त्रीसग, जानवर के पीठ की सवारी, उत्कटुकासन, मल-मूत्र के वेगो का धारण, आस्थापन वस्ति का बार-बार प्रयोग प्रभृति आचरणो को छोड देना चाहिये ।'
नवॉ अध्याय
अग्निमान्द्य-प्रतिषेध क्रियाक्रम
जाठराग्नि–चार प्रकार की होती है। सम (प्राकृत ), विपम ( कभी पाक हो कभी न हो ), तीक्ष्ण ( अतिमात्रा मे पाचन की शक्ति बढ जाना ) तथा मन्दाग्नि ( जिसमे अन्न का परिपाक न होवे )। इनमे प्राकृत या समाग्नि प्राकृतिक जठराग्नि का वोचक है यह कोई विकार नही है-इसका सम्यक्तया ठीक बनाये रखने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिये। शेष अग्नि के विभेद अर्थात् विपम, तीक्ष्ण या मन्द वैकारिक अवस्थायें है-जिनका सम्यक्तया उपचार करते हुए प्राकृत या समाग्नि के रूप मे लाना चिकित्सक का प्रधान उद्देश्य रहता है । पुन इन तीन वैकारिक अवस्थामओ मे तीक्ष्णाग्नि या भस्मक का उपचार विलकुल पृथक् या स्वतन्त्र रूप का है। अस्तु इसका पृथक् उल्लेख किया जायगा। विपमाग्नि तथा मन्दाग्नि ये वास्तव में दो ही रोग प्रधान है जिनकी चिकित्सा का वर्णन इस अग्निमान्य नामक प्रतिपेध अधिकार मे विधेय है ।२
अग्निभेदो का दोपानुसार विचार किया जावे तो कफदोप की अधिकता से अग्नि मद, पित्त दोप की अधिकता से अग्नि तीक्ष्ण, वातदोप की अधिकता से अग्नि विषम तथा तीनो दोपो के समान रहनेसे अग्नि सम या स्वाभाविक रहती है। अस्तु उपचार काल मे काय-चिकित्सा मे जठराग्नि का सर्वाधिक महत्त्व है। औलो दोपो के कुपित हो जाने तथा अनेक रोगो के उत्पन्न हो जाने पर भी कायानि की रक्षा करते रहने से जीवन की रक्षा हो जाती है । अर्थात् पाचकाग्नि १ वेगावरोधस्त्रीपृष्ठयानान्युत्कटुकासनम ।
यथास्व दोपल चान्नमर्श सु परिवर्जयेत् ॥ (सु चि २) २ मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विपम समश्चेति चतुर्विध । कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठरोऽनल. ॥ समस्य रक्षण कार्य विषमे वातनिग्रह । तीक्ष्णे पित्तप्रतीकारो मन्दे श्लेष्मविशोषणम् ॥