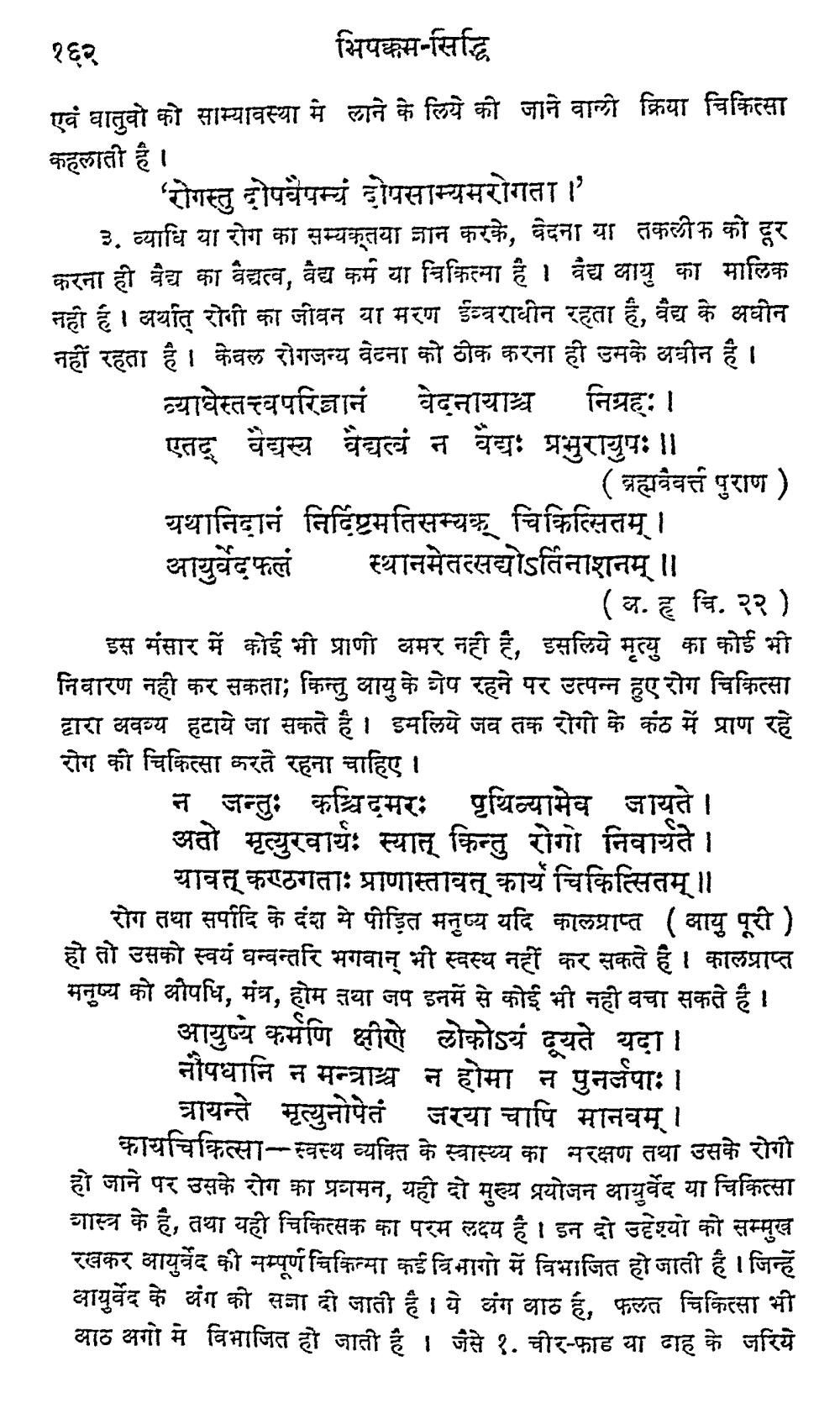________________
१६२
भिपक्कम-सिद्धि
एवं धातुवो को साम्यावस्था में लाने के लिये की जाने वाली क्रिया चिकित्सा कहलाती है ।
'रोगस्तु दोषवैपम्यं दोपसाम्यमरोगता ।'
३. व्याधि या रोग का सम्यक्तया ज्ञान करके, वेदना या तकलीफ को दूर करना ही वैद्य का वैद्यत्व, वैद्य कर्म या चिकित्मा है । वैद्य आयु का मालिक नही है । अर्थात् रोगी का जीवन या मरण ईव्वराधीन रहता है, वैद्य के अधीन नहीं रहता है । केवल रोगजन्य वेदना को ठीक करना ही उसके अधीन है | व्याधेस्तत्त्व परिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः । एतद् वैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्यः प्रभुरायुपः ॥
(ब्रह्मवैवर्त पुराण )
यथानिदानं निर्दिष्टमतिसम्यक् चिकित्सितम् । आयुर्वेद फलं स्थानमेतत्सद्योऽर्तिनाशनम् ॥
(अ. हृ चि. २२ )
इस संसार में कोई भी प्राणी अमर नही है, इसलिये मृत्यु का कोई भी निवारण नही कर सकता; किन्तु आयु के शेष रहने पर उत्पन्न हुए रोग चिकित्सा द्वारा अवग्य हटाये जा सकते है । इमलिये जव तक रोगो के कंठ में प्राण रहे रोग की चिकित्सा करते रहना चाहिए ।
न जन्तुः कश्चिदमरः
पृथिव्यामेव जायते । अतो मृत्युरवार्यः स्यात् किन्तु रोगो निवार्यते । यावत् कण्ठगताः प्राणास्तावत् कार्य चिकित्सितम् ॥
रोग तथा सर्पादि के दंश मे पीड़ित मनुष्य यदि कालप्राप्त ( आयु पूरी ) हो तो उसको स्वयं धन्वन्तरि भगवान् भी स्वस्थ नहीं कर सकते है । कालप्राप्त मनुष्य को औषधि, मंत्र, होम तथा जप इनमें से कोई भी नही बचा सकते है | आयुष्ये कर्मणि क्षीणे लोकोऽयं दूयते यदा । नौपधानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनर्तपाः । त्रायन्ते मृत्युनोपेतं जरया चापि मानवम् । कायचिकित्सा - स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का मरक्षण तथा उसके रोगी हो जाने पर उसके रोग का प्रशमन, यही दो मुख्य प्रयोजन आयुर्वेद या चिकित्सा शास्त्र के है, तथा यही चिकित्सक का परम लक्ष्य है । इन दो उद्देश्यो को सम्मुख रखकर आयुर्वेद की सम्पूर्ण चिकित्सा कई विभागो में विभाजित हो जाती हैं । जिन्हें वायुर्वेद के अंग की सजा दी जाती है । ये अंग आठ है, फलत चिकित्सा भी या अगो मे विभाजित हो जाती है । जैसे १. चीर-फाड या ढाह के जरिये