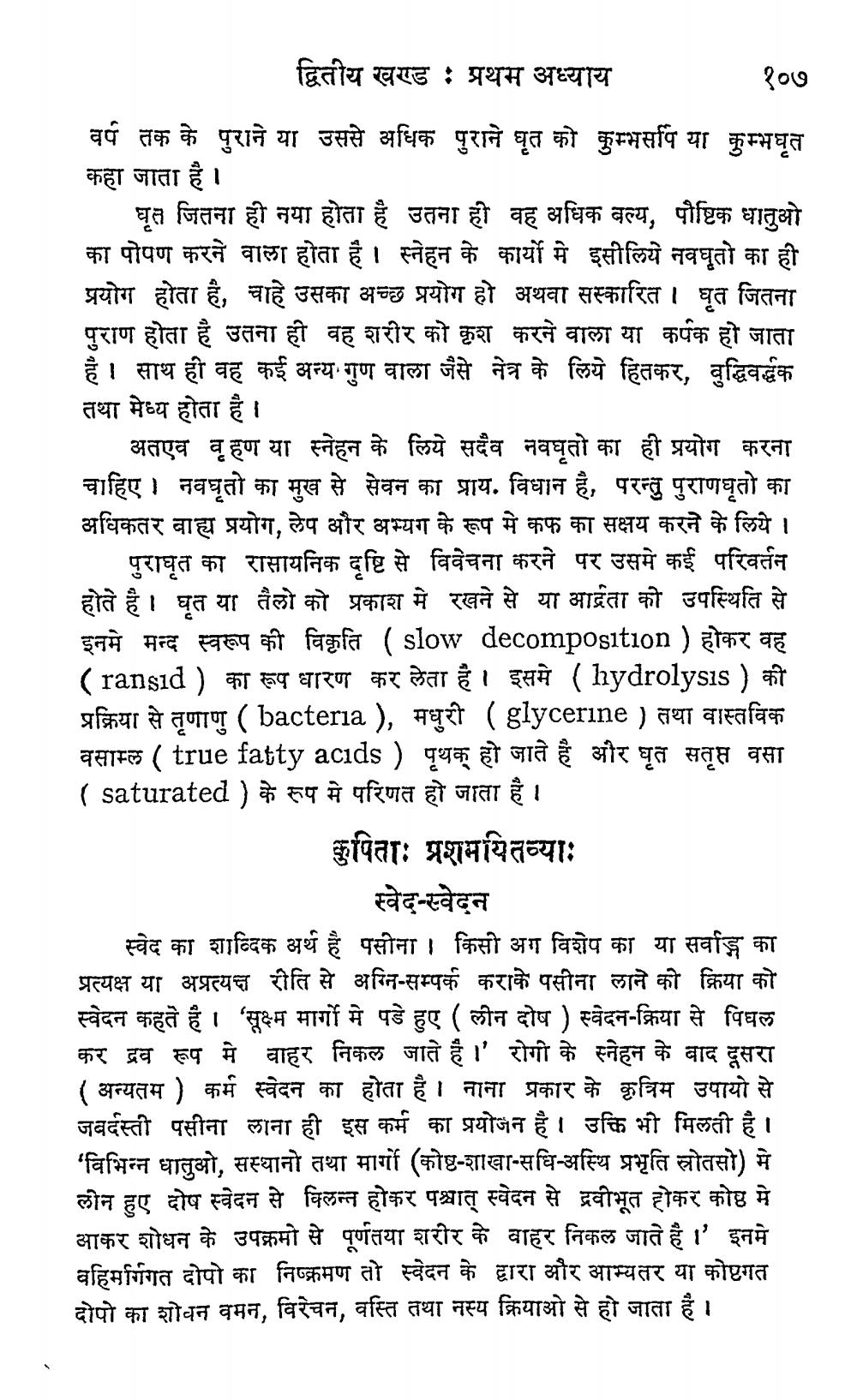________________
द्वितीय खण्ड : प्रथम अध्याय १०७ वर्ष तक के पुराने या उससे अधिक पुराने घृत को कुम्भसपि या कुम्भघृत कहा जाता है।
घृत जितना ही नया होता है उतना ही वह अधिक बल्य, पौष्टिक धातुओ का पोपण करने वाला होता है । स्नेहन के कार्यो मे इसीलिये नवघृतो का ही प्रयोग होता है, चाहे उसका अच्छ प्रयोग हो अथवा सस्कारित । घृत जितना पुराण होता है उतना ही वह शरीर को कृश करने वाला या कर्पक हो जाता है। साथ ही वह कई अन्य गुण वाला जैसे नेत्र के लिये हितकर, बुद्धिवर्द्धक तथा मेध्य होता है।
अतएव वृहण या स्नेहन के लिये सदैव नवघतो का ही प्रयोग करना चाहिए। नवघृतो का मुख से सेवन का प्राय. विधान है, परन्तु पुराणघृतो का अधिकतर बाह्य प्रयोग, लेप और अभ्यग के रूप मे कफ का सक्षय करने के लिये ।
पुराघृत का रासायनिक दृष्टि से विवेचना करने पर उसमे कई परिवर्तन होते है। घृत या तैलो को प्रकाश मे रखने से या आर्द्रता को उपस्थिति से इनमे मन्द स्वरूप की विकृति ( slow decomposition ) होकर वह (ransid ) का रूप धारण कर लेता है। इसमे ( hydrolysis ) की प्रक्रिया से तृणाणु ( bacteria.), मधुरी (glycerine ) तथा वास्तविक वसाम्ल ( true fatty acids ) पृथक् हो जाते है और घृत सतृप्त वसा ( saturated ) के रूप मे परिणत हो जाता है ।
कुपिताः प्रशमयितव्याः
स्वेद-स्वेदन स्वेद का शाब्दिक अर्थ है पसीना । किसी अग विशेप का या सर्वाङ्ग का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से अग्नि-सम्पर्क कराके पसीना लाने की क्रिया को स्वेदन कहते है । 'सूक्ष्म मार्गो मे पडे हुए (लीन दोष ) स्वेदन-क्रिया से पिघल कर द्रव रूप मे बाहर निकल जाते है ।' रोगी के स्नेहन के बाद दूसरा ( अन्यतम ) कर्म स्वेदन का होता है। नाना प्रकार के कृत्रिम उपायो से जबर्दस्ती पसीना लाना ही इस कर्म का प्रयोजन है। उक्ति भी मिलती है । 'विभिन्न धातुओ, सस्थानो तथा मार्गो (कोष्ठ-शाखा-सधि-अस्थि प्रभृति स्रोतसो) मे लीन हुए दोष स्वेदन से क्लिन्न होकर पश्चात् स्वेदन से द्रवीभूत होकर कोष्ठ मे आकर शोधन के उपक्रमो से पूर्णतया शरीर के बाहर निकल जाते है ।' इनमे वहिर्गिगत दोपो का निष्क्रमण तो स्वेदन के द्वारा और आभ्यतर या कोष्टगत दोपो का शोवन वमन, विरेचन, वस्ति तथा नस्य क्रियाओ से हो जाता है ।