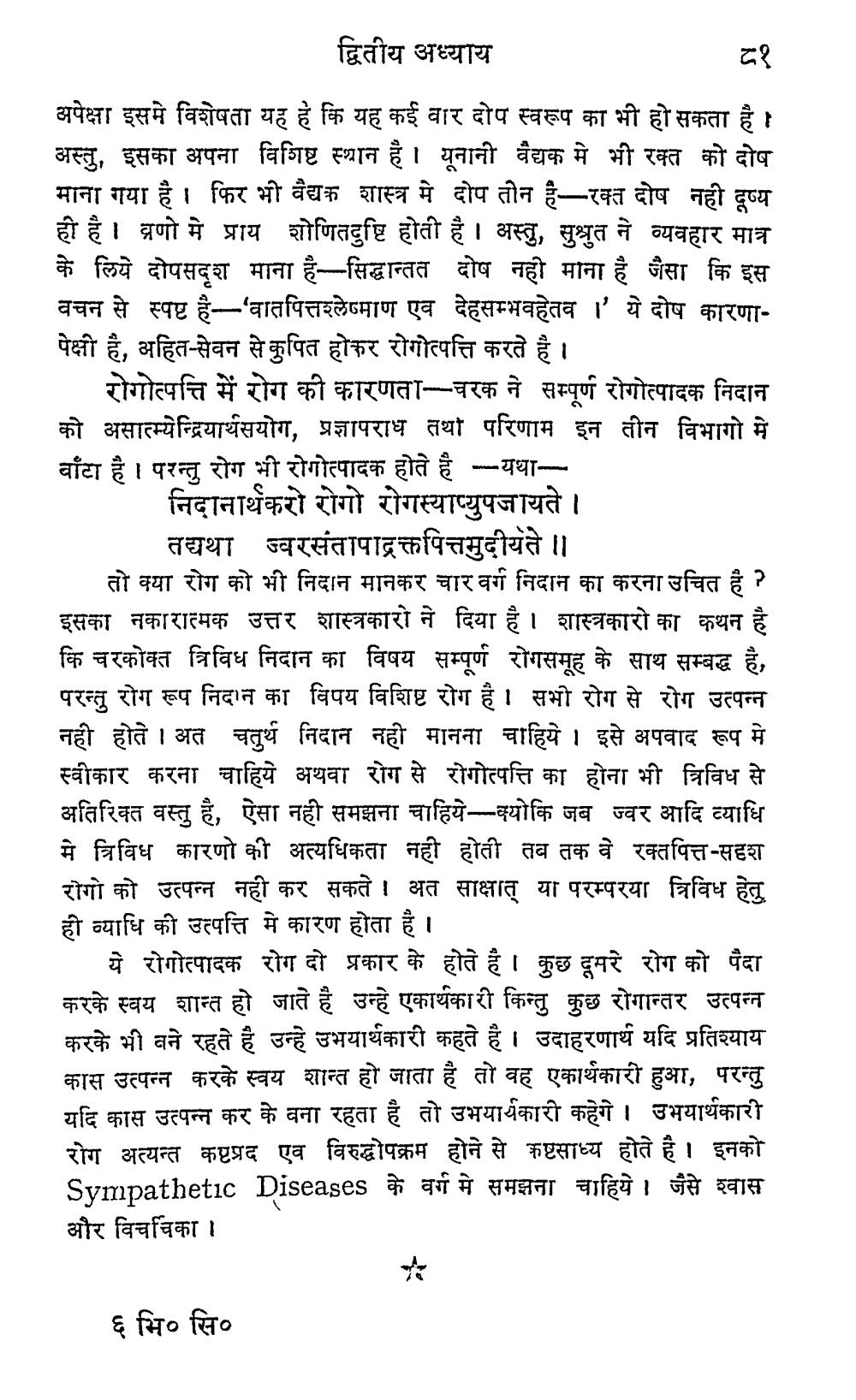________________
द्वितीय अध्याय
८१
अपेक्षा इसमे विशेषता यह है कि यह कई वार दोप स्वरूप का भी हो सकता है । अस्तु, इसका अपना विशिष्ट स्थान है। यूनानी वैद्यक में भी रक्त को दोष माना गया है । फिर भी वैद्यक शास्त्र में दोप तीन है— रक्त दोष नही दृष्य ही है । व्रणो मे प्राय शोणितदुष्टि होती है । अस्तु, सुश्रुत ने व्यवहार मात्र के लिये दोपसदृश माना है - सिद्धान्तत दोष नही माना है जैसा कि इस वचन से स्पष्ट है - ' वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भवहेतव ।' ये दोष कारणापेक्षी है, अहित सेवन से कुपित होकर रोगोत्पत्ति करते है ।
रोगोत्पत्ति में रोग की कारणता - चरक ने सम्पूर्ण रोगोत्पादक निदान को असात्म्येन्द्रियार्थसयोग, प्रज्ञापराध तथा परिणाम इन तीन विभागो मे बाँटा है । परन्तु रोग भी रोगोत्पादक होते हैं
-यथा---
निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते । तद्यथा ज्वरसंतापाद्रक्तपित्तमुदीयते ॥
तो क्या रोग को भी निदान मानकर चार वर्ग निदान का करना उचित है ? इसका नकारात्मक उत्तर शास्त्रकारो ने दिया है । शास्त्रकारो का कथन है कि चरकोक्त त्रिविध निदान का विषय सम्पूर्ण रोगसमूह के साथ सम्बद्ध है, परन्तु रोग रूप निदान का विषय विशिष्ट रोग है । सभी रोग से रोग उत्पन्न नही होते । अत चतुर्थ निदान नही मानना चाहिये । इसे अपवाद रूप मे स्वीकार करना चाहिये अथवा रोग से रोगोत्पत्ति का होना भी त्रिविध से अतिरिक्त वस्तु है, ऐसा नही समझना चाहिये क्योकि जब ज्वर आदि व्याधि मे त्रिविध कारणो की अत्यधिकता नही होती तब तक वे रक्तपित्त- सहश रोगो को उत्पन्न नही कर सकते । अत साक्षात् या परम्परया त्रिविध हेतु ही व्याधि की उत्पत्ति में कारण होता है ।
ये रोगोत्पादक रोग दो प्रकार के होते हैं । कुछ दूसरे रोग को पैदा करके स्वय शान्त हो जाते है उन्हे एकार्थकारी किन्तु कुछ रोगान्तर उत्पन्न करके भी बने रहते है उन्हें उभयार्थकारी कहते है । उदाहरणार्थ यदि प्रतिश्याय कास उत्पन्न करके स्वय शान्त हो जाता है तो वह एकार्थकारी हुआ, परन्तु यदि कास उत्पन्न कर के बना रहता है तो उभयार्यकारी कहेंगे । उभयार्थकारी रोग अत्यन्त कष्टप्रद एव विरुद्धोपक्रम होने से कष्टसाध्य होते है । इनको Sympathetic Diseases के वर्ग मे समझना चाहिये । जैसे श्वास और विचचिका |
६ भि० सि०