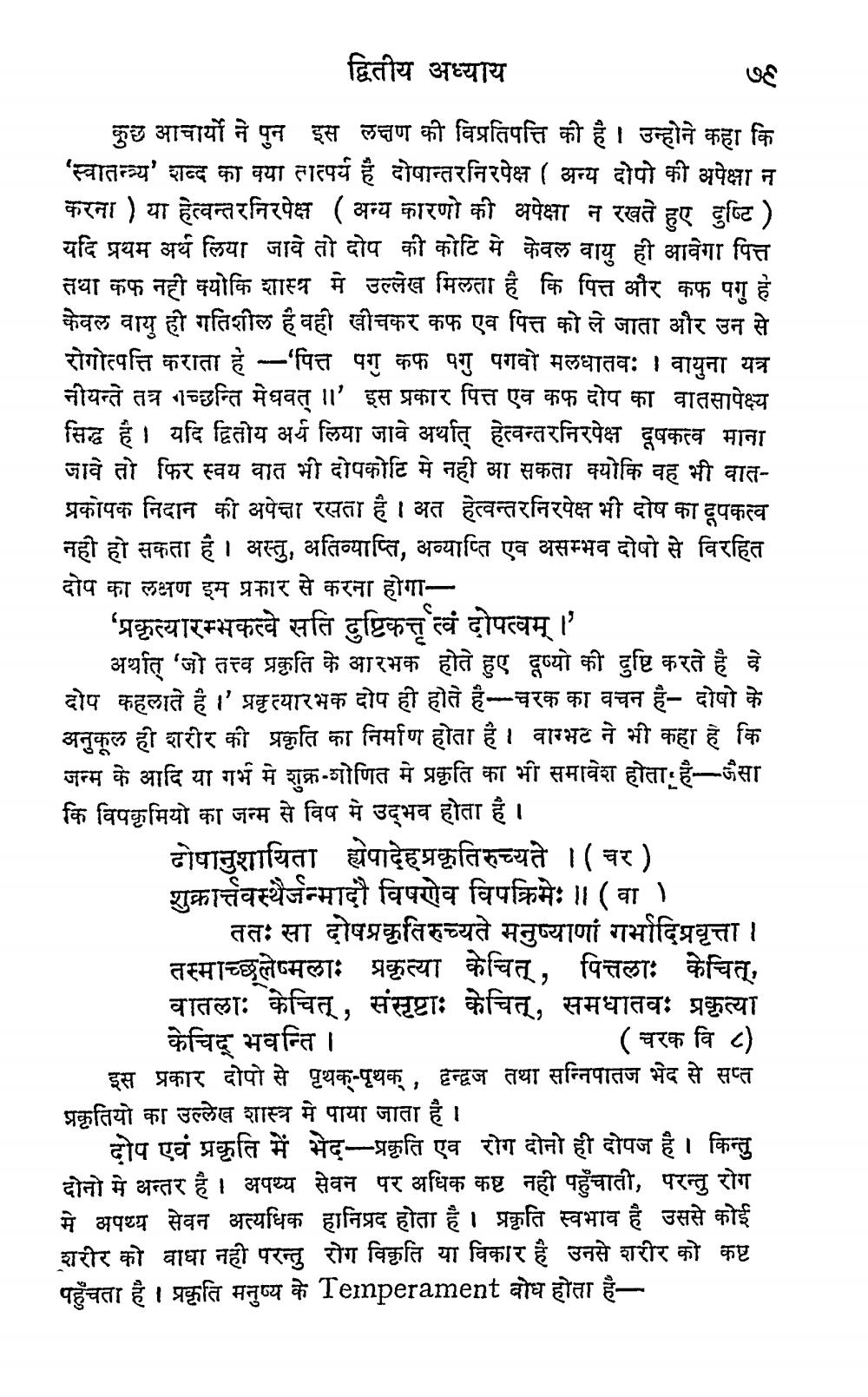________________
द्वितीय अध्याय
७९
कुछ आचार्यों ने पुन इस लक्षण की विप्रतिपत्ति की है। उन्होने कहा कि 'स्वातन्त्र्य' शब्द का क्या तात्पर्य है दोषान्तरनिरपेक्ष ( अन्य दोपो की अपेक्षा न करना ) या हेत्वन्तरनिरपेक्ष ( अन्य कारणो की अपेक्षा न रखते हुए दुष्टि) यदि प्रथम अर्थ लिया जावे तो दोप की कोटि मे केवल वायु ही आवेगा पित्त तथा कफ नहीं क्योकि शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि पित्त और कफ पग है केवल वायु ही गतिशील है वही खीचकर कफ एव पित्त को ले जाता और उन से रोगोत्पत्ति कराता है -'पित्त पगु कफ पगु पगवो मलधातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत् ॥' इस प्रकार पित्त एव कफ दोप का वातसापेक्ष्य सिद्ध है। यदि द्वितीय अर्थ लिया जावे अर्थात् हेत्वन्तरनिरपेक्ष दूषकत्व माना जावे तो फिर स्वय वात भी दोपकोटि मे नही आ सकता क्योकि वह भी वातप्रकोपक निदान की अपेक्षा रसता है । अत हेत्वन्तरनिरपेक्ष भी दोष का दूपकत्व नही हो सकता है। अस्तु, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति एव असम्भव दोषो से विरहित दोप का लक्षण इस प्रकार से करना होगा
'प्रकृत्यारम्भकत्वे सति दुष्टिकत्तु त्वं दोपत्वम् ।'
अर्थात् 'जो तत्त्व प्रकृति के आरभक होते हुए दूष्यो की दुष्टि करते है दे दोप कहलाते है ।' प्रकृत्यारभक दोप ही होते है-चरक का वचन है- दोषो के अनुकूल ही शरीर की प्रकृति का निर्माण होता है। वाग्भट ने भी कहा है कि जन्म के आदि या गर्भ मे शुक्र-गोणित मे प्रकृति का भी समावेश होता है-जैसा कि विपकृमियो का जन्म से विष मे उद्भव होता है ।
दोषानुशायिता ह्येपादेहप्रकृतिरुच्यते । ( चर) शुक्रावस्थैर्जन्मादौ विषणेव विपक्रिमेः ।। ( वा ) ___ततः सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां गर्भादिप्रवृत्ता। तस्माच्छ्लेष्मलाः प्रकृत्या केचित् , पित्तलाः केचित्, वातलाः केचित् , संसृष्टाः केचित्, समधातवः प्रकृत्या केचिद् भवन्ति ।
(चरक वि ८) इस प्रकार दोपो से पृथक्-पृथक् , द्वन्द्वज तथा सन्निपातज भेद से सप्त प्रकृतियो का उल्लेख शास्त्र में पाया जाता है।
दोप एवं प्रकृति में भेद-प्रकृति एव रोग दोनो ही दोपज है। किन्तु दोनो मे अन्तर है। अपथ्य सेवन पर अधिक कष्ट नही पहुँचाती, परन्तु रोग मे अपथ्य सेवन अत्यधिक हानिप्रद होता है। प्रकृति स्वभाव है उससे कोई शरीर को बाधा नही परन्तु रोग विकृति या विकार है उनसे शरीर को कष्ट पहुँचता है । प्रकृति मनुष्य के Temperament बोध होता है