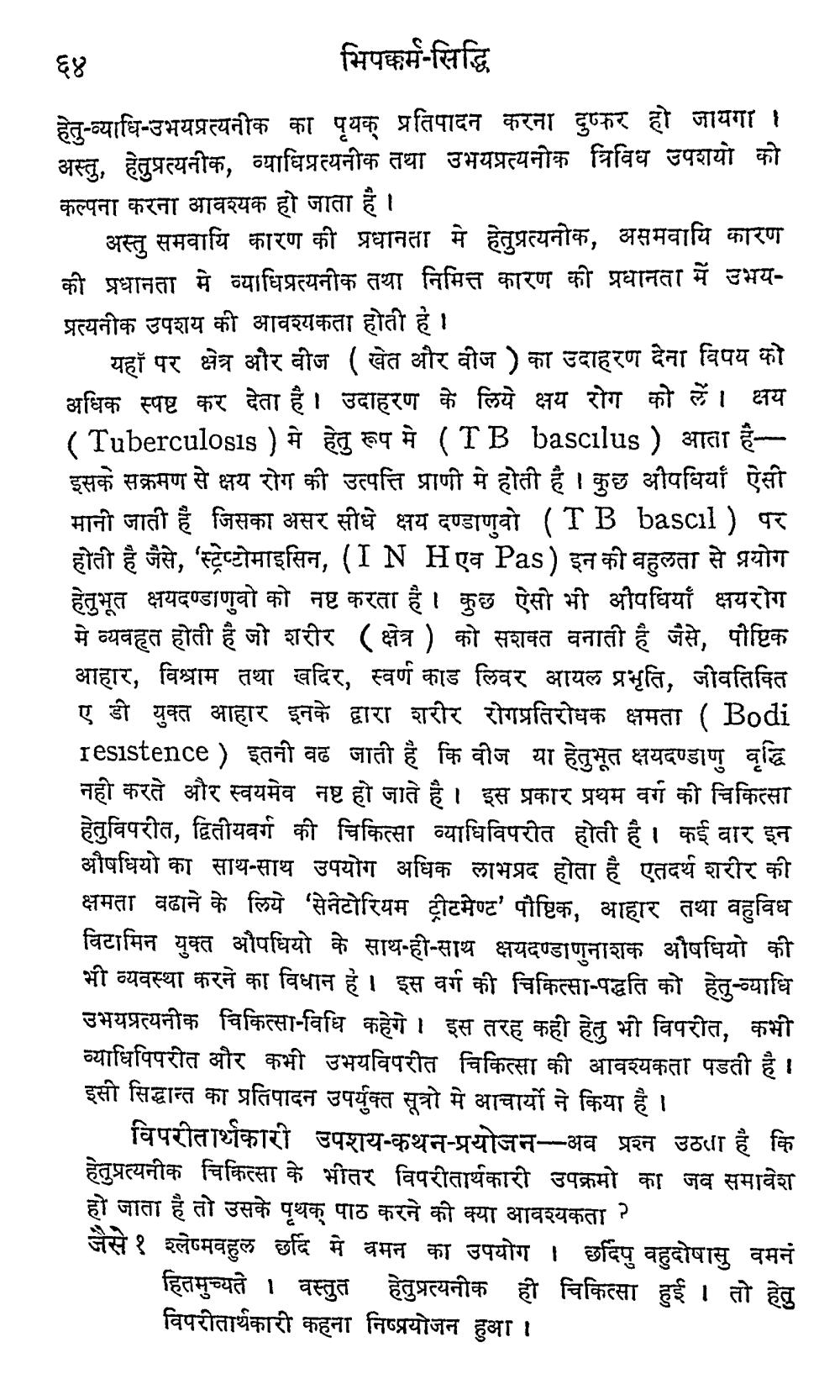________________
भिपकर्म-सिद्धि हेतु-व्याधि-उभयप्रत्यनीक का पृथक् प्रतिपादन करना दुष्कर हो जायगा । अस्तु, हेतुप्रत्यनीक, व्याधिप्रत्यनीक तथा उभयप्रत्यनोक विविध उपशयो को कल्पना करना आवश्यक हो जाता है ।
अस्तु समवायि कारण की प्रधानता मे हेतुप्रत्यनोक, असमवायि कारण की प्रधानता मे व्याधिप्रत्यनीक तथा निमित्त कारण की प्रधानता में उभयप्रत्यनीक उपशय की आवश्यकता होती है।
यहाँ पर क्षेत्र और वीज ( खेत और वीज ) का उदाहरण देना विपय को अधिक स्पष्ट कर देता है। उदाहरण के लिये क्षय रोग को लें। क्षय ( Tuberculosis ) मे हेतु रूप मे (T B_bascilus) आता हैइसके सक्रमण से क्षय रोग की उत्पत्ति प्राणी मे होती है । कुछ औपधियाँ ऐसी मानी जाती है जिसका असर सीधे क्षय दण्डाणुवो (T B_bascil ) पर होती है जैसे, 'स्ट्रेप्टोमाइसिन, (I N Hएव Pas) इन की बहुलता से प्रयोग हेतुभूत क्षयदण्डाणुवो को नष्ट करता है। कुछ ऐसी भी औपधियाँ क्षयरोग मे व्यवहृत होती है जो शरीर (क्षेत्र ) को सशक्त बनाती है जैसे, पौष्टिक आहार, विश्राम तथा खदिर, स्वर्ण काड लिवर आयल प्रभृति, जीवतिक्ति ए डी युक्त आहार इनके द्वारा शरीर रोगप्रतिरोधक क्षमता ( Bodi resistence ) इतनी वढ जाती है कि वीज या हेतुभूत क्षयदण्डाणु वृद्धि नहीं करते और स्वयमेव नष्ट हो जाते है। इस प्रकार प्रथम वर्ग की चिकित्सा हेतुविपरीत, द्वितीयवर्ग की चिकित्सा व्याधिविपरीत होती है। कई बार इन औषधियो का साथ-साथ उपयोग अधिक लाभप्रद होता है एतदर्थ शरीर की क्षमता बढाने के लिये 'सेनेटोरियम ट्रीटमेण्ट' पौष्टिक, आहार तथा बहुविध विटामिन युक्त औपधियो के साथ-ही-साथ क्षयदण्डाणुनाशक औषधियो की भी व्यवस्था करने का विधान है। इस वर्ग की चिकित्सा पद्धति को हेतु-व्याधि उभयप्रत्यनीक चिकित्सा-विधि कहेगे। इस तरह कही हेतु भी विपरीत, कभी व्याधिपिपरीत और कभी उभयविपरीत चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन उपर्युक्त सूत्रो मे आचार्यों ने किया है।
विपरीतार्थकारी उपशय-कथन-प्रयोजन-अव प्रश्न उठता है कि हेतुप्रत्यनीक चिकित्सा के भीतर विपरीतार्थकारी उपक्रमो का जव समावेश हो जाता है तो उसके पृथक् पाठ करने की क्या आवश्यकता ? जैसे १ श्लेष्मवहुल छर्दि मे वमन का उपयोग । छदिपु वहुदोषासु वमनं
हितमुच्यते । वस्तुत हेतुप्रत्यनीक ही चिकित्सा हुई । तो हेतु विपरीतार्थकारी कहना निष्प्रयोजन हुआ।