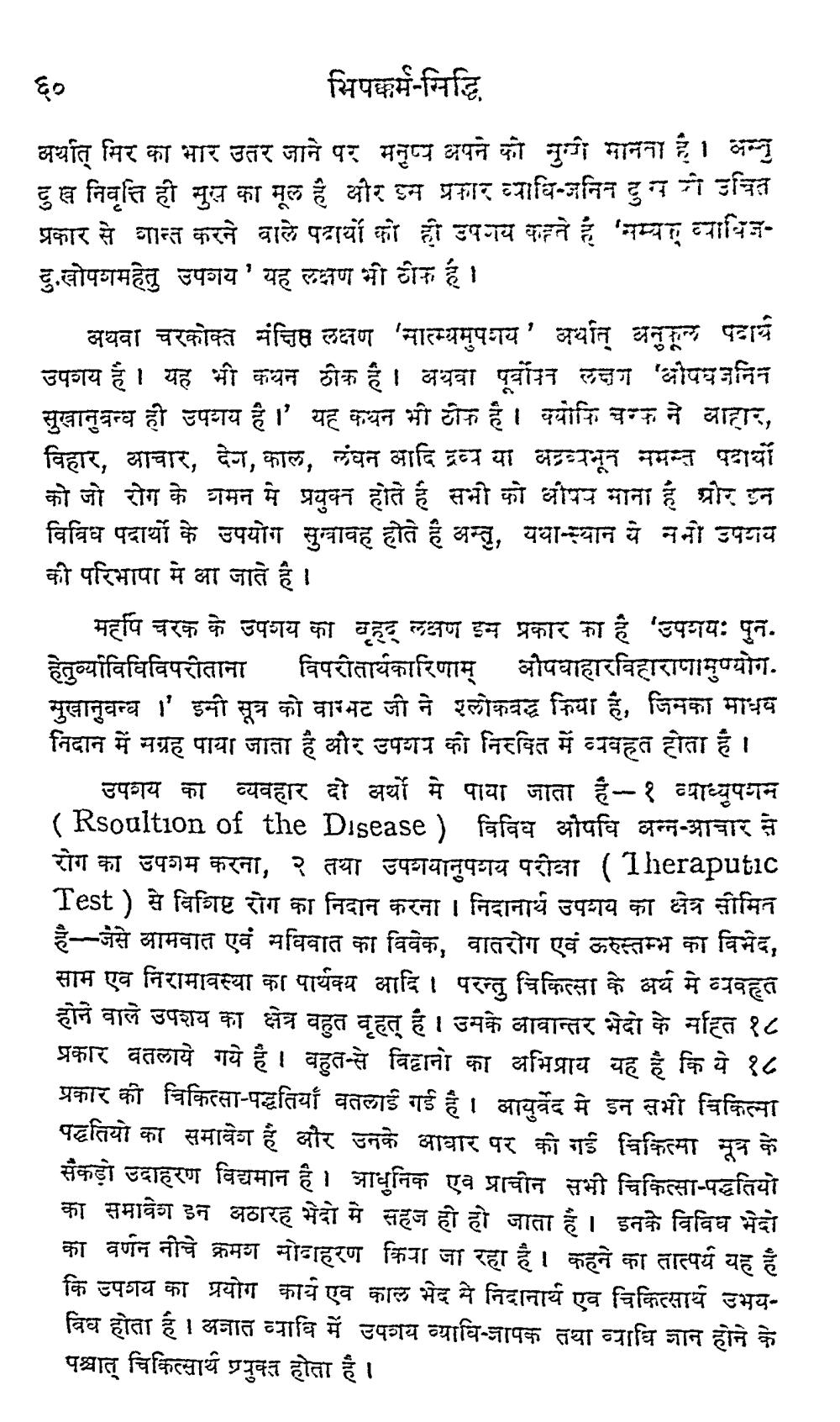________________
भिपकर्म-सिद्धि अर्थात् मिर का भार उतर जाने पर मनुष्य अपने को नुग मानता है । भन्नु दुख निवृत्ति ही सुख का मूल है और इन प्रकार व्याधि-जनित दुपये उचित प्रकार से मान्त करने वाले पदार्यों को ही उपाय कहते है 'सम्यए व्याधिजदु.खोपगमहेतु उपगय ' यह लक्षण भी ठीक है।
अथवा चरकोक्त नंक्षिप्त लक्षण 'मात्म्यमुपगय' अर्थात् अनुकूल पदार्थ उपाय है। यह भी कथन ठीक है। अथवा पूर्वोक्त लक्षग 'ओपय जनित सुखानुबन्ध ही उपगय है।' यह कथन भी ठीक है । क्योकि चरक ने बाहार, विहार, आचार, देश, काल, लंघन आदि द्रव्य या अन्धभूत नमन्त पदार्थों को जो रोग के गमन में प्रयुक्त होते है सभी को श्रीपर माना है और इन विविध पदार्थों के उपयोग सुखावह होते है अन्तु, यथा-स्थान ये ननो उपाय की परिभाषा मे आ जाते है।
महर्षि चरक के उपगय का वृहद् लक्षण इस प्रकार का है 'उपमयः पुन. हेतुाविधिविपरीताना विपरीतार्यकारिणाम् औपचाहारविहाराणामुपयोग. मुखानुबन्ध ।' इनी सूत्र को वाग्मट जी ने श्लोकबद्ध किया है, जिनका माधव निदान में संग्रह पाया जाता है और उपगर की निरक्ति में व्यवहत होता है ।
उपाय का व्यवहार दो अर्थो मे पाया जाता है-१ व्याध्युपगम ( Rsoultion of the Disease ) विविध औषधि अन्न-आचार से रोग का उपशम करना, २ तथा उपगयानुपगय परीक्षा ( Theraputic Test) से विशिष्ट रोग का निदान करना । निदानार्थ उपगय का क्षेत्र सीमित है-जैसे आमवात एवं मविवात का विवेक, वातरोग एवं ऊरुस्तम्भ का विभेद, साम एव निरामावस्या का पार्थक्य आदि। परन्तु चिकित्सा के अर्थ मे व्यवहृत होने वाले उपशय का क्षेत्र वहुत वृहत् है । उसके भावान्तर भेदो के हित १८ प्रकार बतलाये गये है। बहुत-से विद्वानो का अभिप्राय यह है कि ये १८ प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ वतलाई गई है। आयुर्वेद में इन सभी चिकित्सा पद्धतियो का समावेश है और उनके आधार पर की गई चिकित्मा मूत्र के सैकड़ो उदाहरण विद्यमान है। आधुनिक एवं प्राचीन सभी चिकित्सा पद्धतियो का समावेश इन अठारह भेदो मे सहज ही हो जाता है। इनके विविध भेदो का वर्णन नीचे क्रमग मोबाहरण किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपशय का प्रयोग कार्य एव काल भेद से निदानार्थ एव चिकित्सार्थ उभयविध होता है । अज्ञात व्याधि में उपाय व्यावि-जापक तथा व्याधि ज्ञान होने के पश्चात् चिकित्सार्थ प्रयुक्त होता है ।